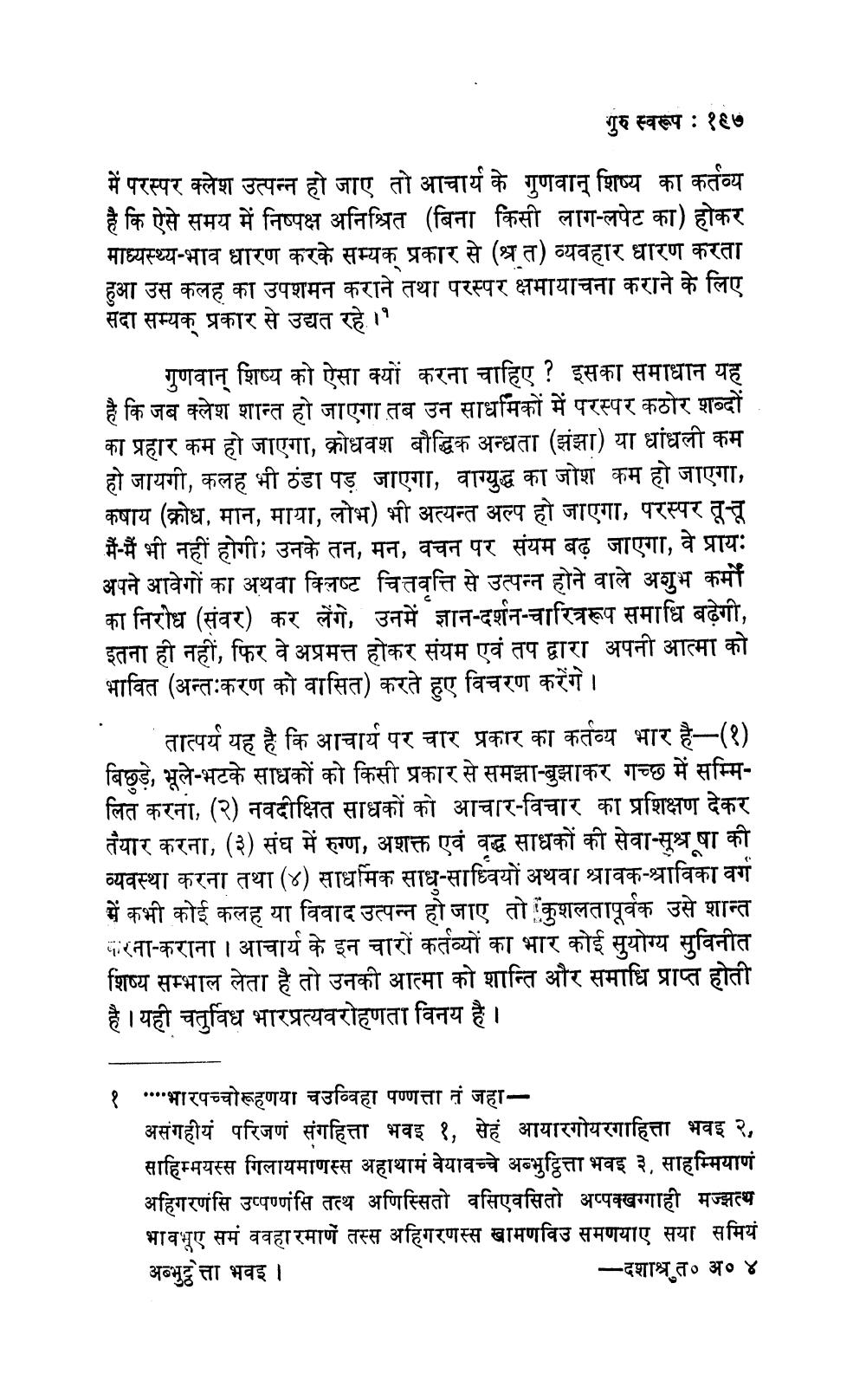________________
गुरु स्वरूप : १६७
में परस्पर क्लेश उत्पन्न हो जाए तो आचार्य के गुणवान् शिष्य का कर्तव्य है कि ऐसे समय में निष्पक्ष अनिश्रित (बिना किसी लाग-लपेट का) होकर माध्यस्थ्य-भाव धारण करके सम्यक प्रकार से (श्र त) व्यवहार धारण करता हुआ उस कलह का उपशमन कराने तथा परस्पर क्षमायाचना कराने के लिए सदा सम्यक् प्रकार से उद्यत रहे ।'
गुणवान् शिष्य को ऐसा क्यों करना चाहिए? इसका समाधान यह है कि जब क्लेश शान्त हो जाएगा तब उन सार्मिकों में परस्पर कठोर शब्दों का प्रहार कम हो जाएगा, क्रोधवश बौद्धिक अन्धता (झंझा) या धांधली कम हो जायगी, कलह भी ठंडा पड़ जाएगा, वाग्युद्ध का जोश कम हो जाएगा, कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) भी अत्यन्त अल्प हो जाएगा, परस्पर तू-तू मैं-मैं भी नहीं होगी; उनके तन, मन, वचन पर संयम बढ़ जाएगा, वे प्रायः अपने आवेगों का अथवा क्लिष्ट चित्तवृत्ति से उत्पन्न होने वाले अशुभ कर्मों का निरोध (संवर) कर लेंगे, उनमें ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप समाधि बढ़ेगी, इतना ही नहीं, फिर वे अप्रमत्त होकर संयम एवं तप द्वारा अपनी आत्मा को भावित (अन्तःकरण को वासित) करते हुए विचरण करेंगे।
तात्पर्य यह है कि आचार्य पर चार प्रकार का कर्तव्य भार है-(१) बिछड़े, भूले-भटके साधकों को किसी प्रकार से समझा-बुझाकर गच्छ में सम्मिलित करना, (२) नवदीक्षित साधकों को आचार-विचार का प्रशिक्षण देकर तैयार करना, (३) संघ में रुग्ण, अशक्त एवं वृद्ध साधकों की सेवा-सुश्रुषा की व्यवस्था करना तथा (४) सार्मिक साधु-साध्वियों अथवा श्रावक-श्राविका वर्ग में कभी कोई कलह या विवाद उत्पन्न हो जाए तो कुशलतापूर्वक उसे शान्त करना-कराना । आचार्य के इन चारों कर्तव्यों का भार कोई सुयोग्य सुविनीत शिष्य सम्भाल लेता है तो उनकी आत्मा को शान्ति और समाधि प्राप्त होती है । यही चतुर्विध भारप्रत्यवरोहणता विनय है।
१ ."भारपच्चोरूहणया चउम्विहा पण्णत्ता तं जहा
असंगहीयं परिजणं संगहित्ता भवइ १, सेहं आयारगोयरगाहित्ता भवइ २, साहिम्मयस्स गिलायमाणस्स अहाथामं वेयावच्चे अब्भुट्टित्ता भवइ ३, साहम्मियाणं अहिगरणंसि उप्पण्णंसि तत्थ अणिस्सितो वसिएवसितो अप्पक्खग्गाही मज्झत्थ भावभूए समं ववहारमाणे तस्स अहिगरणस्स खामणविउ समणयाए सया समियं अब्भुट्ठत्ता भवइ ।
-दशाश्रु त० अ० ४