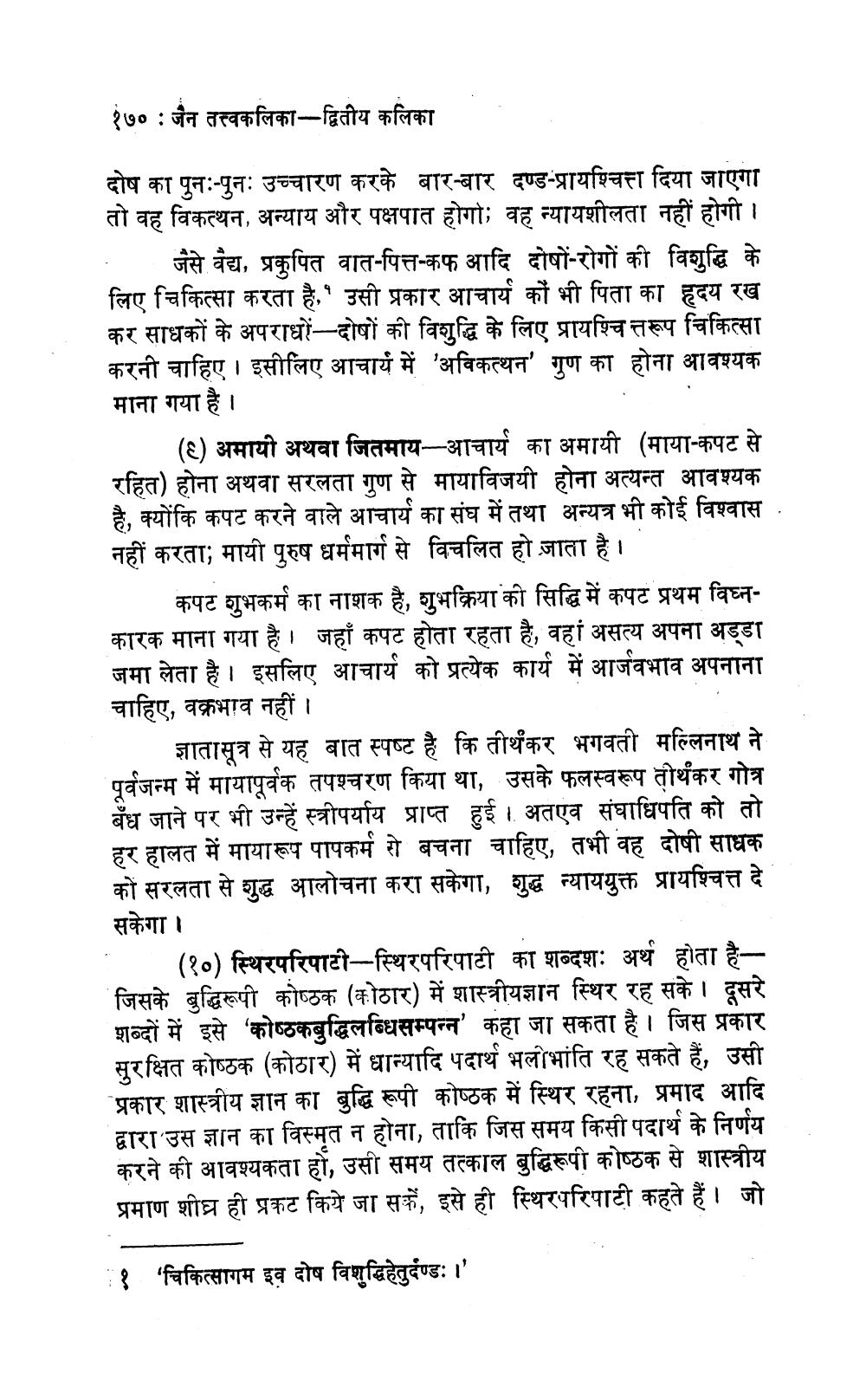________________
१७० : जैन तत्त्वकलिका-द्वितीय कलिका
दोष का पुनः-पुनः उच्चारण करके बार-बार दण्ड-प्रायश्चित्त दिया जाएगा तो वह विकत्थन, अन्याय और पक्षपात होगा; वह न्यायशीलता नहीं होगी। . जैसे वैद्य, प्रकुपित वात-पित्त-कफ आदि दोषों-रोगों की विशुद्धि के लिए चिकित्सा करता है, उसी प्रकार आचार्य को भी पिता का हृदय रख कर साधकों के अपराधों-दोषों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्तरूप चिकित्सा करनी चाहिए । इसीलिए आचार्य में 'अविकत्थन' गुण का होना आवश्यक माना गया है।
(8) अमायी अथवा जितमाय-आचार्य का अमायी (माया-कपट से रहित) होना अथवा सरलता गुण से मायाविजयी होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि कपट करने वाले आचार्य का संघ में तथा अन्यत्र भी कोई विश्वास . नहीं करता; मायी पुरुष धर्ममार्ग से विचलित हो जाता है।
कपट शुभकर्म का नाशक है, शुभक्रिया की सिद्धि में कपट प्रथम विघ्नकारक माना गया है। जहाँ कपट होता रहता है, वहां असत्य अपना अड्डा जमा लेता है। इसलिए आचार्य को प्रत्येक कार्य में आर्जवभाव अपनाना चाहिए, वक्रभाव नहीं।
ज्ञातासूत्र से यह बात स्पष्ट है कि तीर्थंकर भगवती मल्लिनाथ ने पूर्वजन्म में मायापूर्वक तपश्चरण किया था, उसके फलस्वरूप तीर्थंकर गोत्र बँध जाने पर भी उन्हें स्त्रीपर्याय प्राप्त हुई। अतएव संघाधिपति को तो हर हालत में मायारूप पापकर्म से बचना चाहिए, तभी वह दोषी साधक को सरलता से शुद्ध आलोचना करा सकेगा, शुद्ध न्याययुक्त प्रायश्चित्त दे सकेगा।
(१०) स्थिरपरिपाटी-स्थिरपरिपाटी का शब्दशः अर्थ होता हैजिसके बुद्धिरूपी कोष्ठक (कोठार) में शास्त्रीयज्ञान स्थिर रह सके। दूसरे शब्दों में इसे 'कोष्ठकबुद्धिलब्धिसम्पन्न' कहा जा सकता है। जिस प्रकार सुरक्षित कोष्ठक (कोठार) में धान्यादि पदार्थ भलीभांति रह सकते हैं, उसी प्रकार शास्त्रीय ज्ञान का बुद्धि रूपी कोष्ठक में स्थिर रहना, प्रमाद आदि द्वारा उस ज्ञान का विस्मत न होना, ताकि जिस समय किसी पदार्थ के निर्णय करने की आवश्यकता हो, उसी समय तत्काल बुद्धिरूपी कोष्ठक से शास्त्रीय प्रमाण शीघ्र ही प्रकट किये जा सकें, इसे ही स्थिरपरिपाटी कहते हैं। जो
१ 'चिकित्सागम इव दोष विशुद्धिहेतुर्दण्डः ।'