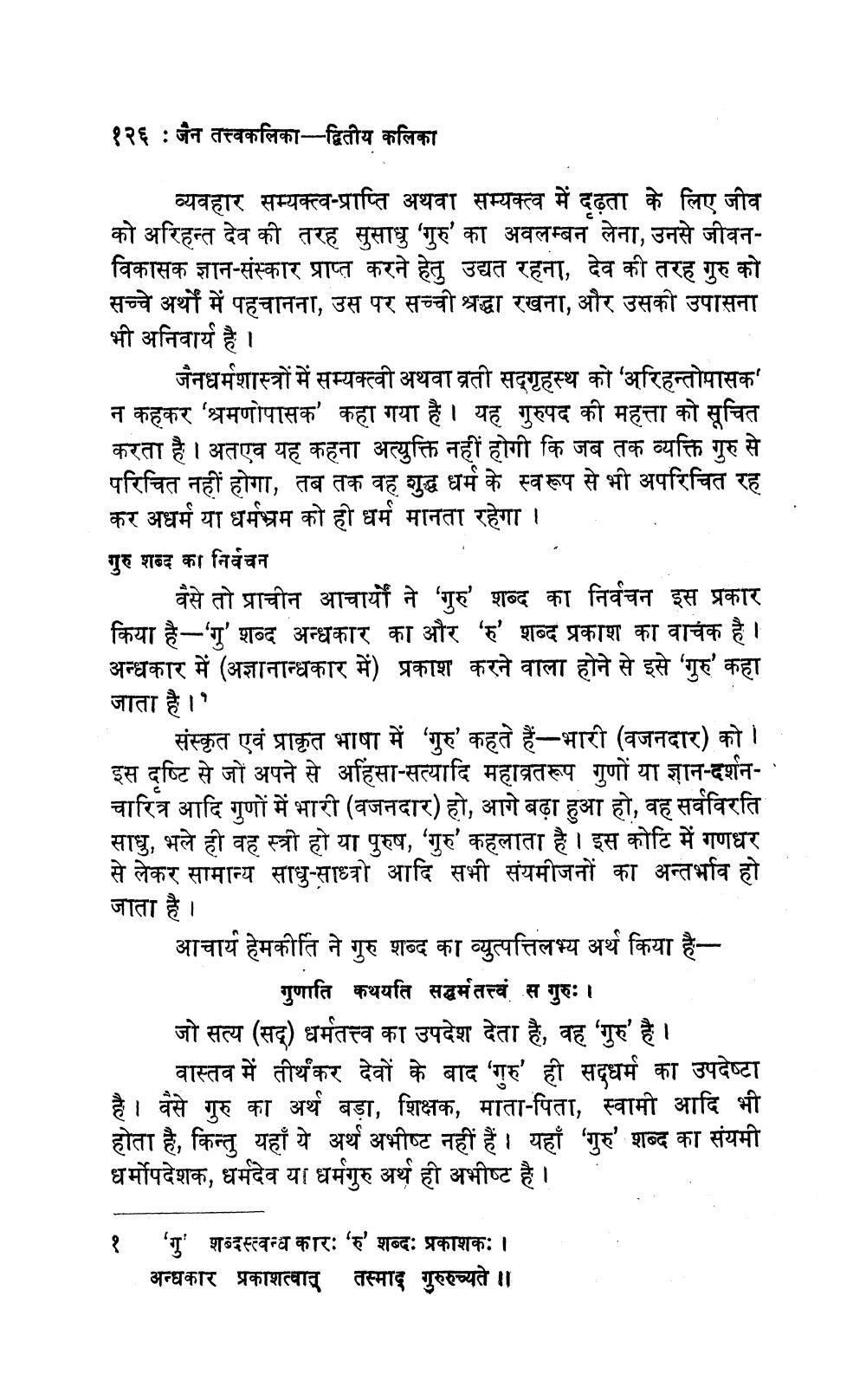________________
१२६ : जैन तत्त्वकलिका-द्वितीय कलिका
व्यवहार सम्यक्त्व-प्राप्ति अथवा सम्यक्त्व में दढ़ता के लिए जीव को अरिहन्त देव की तरह सुसाधु 'गुरु' का अवलम्बन लेना, उनसे जीवनविकासक ज्ञान-संस्कार प्राप्त करने हेतु उद्यत रहना, देव की तरह गुरु को सच्चे अर्थों में पहचानना, उस पर सच्ची श्रद्धा रखना, और उसको उपासना भी अनिवार्य है।
जैनधर्मशास्त्रों में सम्यक्त्वी अथवा व्रती सद्गृहस्थ को 'अरिहन्तोपासक' न कहकर 'श्रमणोपासक' कहा गया है। यह गुरुपद की महत्ता को सूचित करता है । अतएव यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि जब तक व्यक्ति गुरु से परिचित नहीं होगा, तब तक वह शुद्ध धर्म के स्वरूप से भी अपरिचित रह कर अधर्म या धर्मभ्रम को ही धर्म मानता रहेगा। गुरु शब्द का निर्वचन
वैसे तो प्राचीन आचार्यों ने 'गुरु' शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है-'गु' शब्द अन्धकार का और 'रु' शब्द प्रकाश का वाचक है। अन्धकार में (अज्ञानान्धकार में) प्रकाश करने वाला होने से इसे 'गुरु' कहा जाता है।
संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में 'गुरु' कहते हैं-भारी (वजनदार) को । इस दष्टि से जो अपने से अहिंसा-सत्यादि महाव्रतरूप गुणों या ज्ञान-दर्शनचारित्र आदि गुणों में भारी (वजनदार) हो, आगे बढ़ा हुआ हो, वह सर्वविरति साधु, भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, 'गुरु' कहलाता है। इस कोटि में गणधर से लेकर सामान्य साधु-साध्वो आदि सभी संयमीजनों का अन्तर्भाव हो जाता है। आचार्य हेमकीर्ति ने गुरु शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ किया है
गुणाति कथयति सद्धर्मतत्त्वं स गुरुः। जो सत्य (सद्) धर्मतत्त्व का उपदेश देता है, वह 'गुरु' है।
वास्तव में तीर्थंकर देवों के बाद 'गरु' ही सद्धर्म का उपदेष्टा है। वैसे गुरु का अर्थ बड़ा, शिक्षक, माता-पिता, स्वामी आदि भी होता है, किन्तु यहाँ ये अर्थ अभीष्ट नहीं हैं। यहाँ 'गुरु' शब्द का संयमी धर्मोपदेशक, धर्मदेव या धर्मगुरु अर्थ ही अभीष्ट है।
१
'गु' शब्दस्त्वन्ध कारः 'ह' शब्दः प्रकाशकः । अन्धकार प्रकाशत्वात् तस्माद् गुरुरुच्यते ॥