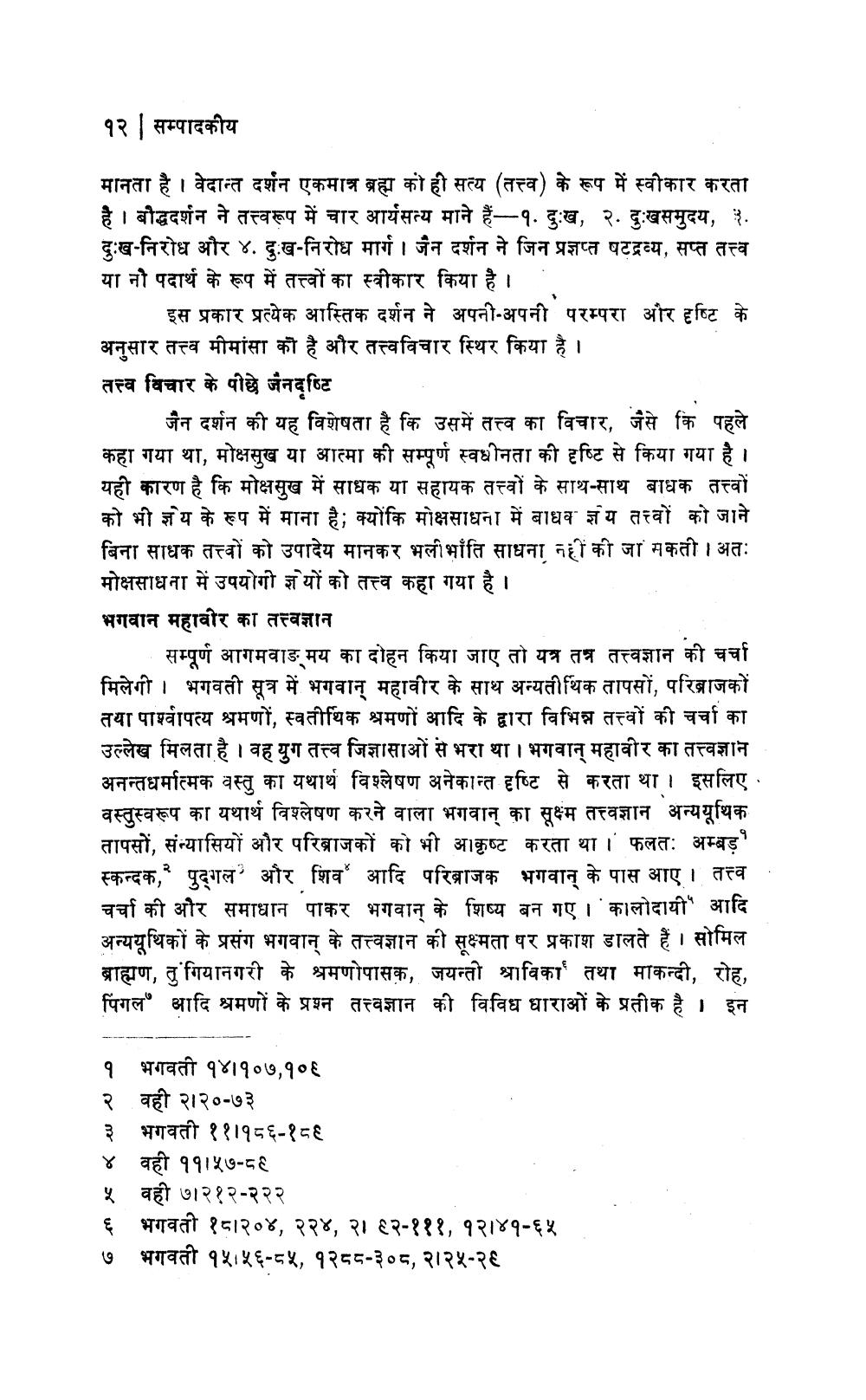________________
१२ / सम्पादकीय
मानता है । वेदान्त दर्शन एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य (तत्त्व) के रूप में स्वीकार करता है । बौद्धदर्शन ने तत्त्वरूप में चार आर्यसत्य माने हैं-१. दुःख, २. दुःखसमुदय, ३. दुःख-निरोध और ४. दुःख-निरोध मार्ग । जैन दर्शन ने जिन प्रज्ञप्त षटद्रव्य, सप्त तत्त्व या नो पदार्थ के रूप में तत्त्वों का स्वीकार किया है।
इस प्रकार प्रत्येक आस्तिक दर्शन ने अपनी-अपनी परम्परा और दृष्टि के अनुसार तत्त्व मीमांसा की है और तत्त्वविचार स्थिर किया है। तत्त्व विचार के पीछे जनदृष्टि
जैन दर्शन की यह विशेषता है कि उसमें तत्त्व का विचार, जैसे कि पहले कहा गया था, मोक्षसुख या आत्मा की सम्पूर्ण स्वधीनता की दृष्टि से किया गया है । यही कारण है कि मोक्षसुख में साधक या सहायक तत्त्वों के साथ-साथ बाधक तत्त्वों को भी ज्ञेय के रूप में माना है; क्योंकि मोक्षसाधना में बाधव ज्ञय तत्त्वों को जाने बिना साधक तत्त्वों को उपादेय मानकर भली भाँति साधना नहीं की जा सकती। अतः मोक्षसाधना में उपयोगी ज्ञ यों को तत्त्व कहा गया है। भगवान महावीर का तत्त्वज्ञान
- सम्पूर्ण आगमवाङमय का दोहन किया जाए तो यत्र तत्र तत्त्वज्ञान की चर्चा मिलेगी। भगवती सूत्र में भगवान् महावीर के साथ अन्यतीथिक तापसों, परिब्राजकों तया पावापत्य श्रमणों, स्वतीथिक श्रमणों आदि के द्वारा विभिन्न तत्त्वों की चर्चा का उल्लेख मिलता है । वह युग तत्त्व जिज्ञासाओं से भरा था। भगवान् महावीर का तत्त्वज्ञान अनन्तधर्मात्मक वस्तु का यथार्थ विश्लेषण अनेकान्त दृष्टि से करता था। इसलिए . वस्तुस्वरूप का यथार्थ विश्लेषण करने वाला भगवान् का सूक्ष्म तत्त्वज्ञान अन्य यूथिक तापसों, संन्यासियों और परिब्राजकों को भी आकृष्ट करता था। फलतः अम्बड़ स्कन्दक, पुद्गल' और शिव आदि परिव्राजक भगवान् के पास आए । तत्त्व चर्चा की और समाधान पाकर भगवान् के शिष्य बन गए। कालोदायी' आदि अन्ययूथिकों के प्रसंग भगवान् के तत्त्वज्ञान की सूक्ष्मता पर प्रकाश डालते हैं । सोमिल ब्राह्मण, तुगियानगरी के श्रमणोपासक, जयन्ती श्राविका तथा माकन्दी, रोह, पिंगल आदि श्रमणों के प्रश्न तत्त्वज्ञान की विविध धाराओं के प्रतीक है । इन
१ भगवती १४।१०७,१०६ २ वही २।२०-७३ ३ भगवती ११।१८६-१८६ ४ वही ११।५७-८६ ५ वही ७।२१२-२२२ ६ भगवती १८।२०४, २२४, २। ६२-१११, १२।४१-६५ ७ भगवती १५५६-८५, १२८८-३०८, २।२५-२६