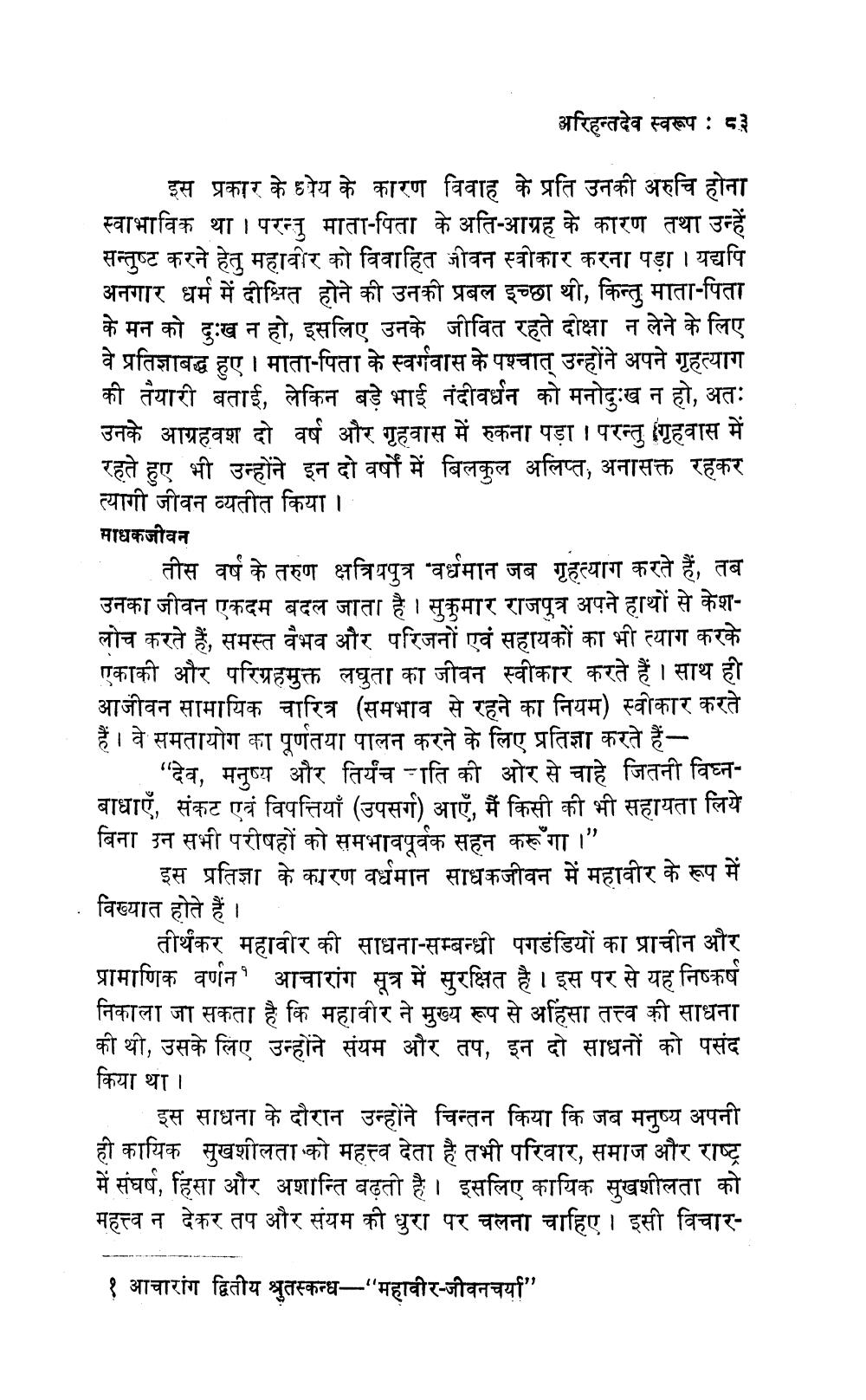________________
अरिहन्तदेव स्वरूप : ८३
इस प्रकार के ध्येय के कारण विवाह के प्रति उनकी अरुचि होना स्वाभाविक था। परन्तु माता-पिता के अति-आग्रह के कारण तथा उन्हें सन्तुष्ट करने हेतु महावीर को विवाहित जीवन स्वीकार करना पड़ा । यद्यपि अनगार धर्म में दीक्षित होने की उनकी प्रबल इच्छा थी, किन्तु माता-पिता के मन को दुःख न हो, इसलिए उनके जीवित रहते दोक्षा न लेने के लिए वे प्रतिज्ञाबद्ध हुए। माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उन्होंने अपने गृहत्याग की तैयारी बताई, लेकिन बड़े भाई नंदीवर्धन को मनोदुःख न हो, अतः उनके आग्रहवश दो वर्ष और गृहवास में रुकना पडा । परन्तु गृहवास में रहते हुए भी उन्होंने इन दो वर्षों में बिलकुल अलिप्त, अनासक्त रहकर त्यागी जीवन व्यतीत किया। माधकजीवन
तीस वर्ष के तरुण क्षत्रियपुत्र “वर्धमान जब गृहत्याग करते हैं, तब उनका जीवन एकदम बदल जाता है। सुकुमार राजपूत्र अपने हाथों से केशलोच करते हैं, समस्त वैभव और परिजनों एवं सहायकों का भी त्याग करके एकाकी और परिग्रहमुक्त लघुता का जीवन स्वीकार करते हैं। साथ ही आजीवन सामायिक चारित्र (समभाव से रहने का नियम) स्वीकार करते हैं। वे समतायोग का पूर्णतया पालन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं
__"देव, मनुष्य और तिर्यंच -गति की ओर से चाहे जितनी विघ्नबाधाएँ, संकट एवं विपत्तियाँ (उपसर्ग) आएँ, मैं किसी की भी सहायता लिये बिना उन सभी परीषहों को समभावपूर्वक सहन करूंगा।"
इस प्रतिज्ञा के कारण वर्धमान साधकजीवन में महावीर के रूप में विख्यात होते हैं।
तीर्थंकर महावीर की साधना-सम्बन्धी पगडंडियों का प्राचीन और प्रामाणिक वर्णन आचारांग सत्र में सरक्षित है। इस पर से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महावीर ने मुख्य रूप से अहिंसा तत्त्व की साधना की थी, उसके लिए उन्होंने संयम और तप, इन दो साधनों को पसंद किया था।
इस साधना के दौरान उन्होंने चिन्तन किया कि जब मनुष्य अपनी ही कायिक सूखशीलता को महत्त्व देता है तभी परिवार, समाज और राष्ट्र में संघर्ष, हिंसा और अशान्ति बढ़ती है। इसलिए कायिक सूखशीलता को महत्त्व न देकर तप और संयम की धुरा पर चलना चाहिए। इसी विचार
१ आचारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध-"महावीर-जीवनचर्या"