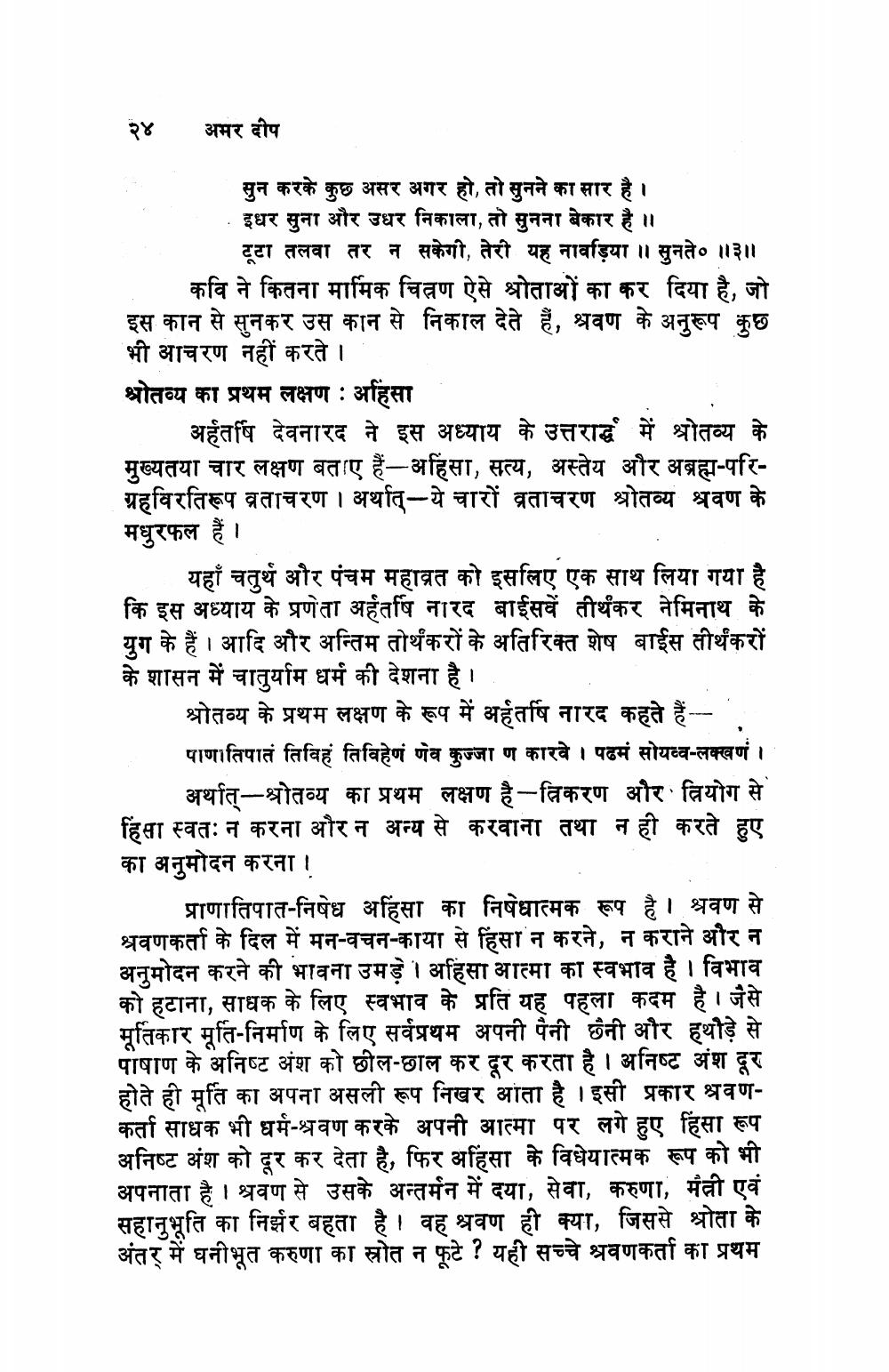________________
२४
अमर दीप
सुन करके कुछ असर अगर हो, तो सुनने का सार है । इधर सुना और उधर निकाला, तो सुनना बेकार है ॥
टूटा तलवा तर न सकेगी, तेरी यह नावड़िया || सुनते० ॥३॥
कवि ने कितना मार्मिक चित्रण ऐसे श्रोताओं का कर दिया है, जो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, श्रवण के अनुरूप कुछ भी आचरण नहीं करते ।
श्रोतव्य का प्रथम लक्षण : अहिंसा
अर्हतषि देवनारद ने इस अध्याय के उत्तरार्द्ध में श्रोतव्य के मुख्यतया चार लक्षण बताए हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अब्रह्म-परिग्रहविरतिरूप व्रताचरण । अर्थात् - ये चारों व्रताचरण श्रोतव्यं श्रवण के मधुरफल हैं ।
यहाँ चतुर्थं और पंचम महाव्रत को इसलिए एक साथ लिया गया है। कि इस अध्याय के प्रणेता अर्हतर्षि नारद बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ के युग 'के हैं । आदि और अन्तिम तोर्थंकरों के अतिरिक्त शेष बाईस तीर्थंकरों के शासन में चातुर्याम धर्म की देशना है ।
1
श्रोतव्य के प्रथम लक्षण के रूप में अर्हतर्षि नारद कहते हैंपाणातिपातं तिविहं तिविहेणं णेव कुज्जा ण कारवे । पढमं सोयव्व - लक्खणं अर्थात् - श्रोतव्य का प्रथम लक्षण है - त्रिकरण और त्रियोग से हिंसा स्वतः न करना और न अन्य से करवाना तथा न ही करते हुए का अनुमोदन करना !
.
प्राणातिपात-निषेध अहिंसा का निषेधात्मक रूप है | श्रवण से श्रवणकर्ता के दिल में मन-वचन काया से हिंसा न करने, न कराने और न अनुमोदन करने की भावना उमड़े । अहिंसा आत्मा का स्वभाव है । विभाव को हटाना, साधक के लिए स्वभाव के प्रति यह पहला कदम है । जैसे मूर्तिकार मूर्ति निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपनी पैनी छैनी और हथौड़े से पाषाण के अनिष्ट अंश को छील छाल कर दूर करता है । अनिष्ट अंश दूर होते ही मूर्ति का अपना असली रूप निखर आता है । इसी प्रकार श्रवणकर्ता साधक भी धर्म-श्रवण करके अपनी आत्मा पर लगे हुए हिंसा रूप अनिष्ट अंश को दूर कर देता है, फिर अहिंसा के विधेयात्मक रूप को भी अपनाता है | श्रवण से उसके अन्तर्मन में दया, सेवा, करुणा, मंत्री एवं सहानुभूति का निर्झर बहता है । वह श्रवण ही क्या, जिससे श्रोता के अंतर् में घनीभूत करुणा का स्रोत न फूटे ? यही सच्चे श्रवणकर्ता का प्रथम