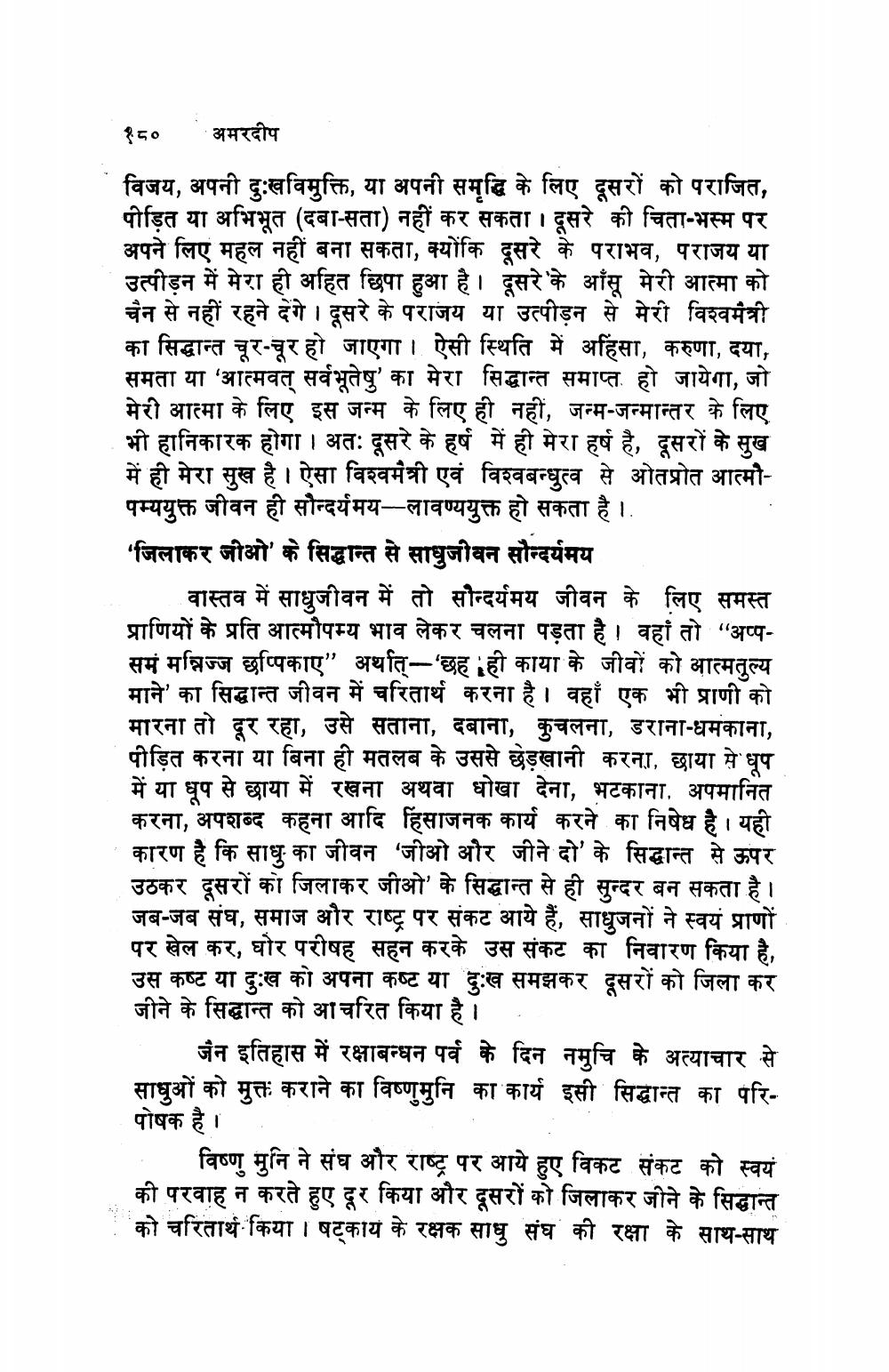________________
१८० अमरदीप विजय, अपनी दुःखविमुक्ति, या अपनी समृद्धि के लिए दूसरों को पराजित, पीड़ित या अभिभूत (दबा-सता) नहीं कर सकता। दूसरे की चिता-भस्म पर अपने लिए महल नहीं बना सकता, क्योंकि दूसरे के पराभव, पराजय या उत्पीड़न में मेरा ही अहित छिपा हुआ है। दूसरे के आँसू मेरी आत्मा को चैन से नहीं रहने देंगे । दूसरे के पराजय या उत्पीड़न से मेरी विश्वमैत्री का सिद्धान्त चूर-चूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अहिंसा, करुणा, दया, समता या 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का मेरा सिद्धान्त समाप्त हो जायेगा, जो मेरी आत्मा के लिए इस जन्म के लिए ही नहीं, जन्म-जन्मान्तर के लिए भी हानिकारक होगा। अतः दूसरे के हर्ष में ही मेरा हर्ष है, दूसरों के सुख में ही मेरा सुख है। ऐसा विश्वमैत्री एवं विश्वबन्धुत्व से ओतप्रोत आत्मीपम्ययुक्त जीवन ही सौन्दर्यमय-लावण्ययुक्त हो सकता है।. 'जिलाकर जीओ' के सिद्धान्त से साधुजीवन सौन्दर्यमय
वास्तव में साधुजीवन में तो सौन्दर्यमय जीवन के लिए समस्त प्राणियों के प्रति आत्मौपम्य भाव लेकर चलना पड़ता है। वहां तो "अप्पसमं मनिज्ज छप्पिकाए" अर्थात्-'छह ही काया के जीवों को आत्मतुल्य माने' का सिद्धान्त जीवन में चरितार्थ करना है। वहाँ एक भी प्राणी को मारना तो दूर रहा, उसे सताना, दबाना, कुचलना, डराना-धमकाना, पीडित करना या बिना ही मतलब के उससे छेड़खानी करना, छाया से धूप में या धूप से छाया में रखना अथवा धोखा देना, भटकाना, अपमानित करना, अपशब्द कहना आदि हिंसाजनक कार्य करने का निषेध है। यही कारण है कि साधु का जीवन 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त से ऊपर उठकर दूसरों को जिलाकर जीओ' के सिद्धान्त से ही सुन्दर बन सकता है। जब-जब संघ, समाज और राष्ट्र पर संकट आये हैं, साधुजनों ने स्वयं प्राणों पर खेल कर, घोर परीषह सहन करके उस संकट का निवारण किया है, उस कष्ट या दुःख को अपना कष्ट या दुःख समझकर दूसरों को जिला कर जीने के सिद्धान्त को आचरित किया है।
जैन इतिहास में रक्षाबन्धन पर्व के दिन नमुचि के अत्याचार से साधुओं को मुक्त कराने का विष्णुमुनि का कार्य इसी सिद्धान्त का परिपोषक है।
विष्णु मुनि ने संघ और राष्ट्र पर आये हुए विकट संकट को स्वयं की परवाह न करते हुए दूर किया और दूसरों को जिलाकर जीने के सिद्धान्त को चरितार्थ किया । षट्काय के रक्षक साधु संघ की रक्षा के साथ-साथ