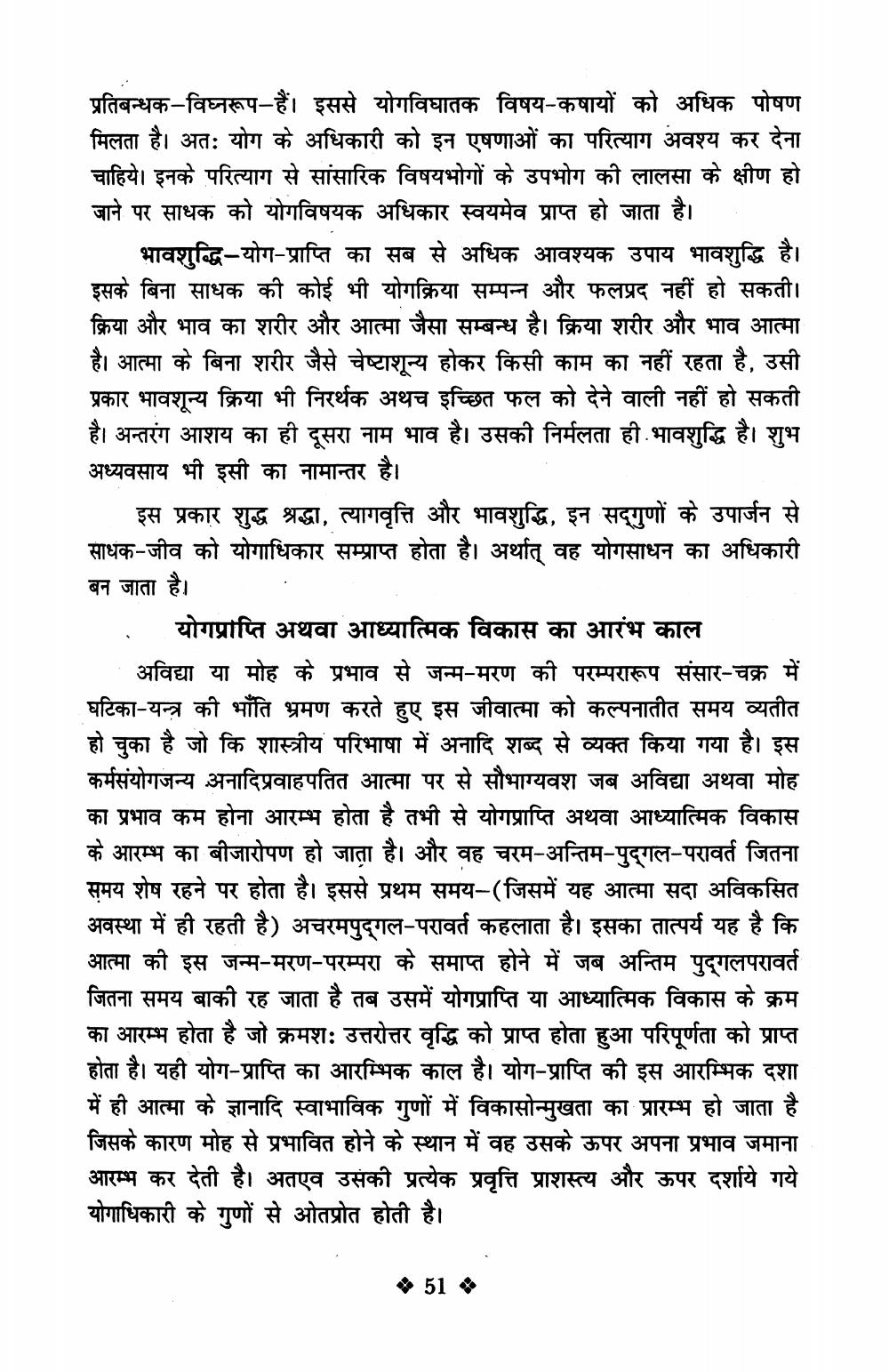________________
प्रतिबन्धक-विघ्नरूप-हैं। इससे योगविघातक विषय-कषायों को अधिक पोषण मिलता है। अतः योग के अधिकारी को इन एषणाओं का परित्याग अवश्य कर देना चाहिये। इनके परित्याग से सांसारिक विषयभोगों के उपभोग की लालसा के क्षीण हो जाने पर साधक को योगविषयक अधिकार स्वयमेव प्राप्त हो जाता है।
भावशुद्धि-योग-प्राप्ति का सब से अधिक आवश्यक उपाय भावशुद्धि है। इसके बिना साधक की कोई भी योगक्रिया सम्पन्न और फलप्रद नहीं हो सकती। क्रिया और भाव का शरीर और आत्मा जैसा सम्बन्ध है। क्रिया शरीर और भाव आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर जैसे चेष्टाशून्य होकर किसी काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार भावशून्य क्रिया भी निरर्थक अथच इच्छित फल को देने वाली नहीं हो सकती है। अन्तरंग आशय का ही दूसरा नाम भाव है। उसकी निर्मलता ही भावशुद्धि है। शुभ अध्यवसाय भी इसी का नामान्तर है।
इस प्रकार शुद्ध श्रद्धा, त्यागवृत्ति और भावशुद्धि, इन सद्गुणों के उपार्जन से साधक-जीव को योगाधिकार सम्प्राप्त होता है। अर्थात् वह योगसाधन का अधिकारी बन जाता है।
. योगप्राप्ति अथवा आध्यात्मिक विकास का आरंभ काल - अविद्या या मोह के प्रभाव से जन्म-मरण की परम्परारूप संसार-चक्र में घटिका-यन्त्र की भाँति भ्रमण करते हुए इस जीवात्मा को कल्पनातीत समय व्यतीत हो चुका है जो कि शास्त्रीय परिभाषा में अनादि शब्द से व्यक्त किया गया है। इस कर्मसंयोगजन्य अनादिप्रवाहपतित आत्मा पर से सौभाग्यवश जब अविद्या अथवा मोह का प्रभाव कम होना आरम्भ होता है तभी से योगप्राप्ति अथवा आध्यात्मिक विकास के आरम्भ का बीजारोपण हो जाता है। और वह चरम-अन्तिम-पुद्गल-परावर्त जितना समय शेष रहने पर होता है। इससे प्रथम समय-(जिसमें यह आत्मा सदा अविकसित अवस्था में ही रहती है) अचरमपुद्गल-परावर्त कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा की इस जन्म-मरण-परम्परा के समाप्त होने में जब अन्तिम पुद्गलपरावर्त जितना समय बाकी रह जाता है तब उसमें योगप्राप्ति या आध्यात्मिक विकास के क्रम का आरम्भ होता है जो क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ परिपूर्णता को प्राप्त होता है। यही योग-प्राप्ति का आरम्भिक काल है। योग-प्राप्ति की इस आरम्भिक दशा में ही आत्मा के ज्ञानादि स्वाभाविक गुणों में विकासोन्मुखता का प्रारम्भ हो जाता है जिसके कारण मोह से प्रभावित होने के स्थान में वह उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ कर देती है। अतएव उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति प्राशस्त्य और ऊपर दर्शाये गये योगाधिकारी के गुणों से ओतप्रोत होती है।
.51.