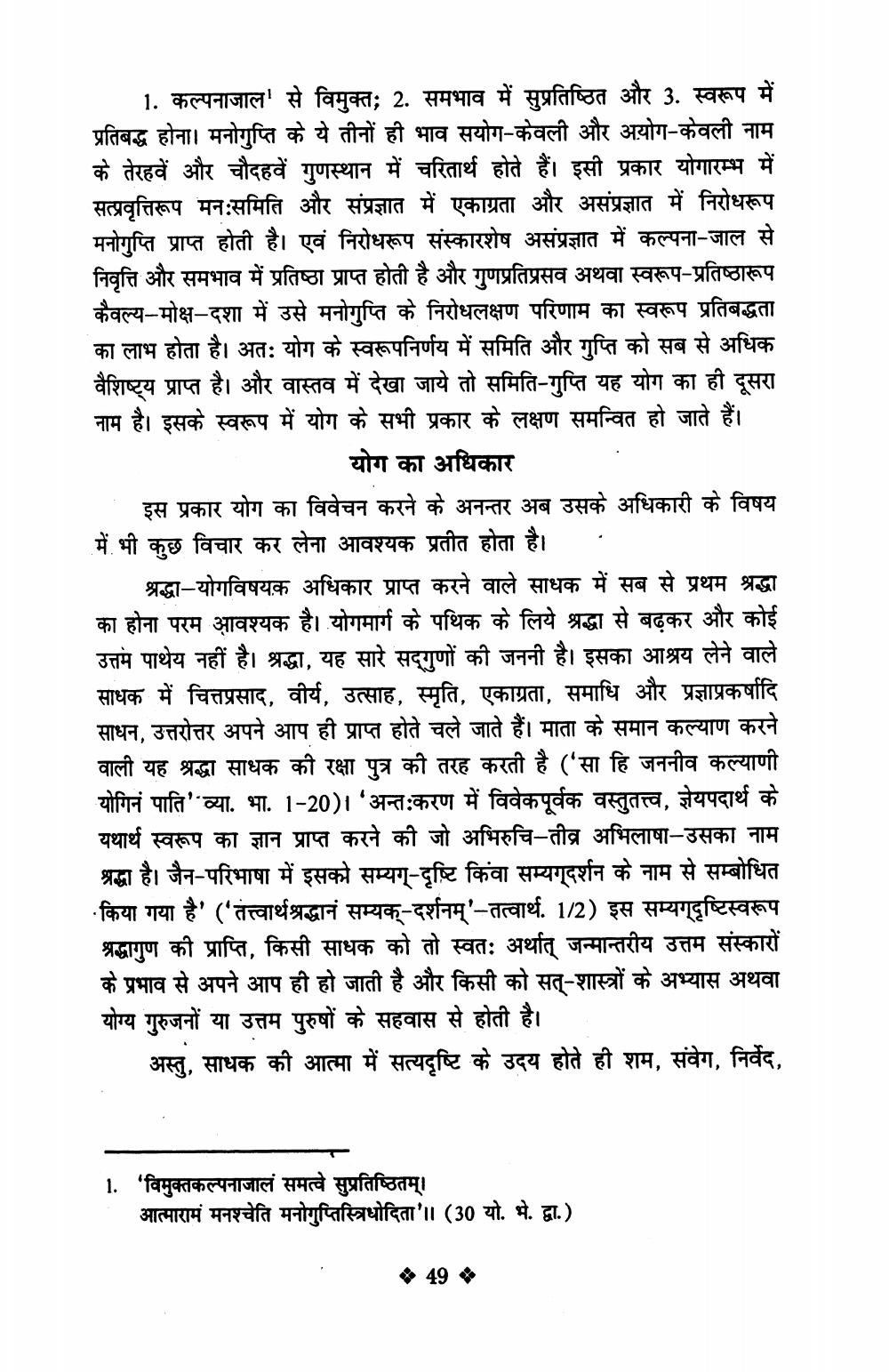________________
1. कल्पनाजाल' से विमुक्त; 2. समभाव में सुप्रतिष्ठित और 3. स्वरूप में प्रतिबद्ध होना । मनोगुप्ति के ये तीनों ही भाव सयोग- केवली और अयोग- केवली नाम के तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में चरितार्थ होते हैं। इसी प्रकार योगारम्भ में सत्प्रवृत्तिरूप मनःसमिति और संप्रज्ञात में एकाग्रता और असंप्रज्ञात में निरोधरूप मनोगुप्ति प्राप्त होती है। एवं निरोधरूप संस्कारशेष असंप्रज्ञात में कल्पना - जाल से निवृत्ति और समभाव में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और गुणप्रतिप्रसव अथवा स्वरूप- प्रतिष्ठारूप कैवल्य - मोक्ष - दशा में उसे मनोगुप्ति के निरोधलक्षण परिणाम का स्वरूप प्रतिबद्धता का लाभ होता है। अतः योग के स्वरूपनिर्णय में समिति और गुप्ति को सब से अधिक वैशिष्ट्य प्राप्त है। और वास्तव में देखा जाये तो समिति गुप्ति यह योग का ही दूसरा नाम है। इसके स्वरूप में योग के सभी प्रकार के लक्षण समन्वित हो जाते हैं। योग का अधिकार
इस प्रकार योग का विवेचन करने के अनन्तर अब उसके अधिकारी के विषय में भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।
श्रद्धा-योगविषयक अधिकार प्राप्त करने वाले साधक में सब से प्रथम श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। योगमार्ग के पथिक के लिये श्रद्धा से बढ़कर और कोई उत्तम पाथेय नहीं है। श्रद्धा, यह सारे सद्गुणों की जननी है। इसका आश्रय लेने वाले साधक में चित्तप्रसाद, वीर्य, उत्साह, स्मृति, एकाग्रता, समाधि और प्रज्ञाप्रकर्षादि साधन, उत्तरोत्तर अपने आप ही प्राप्त होते चले जाते हैं। माता के समान कल्याण करने वाली यह श्रद्धा साधक की रक्षा पुत्र की तरह करती है ('सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति' व्या. भा. 1 - 20 ) । ' अन्त:करण में विवेकपूर्वक वस्तुतत्त्व, ज्ञेयपदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की जो अभिरुचि - तीव्र अभिलाषा - उसका नाम श्रद्धा है। जैन- परिभाषा में इसको सम्यग्दृष्टि किंवा सम्यग्दर्शन के नाम से सम्बोधित · किया गया है' ('तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् - दर्शनम्' - तत्वार्थ. 1/2 ) इस सम्यग्दृष्टिस्वरूप श्रद्धागुण की प्राप्ति, किसी साधक को तो स्वतः अर्थात् जन्मान्तरीय उत्तम संस्कारों के प्रभाव से अपने आप ही हो जाती है और किसी को सत्-शास्त्रों के अभ्यास अथवा योग्य गुरुजनों या उत्तम पुरुषों के सहवास से होती है।
अस्तु, साधक की आत्मा में सत्यदृष्टि के उदय होते ही शम,
1. 'विमुक्तकल्पनाजालं समत्वे सुप्रतिष्ठितम्।
आत्मारामं मनश्चेति मनोगुप्तिस्त्रिधोदिता ।। (30 यो. भे. द्वा.)
49
संवेग, निर्वेद,