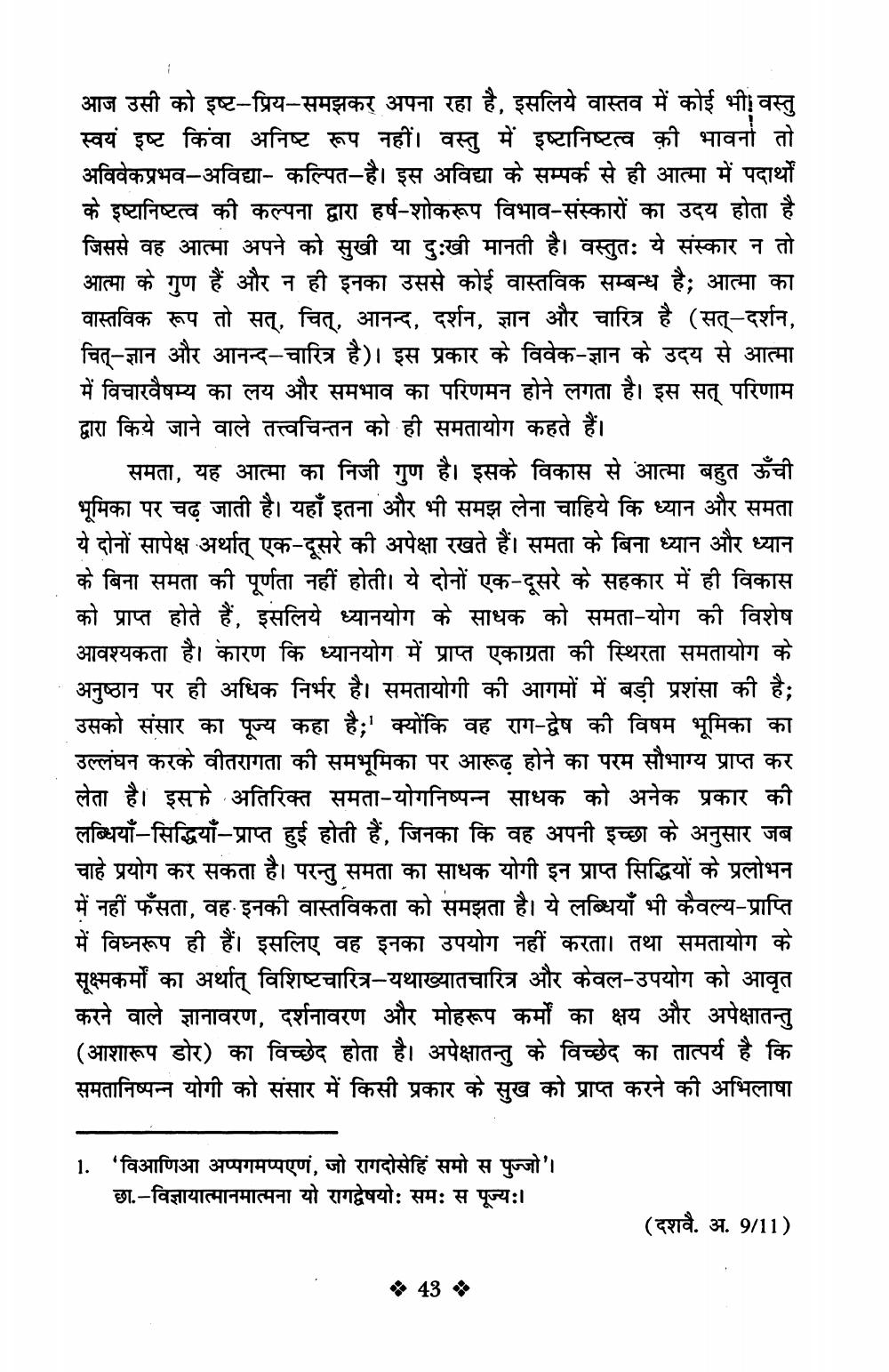________________
आज उसी को इष्ट-प्रिय-समझकर अपना रहा है, इसलिये वास्तव में कोई भी वस्तु स्वयं इष्ट किंवा अनिष्ट रूप नहीं। वस्तु में इष्टानिष्टत्व की भावना तो अविवेकप्रभव-अविद्या- कल्पित है। इस अविद्या के सम्पर्क से ही आत्मा में पदार्थों के इष्टानिष्टत्व की कल्पना द्वारा हर्ष-शोकरूप विभाव-संस्कारों का उदय होता है जिससे वह आत्मा अपने को सुखी या दुःखी मानती है। वस्तुतः ये संस्कार न तो आत्मा के गुण हैं और न ही इनका उससे कोई वास्तविक सम्बन्ध है; आत्मा का वास्तविक रूप तो सत्, चित्, आनन्द, दर्शन, ज्ञान और चारित्र है (सत्-दर्शन, चित्-ज्ञान और आनन्द-चारित्र है)। इस प्रकार के विवेक-ज्ञान के उदय से आत्मा में विचारवैषम्य का लय और समभाव का परिणमन होने लगता है। इस सत् परिणाम द्वारा किये जाने वाले तत्त्वचिन्तन को ही समतायोग कहते हैं। __समता, यह आत्मा का निजी गुण है। इसके विकास से आत्मा बहुत ऊँची भूमिका पर चढ़ जाती है। यहाँ इतना और भी समझ लेना चाहिये कि ध्यान और समता ये दोनों सापेक्ष अर्थात् एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। समता के बिना ध्यान और ध्यान के बिना समता की पूर्णता नहीं होती। ये दोनों एक-दूसरे के सहकार में ही विकास को प्राप्त होते हैं, इसलिये ध्यानयोग के साधक को समता-योग की विशेष आवश्यकता है। कारण कि ध्यानयोग में प्राप्त एकाग्रता की स्थिरता समतायोग के अनुष्ठान पर ही अधिक निर्भर है। समतायोगी की आगमों में बड़ी प्रशंसा की है। उसको संसार का पूज्य कहा है; क्योंकि वह राग-द्वेष की विषम भूमिका का उल्लंघन करके वीतरागता की समभूमिका पर आरूढ़ होने का परम सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त समता-योगनिष्पन्न साधक को अनेक प्रकार की लब्धियाँ-सिद्धियाँ-प्राप्त हुई होती हैं, जिनका कि वह अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे प्रयोग कर सकता है। परन्तु समता का साधक योगी इन प्राप्त सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं फंसता, वह इनकी वास्तविकता को समझता है। ये लब्धियाँ भी कैवल्य-प्राप्ति में विघ्नरूप ही हैं। इसलिए वह इनका उपयोग नहीं करता। तथा समतायोग के सूक्ष्मकर्मों का अर्थात् विशिष्टचारित्र-यथाख्यातचारित्र और केवल-उपयोग को आवृत करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहरूप कर्मों का क्षय और अपेक्षातन्तु (आशारूप डोर) का विच्छेद होता है। अपेक्षातन्तु के विच्छेद का तात्पर्य है कि समतानिष्पन्न योगी को संसार में किसी प्रकार के सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा
1. 'विआणिआ अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो'।
छा.-विज्ञायात्मानमात्मना यो रागद्वेषयोः समः स पूज्यः।
(दशवै. अ. 9/11)