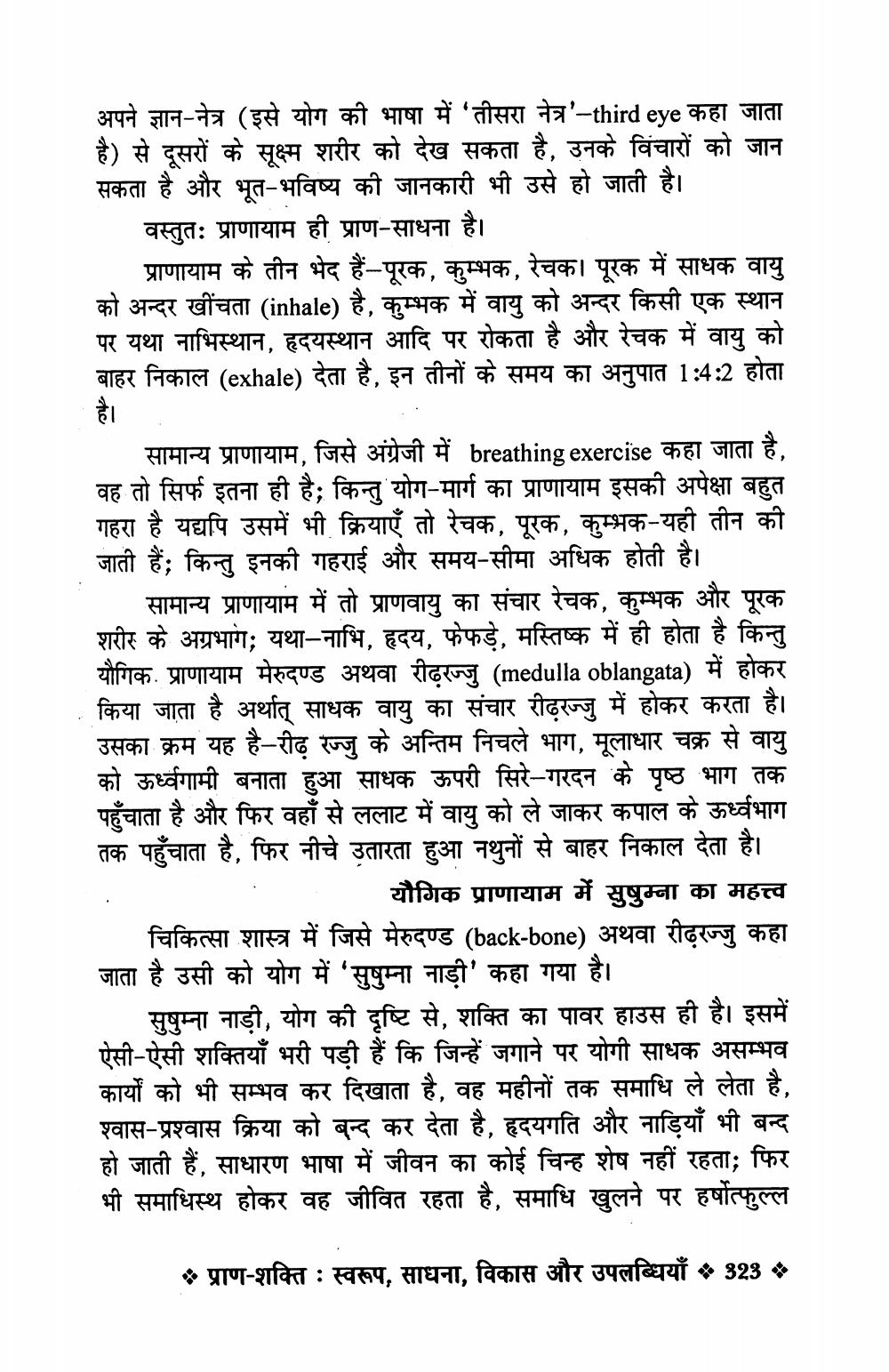________________
अपने ज्ञान-नेत्र (इसे योग की भाषा में 'तीसरा नेत्र'-third eye कहा जाता है) से दूसरों के सूक्ष्म शरीर को देख सकता है, उनके विचारों को जान सकता है और भूत-भविष्य की जानकारी भी उसे हो जाती है।
वस्तुतः प्राणायाम ही प्राण-साधना है।
प्राणायाम के तीन भेद हैं-पूरक, कुम्भक, रेचक। पूरक में साधक वायु को अन्दर खींचता (inhale) है, कुम्भक में वायु को अन्दर किसी एक स्थान पर यथा नाभिस्थान, हृदयस्थान आदि पर रोकता है और रेचक में वायु को बाहर निकाल (exhale) देता है, इन तीनों के समय का अनुपात 1:4:2 होता
सामान्य प्राणायाम, जिसे अंग्रेजी में breathing exercise कहा जाता है, वह तो सिर्फ इतना ही है; किन्तु योग-मार्ग का प्राणायाम इसकी अपेक्षा बहुत गहरा है यद्यपि उसमें भी क्रियाएँ तो रेचक, पूरक, कुम्भक-यही तीन की जाती हैं; किन्तु इनकी गहराई और समय-सीमा अधिक होती है।
सामान्य प्राणायाम में तो प्राणवायु का संचार रेचक, कुम्भक और पूरक शरीर के अग्रभाग; यथा-नाभि, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क में ही होता है किन्तु यौगिक. प्राणायाम मेरुदण्ड अथवा रीढ़रज्जु (medulla oblangata) में होकर किया जाता है अर्थात् साधक वायु का संचार रीढरज्जु में होकर करता है। उसका क्रम यह है-रीढ़ रज्जु के अन्तिम निचले भाग, मूलाधार चक्र से वायु को ऊर्ध्वगामी बनाता हुआ साधक ऊपरी सिरे-गरदन के पृष्ठ भाग तक पहुँचाता है और फिर वहाँ से ललाट में वायु को ले जाकर कपाल के ऊर्ध्वभाग तक पहुँचाता है, फिर नीचे उतारता हुआ नथुनों से बाहर निकाल देता है।
यौगिक प्राणायाम में सुषुम्ना का महत्त्व चिकित्सा शास्त्र में जिसे मेरुदण्ड (back-bone) अथवा रीढ़रज्जु कहा जाता है उसी को योग में 'सुषुम्ना नाड़ी' कहा गया है।
सुषुम्ना नाड़ी, योग की दृष्टि से, शक्ति का पावर हाउस ही है। इसमें ऐसी-ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि जिन्हें जगाने पर योगी साधक असम्भव कार्यों को भी सम्भव कर दिखाता है, वह महीनों तक समाधि ले लेता है, श्वास-प्रश्वास क्रिया को बन्द कर देता है, हृदयगति और नाड़ियाँ भी बन्द हो जाती हैं, साधारण भाषा में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं रहता; फिर भी समाधिस्थ होकर वह जीवित रहता है, समाधि खुलने पर हर्षोत्फुल्ल
* प्राण-शक्ति : स्वरूप, साधना, विकास और उपलब्धियाँ * 323 *