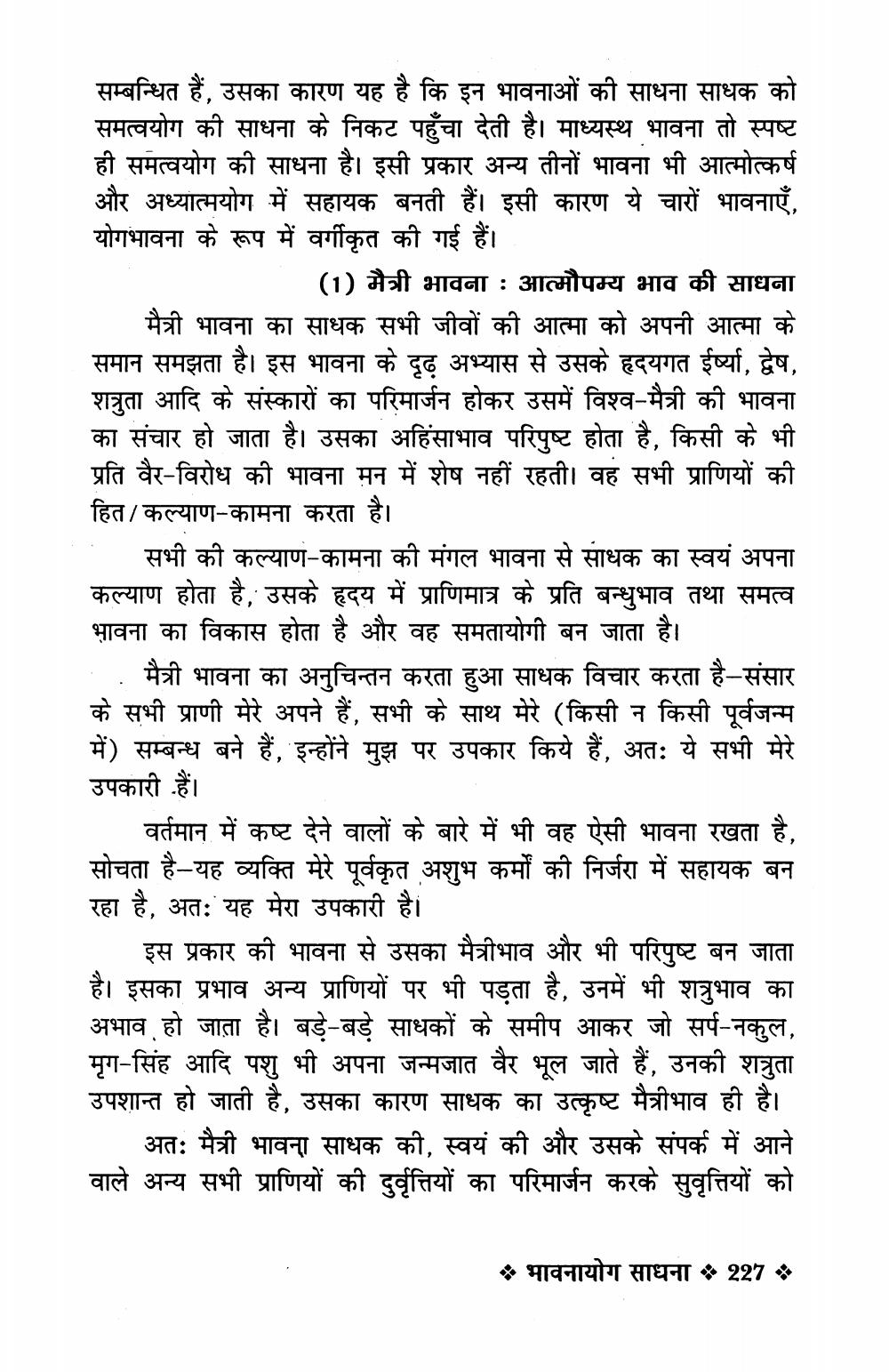________________
सम्बन्धित हैं, उसका कारण यह है कि इन भावनाओं की साधना साधक को समत्वयोग की साधना के निकट पहुँचा देती है। माध्यस्थ भावना तो स्पष्ट ही समत्वयोग की साधना है। इसी प्रकार अन्य तीनों भावना भी आत्मोत्कर्ष
और अध्यात्मयोग में सहायक बनती हैं। इसी कारण ये चारों भावनाएँ, योगभावना के रूप में वर्गीकृत की गई हैं।
(1) मैत्री भावना : आत्मौपम्य भाव की साधना मैत्री भावना का साधक सभी जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है। इस भावना के दृढ़ अभ्यास से उसके हृदयगत ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता आदि के संस्कारों का परिमार्जन होकर उसमें विश्व-मैत्री की भावना का संचार हो जाता है। उसका अहिंसाभाव परिपुष्ट होता है, किसी के भी प्रति वैर-विरोध की भावना मन में शेष नहीं रहती। वह सभी प्राणियों की हित / कल्याण-कामना करता है।
सभी की कल्याण-कामना की मंगल भावना से साधक का स्वयं अपना कल्याण होता है, उसके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति बन्धुभाव तथा समत्व भावना का विकास होता है और वह समतायोगी बन जाता है। .. मैत्री भावना का अनुचिन्तन करता हुआ साधक विचार करता है-संसार के सभी प्राणी मेरे अपने हैं, सभी के साथ मेरे (किसी न किसी पूर्वजन्म में) सम्बन्ध बने हैं, इन्होंने मुझ पर उपकार किये हैं, अतः ये सभी मेरे उपकारी हैं।
वर्तमान में कष्ट देने वालों के बारे में भी वह ऐसी भावना रखता है, सोचता है-यह व्यक्ति मेरे पूर्वकृत अशुभ कर्मों की निर्जरा में सहायक बन रहा है, अतः यह मेरा उपकारी है।
इस प्रकार की भावना से उसका मैत्रीभाव और भी परिपुष्ट बन जाता है। इसका प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी पड़ता है, उनमें भी शत्रुभाव का अभाव हो जाता है। बड़े-बड़े साधकों के समीप आकर जो सर्प-नकुल, मृग-सिंह आदि पशु भी अपना जन्मजात वैर भूल जाते हैं, उनकी शत्रुता उपशान्त हो जाती है, उसका कारण साधक का उत्कृष्ट मैत्रीभाव ही है।
अतः मैत्री भावना साधक की, स्वयं की और उसके संपर्क में आने वाले अन्य सभी प्राणियों की दुर्वृत्तियों का परिमार्जन करके सुवृत्तियों को
* भावनायोग साधना * 227*