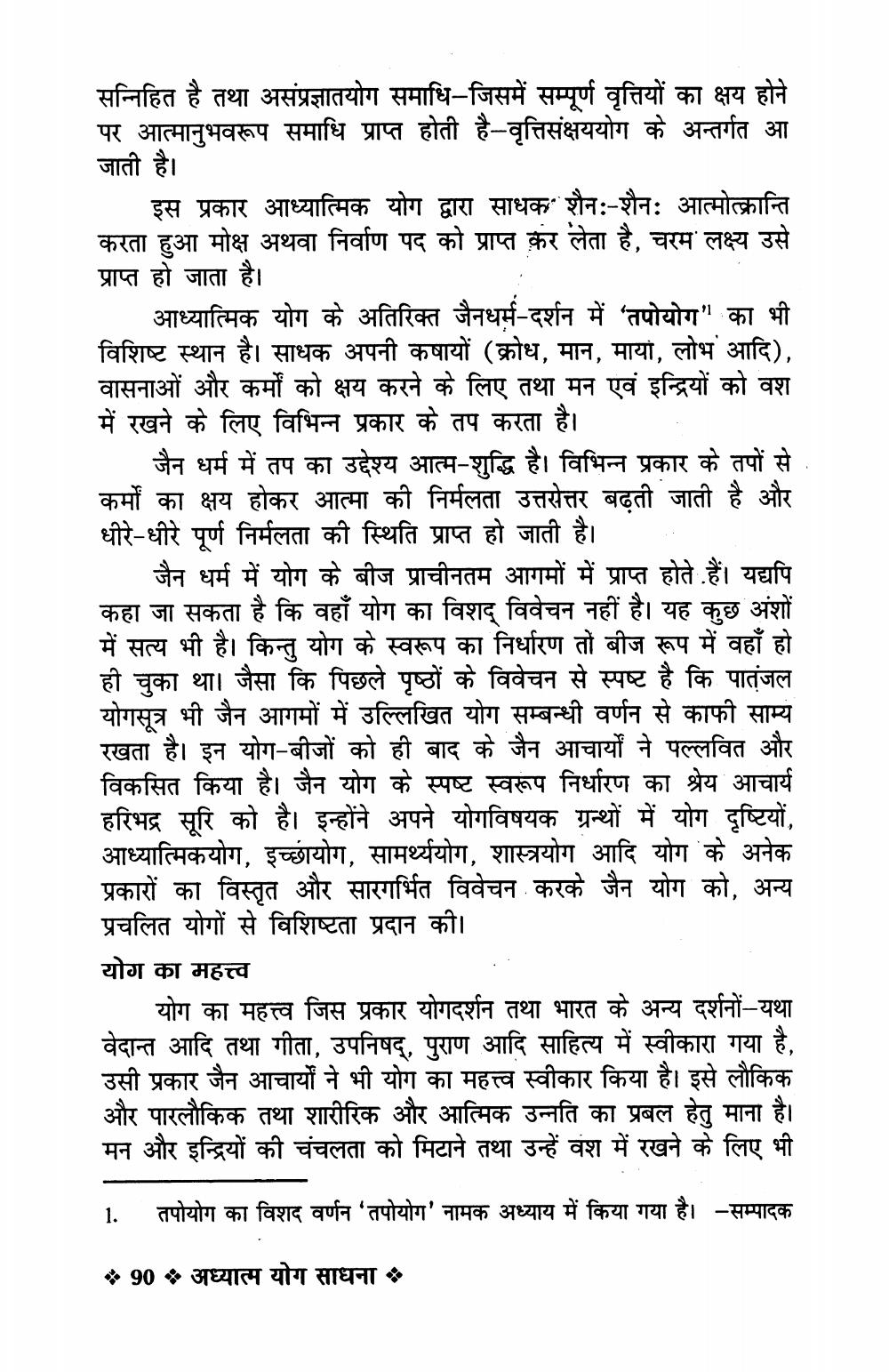________________
सन्निहित है तथा असंप्रज्ञातयोग समाधि-जिसमें सम्पूर्ण वृत्तियों का क्षय होने पर आत्मानुभवरूप समाधि प्राप्त होती है-वृत्तिसंक्षययोग के अन्तर्गत आ जाती है।
इस प्रकार आध्यात्मिक योग द्वारा साधक शैनः-शैनः आत्मोत्क्रान्ति करता हुआ मोक्ष अथवा निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, चरम लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाता है।
आध्यात्मिक योग के अतिरिक्त जैनधर्म-दर्शन में 'तपोयोग" का भी विशिष्ट स्थान है। साधक अपनी कषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ आदि), वासनाओं और कर्मों को क्षय करने के लिए तथा मन एवं इन्द्रियों को वश में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तप करता है।
जैन धर्म में तप का उद्देश्य आत्म-शुद्धि है। विभिन्न प्रकार के तपों से . कर्मों का क्षय होकर आत्मा की निर्मलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और धीरे-धीरे पूर्ण निर्मलता की स्थिति प्राप्त हो जाती है।
जैन धर्म में योग के बीज प्राचीनतम आगमों में प्राप्त होते हैं। यद्यपि कहा जा सकता है कि वहाँ योग का विशद् विवेचन नहीं है। यह कुछ अंशों में सत्य भी है। किन्तु योग के स्वरूप का निर्धारण तो बीज रूप में वहाँ हो ही चुका था। जैसा कि पिछले पृष्ठों के विवेचन से स्पष्ट है कि पातंजल योगसूत्र भी जैन आगमों में उल्लिखित योग सम्बन्धी वर्णन से काफी साम्य रखता है। इन योग-बीजों को ही बाद के जैन आचार्यों ने पल्लवित और विकसित किया है। जैन योग के स्पष्ट स्वरूप निर्धारण का श्रेय आचार्य हरिभद्र सूरि को है। इन्होंने अपने योगविषयक ग्रन्थों में योग दृष्टियों, आध्यात्मिकयोग, इच्छायोग, सामर्थ्ययोग, शास्त्रयोग आदि योग के अनेक प्रकारों का विस्तृत और सारगर्भित विवेचन करके जैन योग को, अन्य प्रचलित योगों से विशिष्टता प्रदान की। योग का महत्त्व
___ योग का महत्त्व जिस प्रकार योगदर्शन तथा भारत के अन्य दर्शनों-यथा वेदान्त आदि तथा गीता, उपनिषद्, पुराण आदि साहित्य में स्वीकारा गया है, उसी प्रकार जैन आचार्यों ने भी योग का महत्त्व स्वीकार किया है। इसे लौकिक
और पारलौकिक तथा शारीरिक और आत्मिक उन्नति का प्रबल हेतु माना है। मन और इन्द्रियों की चंचलता को मिटाने तथा उन्हें वंश में रखने के लिए भी
1. तपोयोग का विशद वर्णन 'तपोयोग' नामक अध्याय में किया गया है। -सम्पादक
* 90 * अध्यात्म योग साधना *