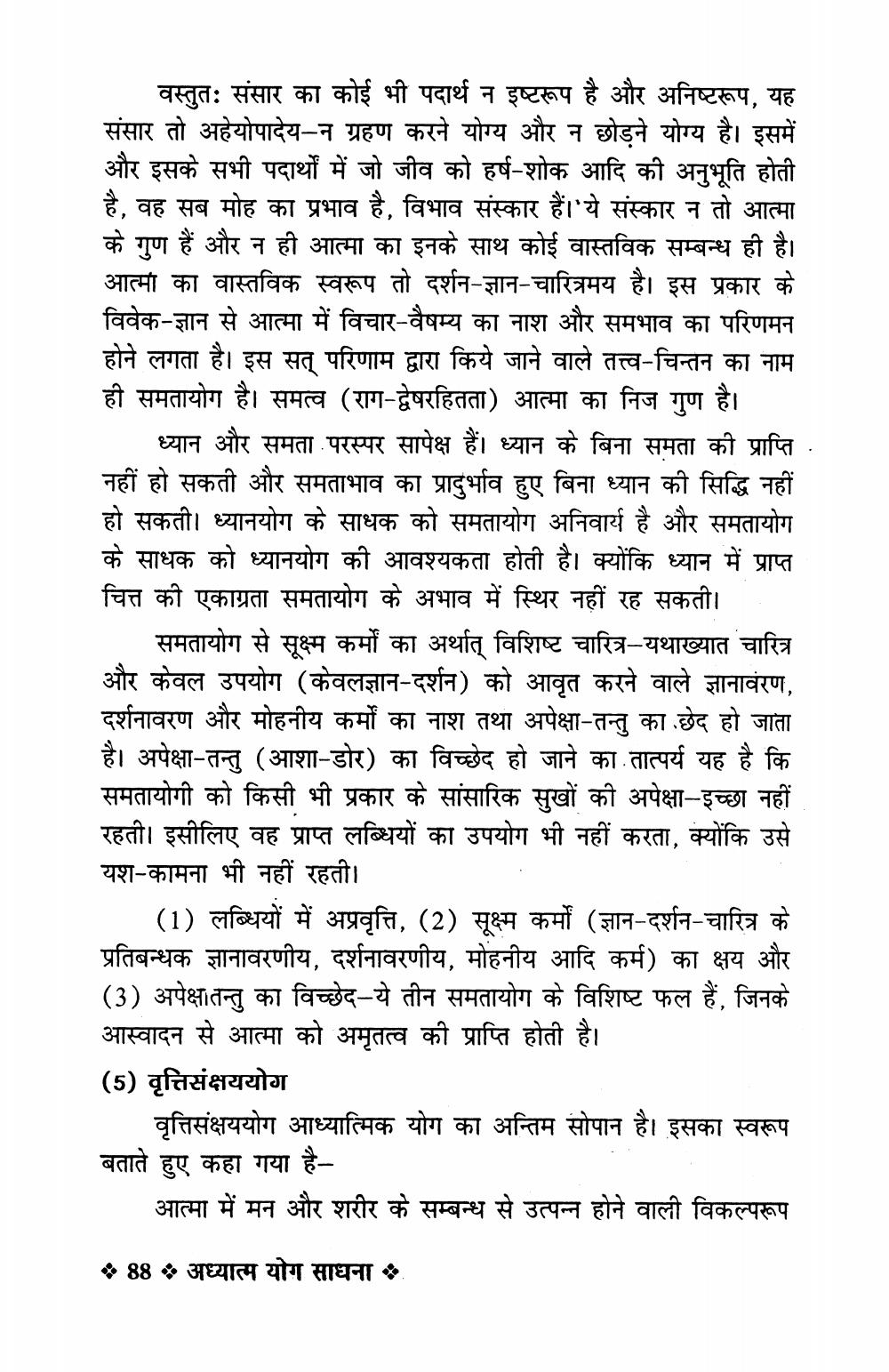________________
वस्तुतः संसार का कोई भी पदार्थ न इष्टरूप है और अनिष्टरूप, यह संसार तो अहेयोपादेय-न ग्रहण करने योग्य और न छोड़ने योग्य है। इसमें
और इसके सभी पदार्थों में जो जीव को हर्ष-शोक आदि की अनुभूति होती है, वह सब मोह का प्रभाव है, विभाव संस्कार हैं। ये संस्कार न तो आत्मा के गुण हैं और न ही आत्मा का इनके साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध ही है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय है। इस प्रकार के विवेक-ज्ञान से आत्मा में विचार-वैषम्य का नाश और समभाव का परिणमन होने लगता है। इस सत् परिणाम द्वारा किये जाने वाले तत्त्व-चिन्तन का नाम ही समतायोग है। समत्व (राग-द्वेषरहितता) आत्मा का निज गुण है।
ध्यान और समता परस्पर सापेक्ष हैं। ध्यान के बिना समता की प्राप्ति . नहीं हो सकती और समताभाव का प्रादुर्भाव हुए बिना ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। ध्यानयोग के साधक को समतायोग अनिवार्य है और समतायोग के साधक को ध्यानयोग की आवश्यकता होती है। क्योंकि ध्यान में प्राप्त चित्त की एकाग्रता समतायोग के अभाव में स्थिर नहीं रह सकती।
समतायोग से सूक्ष्म कर्मों का अर्थात् विशिष्ट चारित्र-यथाख्यात चारित्र और केवल उपयोग (केवलज्ञान-दर्शन) को आवृत करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्मों का नाश तथा अपेक्षा-तन्तु का छेद हो जाता है। अपेक्षा-तन्तु (आशा-डोर) का विच्छेद हो जाने का तात्पर्य यह है कि समतायोगी को किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों की अपेक्षा-इच्छा नहीं रहती। इसीलिए वह प्राप्त लब्धियों का उपयोग भी नहीं करता, क्योंकि उसे यश-कामना भी नहीं रहती।
(1) लब्धियों में अप्रवृत्ति, (2) सूक्ष्म कर्मों (ज्ञान-दर्शन-चारित्र के प्रतिबन्धक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय आदि कर्म) का क्षय और (3) अपेक्षातन्तु का विच्छेद-ये तीन समतायोग के विशिष्ट फल हैं, जिनके आस्वादन से आत्मा को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। (5) वृत्तिसंक्षययोग
वृत्तिसंक्षययोग आध्यात्मिक योग का अन्तिम सोपान है। इसका स्वरूप बताते हुए कहा गया है
आत्मा में मन और शरीर के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली विकल्परूप
688 * अध्यात्म योग साधना.