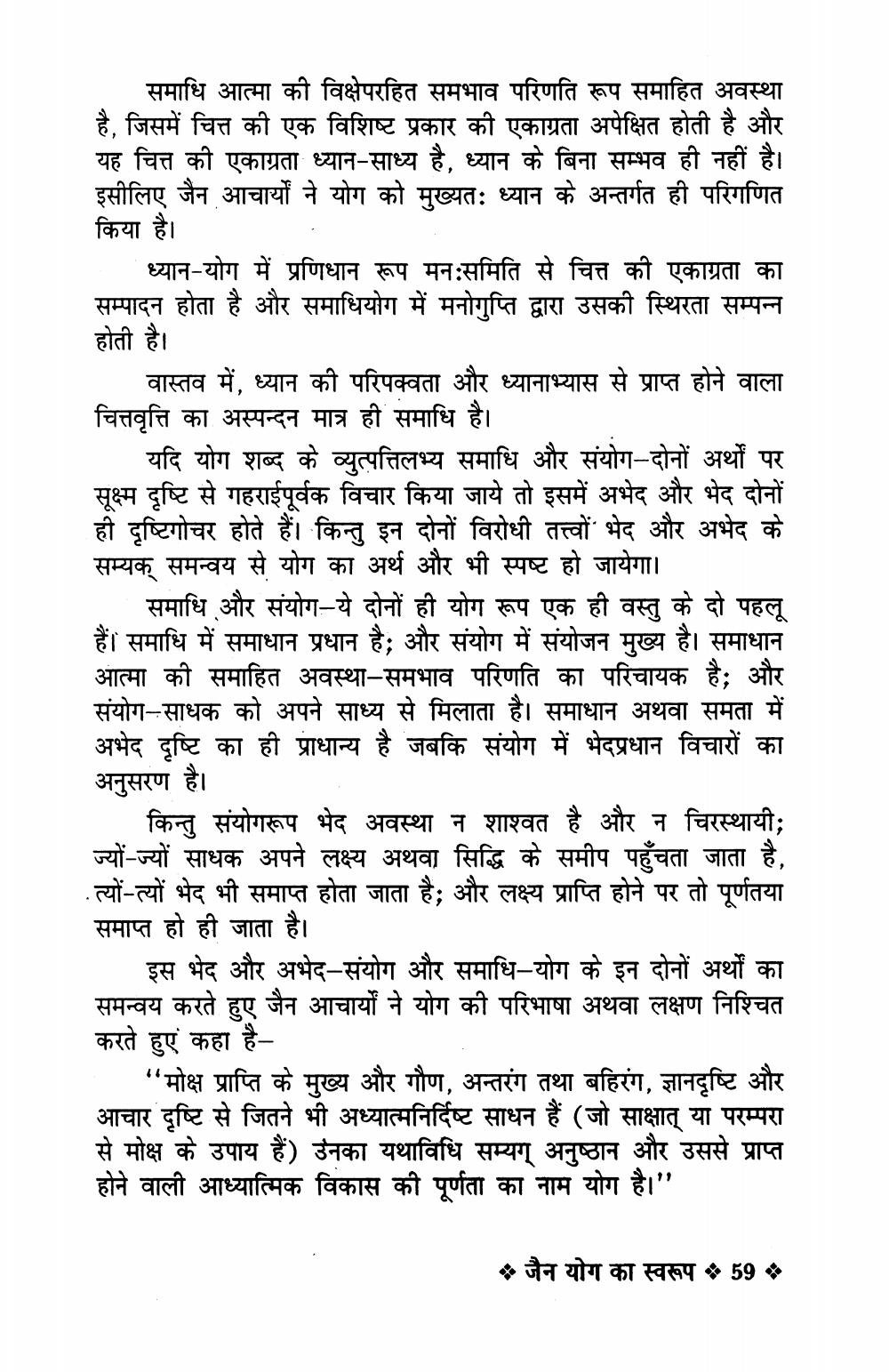________________
समाधि आत्मा की विक्षेपरहित समभाव परिणति रूप समाहित अवस्था है, जिसमें चित्त की एक विशिष्ट प्रकार की एकाग्रता अपेक्षित होती है और यह चित्त की एकाग्रता ध्यान-साध्य है, ध्यान के बिना सम्भव ही नहीं है। इसीलिए जैन आचार्यों ने योग को मुख्यतः ध्यान के अन्तर्गत ही परिगणित किया है।
ध्यान - योग में प्रणिधान रूप मनःसमिति से चित्त की एकाग्रता का सम्पादन होता है और समाधियोग में मनोगुप्ति द्वारा उसकी स्थिरता सम्पन्न होती है।
वास्तव में, ध्यान की परिपक्वता और ध्यानाभ्यास से प्राप्त होने वाला चित्तवृत्ति का अस्पन्दन मात्र ही समाधि है।
यदि योग शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य समाधि और संयोग- दोनों अर्थों पर सूक्ष्म दृष्टि से गहराईपूर्वक विचार किया जाये तो इसमें अभेद और भेद दोनों ही दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु इन दोनों विरोधी तत्त्वों भेद और अभेद के सम्यक् समन्वय से योग का अर्थ और भी स्पष्ट हो जायेगा ।
समाधि और संयोग- ये दोनों ही योग रूप एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। समाधि में समाधान प्रधान है; और संयोग में संयोजन मुख्य है। समाधान आत्मा की समाहित अवस्था - समभाव परिणति का परिचायक है; और संयोग-साधक को अपने साध्य से मिलाता है। समाधान अथवा समता में अभेद दृष्टि का ही प्राधान्य है जबकि संयोग में भेदप्रधान विचारों का अनुसरण है।
किन्तु संयोगरूप भेद अवस्था न शाश्वत है और न चिरस्थायी; ज्यों-ज्यों साधक अपने लक्ष्य अथवा सिद्धि के समीप पहुँचता जाता है, . त्यों-त्यों भेद भी समाप्त होता जाता है; और लक्ष्य प्राप्ति होने पर तो पूर्णतया समाप्त हो ही जाता है।
इस भेद और अभेद-संयोग और समाधि - योग के इन दोनों अर्थों का समन्वय करते हुए जैन आचार्यों ने योग की परिभाषा अथवा लक्षण निश्चित करते हुए कहा है
"मोक्ष प्राप्ति के मुख्य और गौण, अन्तरंग तथा बहिरंग, ज्ञानदृष्टि और आचार दृष्टि से जितने भी अध्यात्मनिर्दिष्ट साधन हैं (जो साक्षात् या परम्परा से मोक्ष के उपाय हैं) उनका यथाविधि सम्यग् अनुष्ठान और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक विकास की पूर्णता का नाम योग है । "
जैन योग का स्वरूप 59