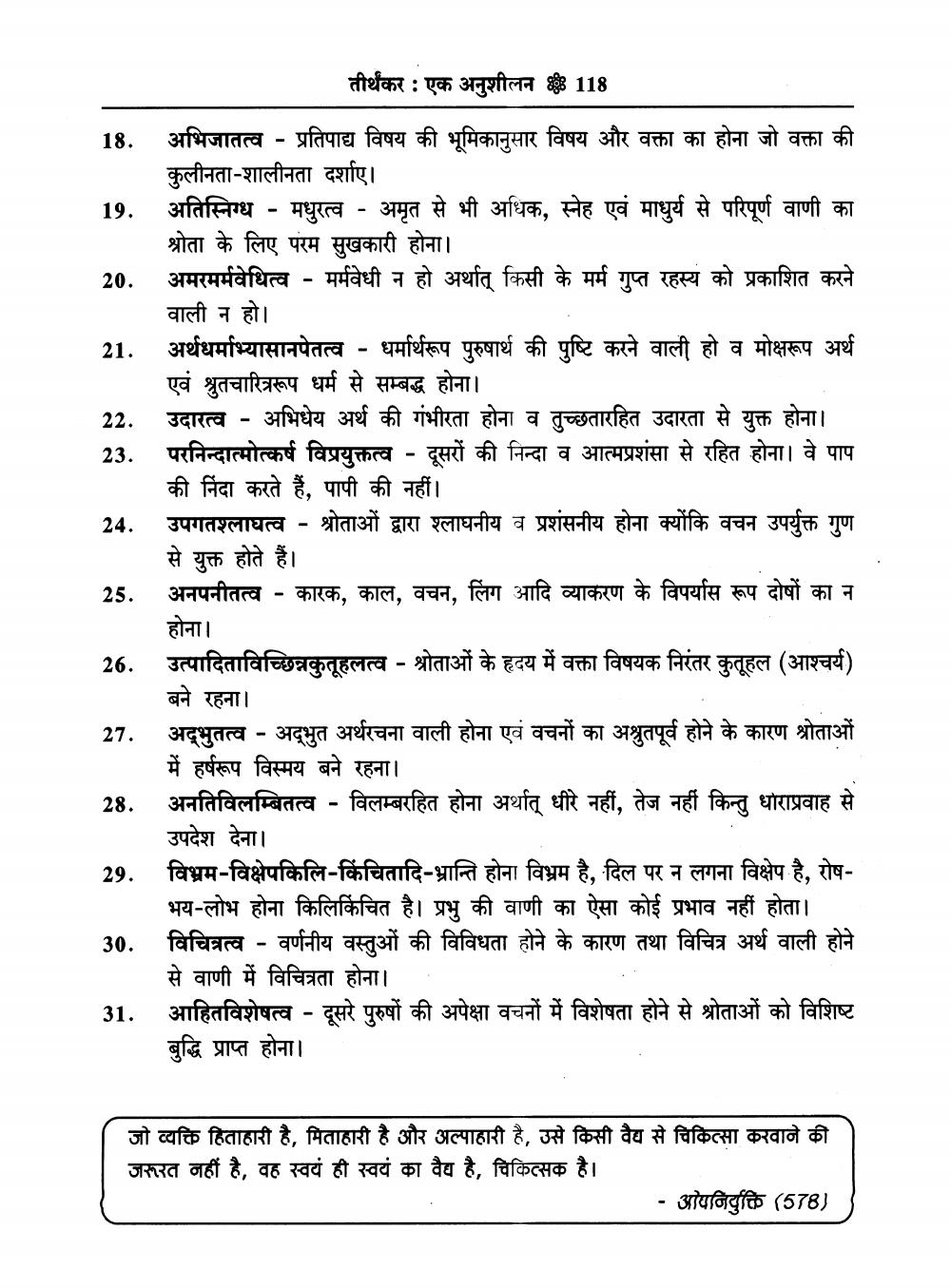________________
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
तीर्थंकर : एक अनुशीलन 118
अभिजातत्व प्रतिपाद्य विषय की भूमिकानुसार विषय और वक्ता का होना जो वक्ता की कुलीनता - शालीनता दर्शाए ।
अतिस्निग्ध - मधुरत्व - अमृत से भी अधिक, स्नेह एवं माधुर्य से परिपूर्ण वाणी का श्रोता के लिए परम सुखकारी होना ।
अमरमर्मवेधित्व - मर्मवेधी न हो अर्थात् किसी के मर्म गुप्त रहस्य को प्रकाशित करने वाली न हो ।
31.
26. उत्पादिताविच्छिन्नकुतूहलत्व - श्रोताओं के हृदय में वक्ता विषयक निरंतर कुतूहल (आश्चर्य)
बने रहना ।
अद्भुतत्व - अद्भुत अर्थरचना वाली होना एवं वचनों का अश्रुतपूर्व होने के कारण श्रोताओं में हर्षरूप विस्मय बने रहना ।
अनतिविलम्बितत्व - विलम्बरहित होना अर्थात् धीरे नहीं, तेज नहीं किन्तु धाराप्रवाह उपदेश देना ।
-
अर्थधर्माभ्यासानपेतत्व - धर्मार्थरूप पुरुषार्थ की पुष्टि करने वाली हो व मोक्षरूप अर्थ एवं श्रुतचारित्ररूप धर्म से सम्बद्ध होना ।
उदारत्व अभिधेय अर्थ की गंभीरता होना व तुच्छतारहित उदारता से युक्त होना । परनिन्दात्मोत्कर्ष विप्रयुक्तत्व - दूसरों की निन्दा व आत्मप्रशंसा से रहित होना । वे पाप की निंदा करते हैं, पापी की नहीं ।
श्रोताओं द्वारा श्लाघनीय व प्रशंसनीय होना क्योंकि वचन उपर्युक्त गुण
-
उपगतश्लाघत्व
से युक्त होते हैं ।
अनपनीतत्व - कारक, काल, वचन, लिंग आदि व्याकरण के विपर्यास रूप दोषों का न
होना ।
-
विभ्रम-विक्षेपकिलि-किंचितादि - भ्रान्ति होना विभ्रम है, दिल पर न लगना विक्षेप है, रोषभय-लोभ होना किलिकिंचित है। प्रभु की वाणी का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता । विचित्रत्व - वर्णनीय वस्तुओं की विविधता होने के कारण तथा विचित्र अर्थ वाली से वाणी में विचित्रता होना ।
आहित विशेषत्व - दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वचनों में विशेषता होने से श्रोताओं को विशिष्ट बुद्धि प्राप्त होना ।
जो व्यक्ति हिताहारी है, मिताहारी है और अल्पाहारी है, उसे किसी वैद्य से चिकित्सा करवाने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही स्वयं का वैद्य है, चिकित्सक है।
ओपनियुक्ति (578)