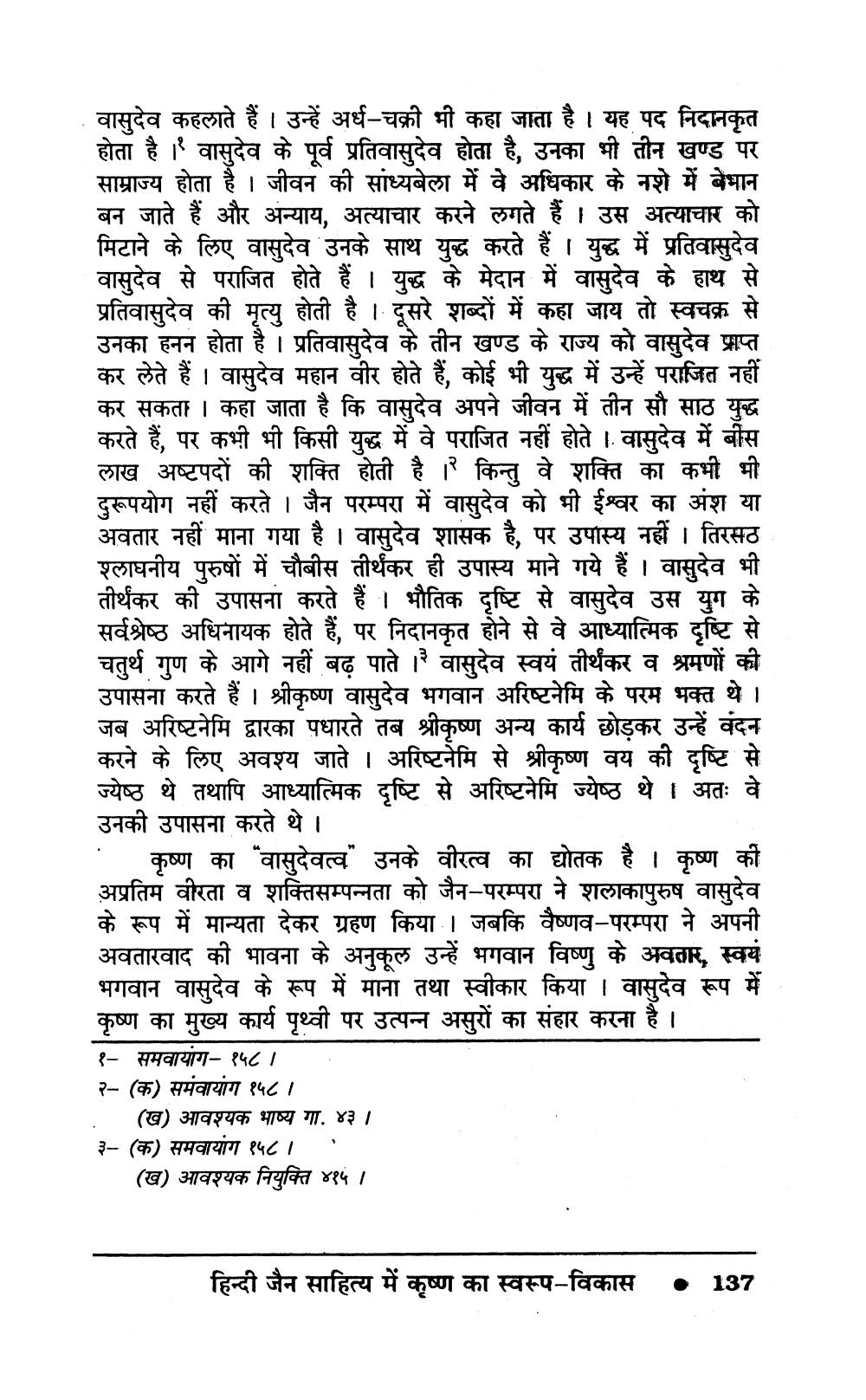________________
वासुदेव कहलाते हैं । उन्हें अर्ध-चक्री भी कहा जाता है । यह पद निदानकृत होता है । वासुदेव के पूर्व प्रतिवासुदेव होता है, उनका भी तीन खण्ड पर साम्राज्य होता है । जीवन की सांध्यबेला में वे अधिकार के नशे में बेभान बन जाते हैं और अन्याय, अत्याचार करने लगते हैं । उस अत्याचार को मिटाने के लिए वासुदेव उनके साथ युद्ध करते हैं । युद्ध में प्रतिवासुदेव वासुदेव से पराजित होते हैं । युद्ध के मेदान में वासुदेव के हाथ से प्रतिवासुदेव की मृत्यु होती है । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो स्वचक्र से उनका हनन होता है । प्रतिवासुदेव के तीन खण्ड के राज्य को वासुदेव प्राप्त कर लेते हैं । वासुदेव महान वीर होते हैं, कोई भी युद्ध में उन्हें पराजित नहीं कर सकता । कहा जाता है कि वासुदेव अपने जीवन में तीन सौ साठ युद्ध करते हैं, पर कभी भी किसी युद्ध में वे पराजित नहीं होते । वासुदेव में बीस लाख अष्टपदों की शक्ति होती है । किन्तु वे शक्ति का कभी भी दुरूपयोग नहीं करते । जैन परम्परा में वासुदेव को भी ईश्वर का अंश या अवतार नहीं माना गया है । वासुदेव शासक है, पर उपास्य नहीं । तिरसठ श्लाघनीय पुरुषों में चौबीस तीर्थंकर ही उपास्य माने गये हैं । वासुदेव भी तीर्थंकर की उपासना करते हैं । भौतिक दृष्टि से वासुदेव उस युग के सर्वश्रेष्ठ अधिनायक होते हैं, पर निदानकृत होने से वे आध्यात्मिक दृष्टि से चतुर्थ गुण के आगे नहीं बढ़ पाते । वासुदेव स्वयं तीर्थंकर व श्रमणों की उपासना करते हैं । श्रीकृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि के परम भक्त थे । जब अरिष्टनेमि द्वारका पधारते तब श्रीकृष्ण अन्य कार्य छोड़कर उन्हें वंदन करने के लिए अवश्य जाते । अरिष्टनेमि से श्रीकृष्ण वय की दृष्टि से ज्येष्ठ थे तथापि आध्यात्मिक दृष्टि से अरिष्टनेमि ज्येष्ठ थे । अतः वे उनकी उपासना करते थे । - कृष्ण का वासुदेवत्व उनके वीरत्व का द्योतक है । कृष्ण की अप्रतिम वीरता व शक्तिसम्पन्नता को जैन-परम्परा ने शलाकापुरुष वासुदेव के रूप में मान्यता देकर ग्रहण किया । जबकि वैष्णव-परम्परा ने अपनी अवतारवाद की भावना के अनुकूल उन्हें भगवान विष्णु के अवतार, स्वयं भगवान वासुदेव के रूप में माना तथा स्वीकार किया । वासुदेव रूप में कृष्ण का मुख्य कार्य पृथ्वी पर उत्पन्न असुरों का संहार करना है। १- समवायांग- १५८ । २- (क) समंवायांग १५४। . (ख) आवश्यक भाष्य गा. ४३ । ३- (क) समवायांग १५८ । ।
(ख) आवश्यक नियुक्ति ४१५ ।
हिन्दी जैन साहित्य में कृष्ण का स्वरूप-विकास • 137