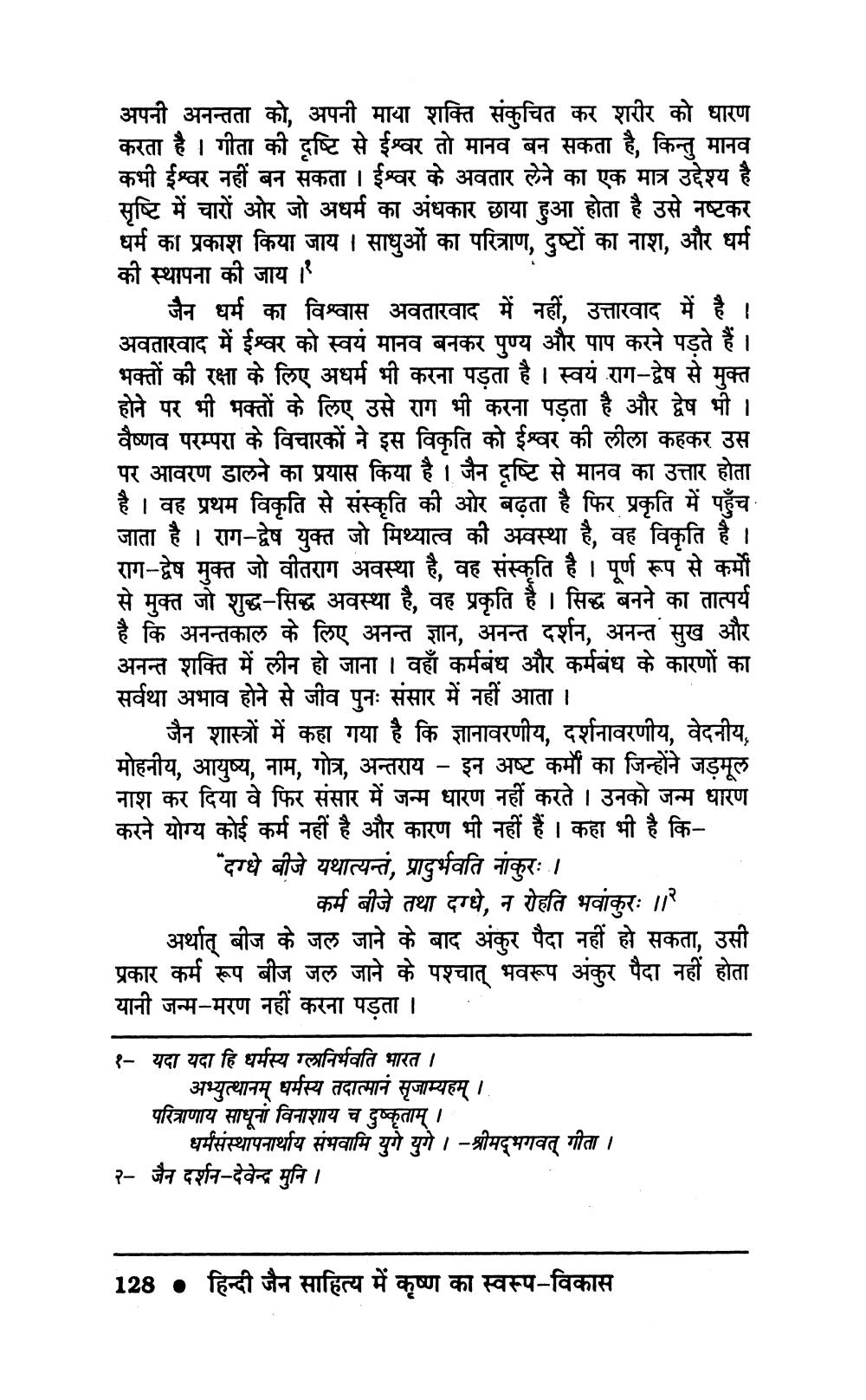________________
अपनी अनन्तता को, अपनी माया शक्ति संकुचित कर शरीर को धारण करता है । गीता की दृष्टि से ईश्वर तो मानव बन सकता है, किन्तु मानव कभी ईश्वर नहीं बन सकता । ईश्वर के अवतार लेने का एक मात्र उद्देश्य है सृष्टि में चारों ओर जो अधर्म का अंधकार छाया हुआ होता है उसे नष्टकर धर्म का प्रकाश किया जाय । साधुओं का परित्राण, दुष्टों का नाश, और धर्म की स्थापना की जाय ।
जैन धर्म का विश्वास अवतारवाद में नहीं, उत्तारवाद में है । अवतारवाद में ईश्वर को स्वयं मानव बनकर पुण्य और पाप करने पड़ते हैं । भक्तों की रक्षा के लिए अधर्म भी करना पड़ता है । स्वयं राग-द्वेष से मुक्त होने पर भी भक्तों के लिए उसे राग भी करना पड़ता है और द्वेष भी । वैष्णव परम्परा के विचारकों ने इस विकृति को ईश्वर की लीला कहकर उस पर आवरण डालने का प्रयास किया है । जैन दृष्टि से मानव का उत्तार होता है । वह प्रथम विकृति से संस्कृति की ओर बढ़ता है फिर प्रकृति में पहुँच जाता है । राग-द्वेष युक्त जो मिथ्यात्व की अवस्था है, वह विकृति है । राग-द्वेष मुक्त जो वीतराग अवस्था है, वह संस्कृति है । पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त जो शुद्ध-सिद्ध अवस्था है, वह प्रकृति है । सिद्ध बनने का तात्पर्य है कि अनन्तकाल के लिए अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति में लीन हो जाना । वहाँ कर्मबंध और कर्मबंध के कारणों का सर्वथा अभाव होने से जीव पुनः संसार में नहीं आता।
जैन शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अन्तराय – इन अष्ट कर्मों का जिन्होंने जड़मूल नाश कर दिया वे फिर संसार में जन्म धारण नहीं करते । उनको जन्म धारण करने योग्य कोई कर्म नहीं है और कारण भी नहीं हैं । कहा भी है किदग्धे बीजे यथात्यन्तं, प्रादुर्भवति नांकुरः ।
कर्म बीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांकुरः ॥२ अर्थात् बीज के जल जाने के बाद अंकुर पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्म रूप बीज जल जाने के पश्चात् भवरूप अंकुर पैदा नहीं होता यानी जन्म-मरण नहीं करना पड़ता।
१- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । ___अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।।
____धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । -श्रीमद्भगवत् गीता । २- जैन दर्शन-देवेन्द्र मुनि ।
128 • हिन्दी जैन साहित्य में कृष्ण का स्वरूप-विकास