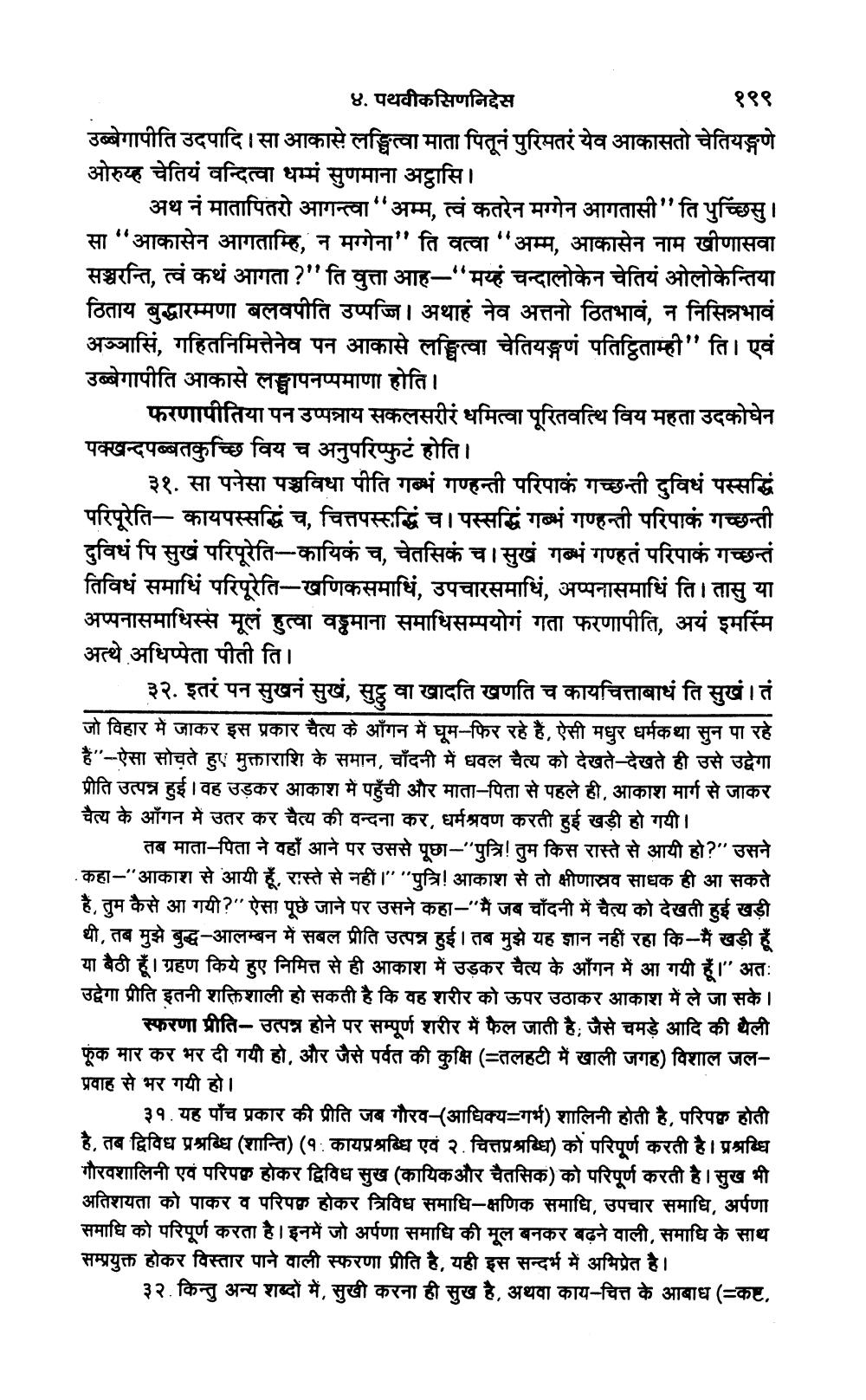________________
४. पथवीकसिणनिद्देस
१९९
उब्बेगापीति उदपादि । सा आकासे लङ्घित्वा माता पितूनं पुरिमतरं येव आकासतो चेतियङ्गणे ओरुव्ह चेतियं वन्दित्वा धम्मं सुणमाना अट्ठासि ।
अथ नं मातापितरो आगन्त्वा "अम्म, त्वं कतरेन मग्गेन आगतासी" ति पुच्छिसु । सा " आकासेन आगताम्हि, न मग्गेना" ति वत्वा "अम्म, आकासेन नाम खीणासवा सञ्चरन्ति, त्वं कथं आगता ?" ति वुत्ता आह- " मय्हं चन्दालोकेन चेतियं ओलोकेन्तिया ठिताय बुद्धारम्मणा बलवपीति उप्पज्जि । अथाहं नेव अत्तनो ठितभावं, न निसिन्नभावं अञ्ञासिं, गहितनिमित्तेनेव पन आकासे लङ्घित्वा चेतियङ्गणं पतिट्ठिताम्ही" ति । एवं उब्बेगापीति आकासे लङ्घापनप्पमाणा होति ।
फरणापीतिया पन उप्पन्नाय सकलसरीरं धमित्वा पूरितवत्थि विय महता उदकोघेन पक्खन्दपब्बतकुच्छि विय च अनुपरिप्फुटं होति ।
३१. सा पनेसा पञ्चविधा पीति गब्धं गण्हन्ती परिपाकं गच्छन्ती दुविधं पस्सद्धिं परिपूरेति — कायपस्सद्धिं च, चित्तपस्सद्धिं च । पस्सद्धिं गब्धं गण्हन्ती परिपाकं गच्छन्ती दुविधं पि सुखं परिपूरेति - कायिकं च, चेतसिकं च । सुखं गब्धं गण्हतं परिपाकं गच्छन्तं तिविधं समाधिं परिपूरेति - खणिकसमाधिं, उपचारसमाधिं, अप्पनासमाधिं ति । तासु या अप्पनासमाधिस्स मूलं हुत्वा वड्डमाना समाधिसम्पयोगं गता फरणापीति, अयं इमस्मि अत्थे अधिप्पेता पीती ति ।
३२. इतरं पन सुखनं सुखं, सुट्टु वा खादति खणति च कायचित्ताबाधं ति सुखं । तं जो विहार में जाकर इस प्रकार चैत्य के आँगन में घूम-फिर रहे हैं, ऐसी मधुर धर्मकथा सुन पा रहे हैं" - ऐसा सोचते हुए मुक्ताराशि के समान, चाँदनी में धवल चैत्य को देखते-देखते ही उसे उद्वेगा प्रीति उत्पन्न हुई । वह उड़कर आकाश में पहुँची और माता-पिता से पहले ही, आकाश मार्ग से जाकर चैत्य के आँगन में उतर कर चैत्य की वन्दना कर, धर्मश्रवण करती हुई खड़ी हो गयी।
तब माता-पिता ने वहाँ आने पर उससे पूछा - "पुत्रि ! तुम किस रास्ते से आयी हो?" उसने . कहा- "आकाश से आयी हूँ, रास्ते से नहीं।" "पुत्रि ! आकाश से तो क्षीणास्रव साधक ही आ सकते हैं, तुम कैसे आ गयी?" ऐसा पूछे जाने पर उसने कहा- "मैं जब चाँदनी में चैत्य को देखती हुई खड़ी थी, तब मुझे बुद्ध - आलम्बन में सबल प्रीति उत्पन्न हुई। तब मुझे यह ज्ञान नहीं रहा कि मैं खड़ी हूँ या बैठी हूँ। ग्रहण किये हुए निमित्त से ही आकाश में उड़कर चैत्य के आँगन में आ गयी हूँ।" अतः उद्वेगा प्रीति इतनी शक्तिशाली हो सकती है। वह शरीर को ऊपर उठाकर आकाश में ले जा सके। स्फरणा प्रीति - उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर में फैल जाती है; जैसे चमड़े आदि की थैली फूंक मार कर भर दी गयी हो, और जैसे पर्वत की कुक्षि (= तलहटी में खाली जगह) विशाल जलप्रवाह से भर गयी हो ।
३१. यह पाँच प्रकार की प्रीति जब गौरव - ( आधिक्य = गर्भ) शालिनी होती है, परिपक्व होती है, तब द्विविध प्रश्रब्धि (शान्ति) (१: कायप्रश्रब्धि एवं २ चित्तप्रश्रब्धि) को परिपूर्ण करती है। प्रश्रब्धि गौरवशालिनी एवं परिपक्व होकर द्विविध सुख (कायिक और चैतसिक) को परिपूर्ण करती है। सुख भी अतिशयता को पाकर व परिपक्व होकर त्रिविध समाधि-क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि को परिपूर्ण करता है। इनमें जो अर्पणा समाधि की मूल बनकर बढ़ने वाली, समाधि के साथ सम्प्रयुक्त होकर विस्तार पाने वाली स्फरणा प्रीति है, यही इस सन्दर्भ में अभिप्रेत है।
३२. किन्तु अन्य शब्दों में, सुखी करना ही सुख है, अथवा काय-चित्त के आबाध (=कष्ट,