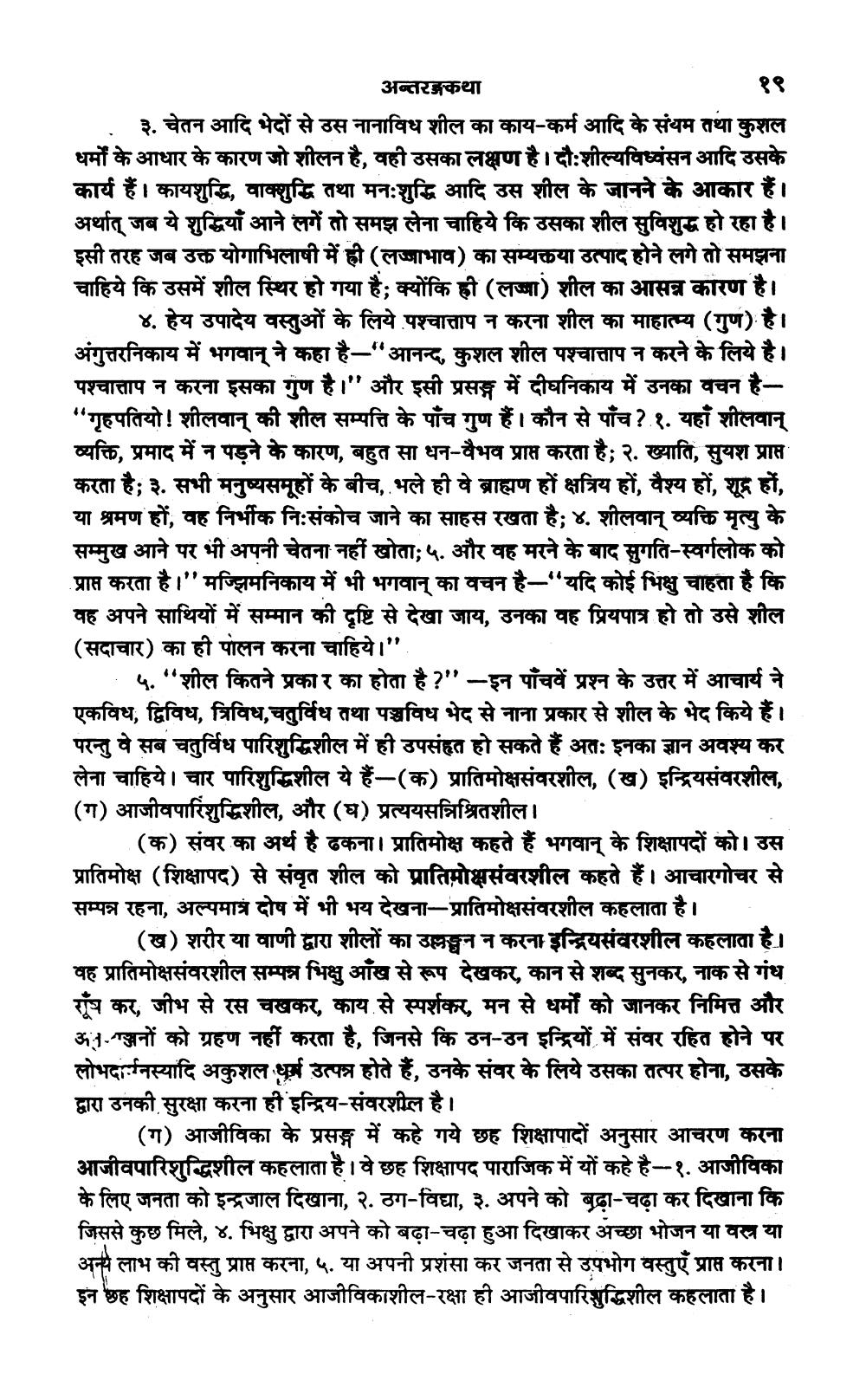________________
अन्तरङ्गकथा
३. चेतन आदि भेदों से उस नानाविध शील का काय-कर्म आदि के संयम तथा कुशल धर्मों के आधार के कारण जो शीलन है, वही उसका लक्षण है। दौःशील्यविध्वंसन आदि उसके कार्य हैं। कायशुद्धि, वाक्शुद्धि तथा मनःशुद्धि आदि उस शील के जानने के आकार हैं। अर्थात् जब ये शुद्धियाँ आने लगें तो समझ लेना चाहिये कि उसका शील सुविशुद्ध हो रहा है। इसी तरह जब उक्त योगाभिलाषी में ही (लज्जाभाव) का सम्यक्तया उत्पाद होने लगे तो समझना चाहिये कि उसमें शील स्थिर हो गया है; क्योंकि ही (लज्जा) शील का आसन्न कारण है।
४. हेय उपादेय वस्तुओं के लिये पश्चात्ताप न करना शील का माहात्म्य (गुण) है। अंगुत्तरनिकाय में भगवान् ने कहा है-"आनन्द, कुशल शील पश्चात्ताप न करने के लिये है। पश्चात्ताप न करना इसका गुण है।" और इसी प्रसङ्ग में दीघनिकाय में उनका वचन है"गृहपतियो! शीलवान् की शील सम्पत्ति के पाँच गुण हैं। कौन से पाँच?.१. यहाँ शीलवान् व्यक्ति, प्रमाद में न पड़ने के कारण, बहुत सा धन-वैभव प्राप्त करता है; २. ख्याति, सुयश प्राप्त करता है; ३. सभी मनुष्यसमूहों के बीच, भले ही वे ब्राह्मण हों क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, या श्रमण हों, वह निर्भीक निःसंकोच जाने का साहस रखता है; ४. शीलवान् व्यक्ति मृत्यु के सम्मुख आने पर भी अपनी चेतना नहीं खोता; ५. और वह मरने के बाद सुगति-स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।" मज्झिमनिकाय में भी भगवान् का वचन है-"यदि कोई भिक्षु चाहता है कि वह अपने साथियों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाय, उनका वह प्रियपात्र हो तो उसे शील (सदाचार) का ही पालन करना चाहिये।"
५. "शील कितने प्रकार का होता है?" -इन पाँचवें प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने एकविध, द्विविध, त्रिविध,चतुर्विध तथा पञ्चविध भेद से नाना प्रकार से शील के भेद किये हैं। परन्तु वे सब चतुर्विध पारिशुद्धिशील में ही उपसंहत हो सकते हैं अत: इनका ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिये। चार पारिशुद्धिशील ये हैं-(क) प्रातिमोक्षसंवरशील, (ख) इन्द्रियसंवरशील, (ग) आजीवपारिशुद्धिशील, और (घ) प्रत्ययसनिश्रितशील।
(क) संवर का अर्थ है ढकना। प्रातिमोक्ष कहते हैं भगवान् के शिक्षापदों को। उस प्रातिमोक्ष (शिक्षापद) से संवृत शील को प्रातिमोक्षसंवरशील कहते हैं। आचारगोचर से सम्पन्न रहना, अल्पमात्र दोष में भी भय देखना-प्रातिमोक्षसंवरशील कहलाता है।
(ख) शरीर या वाणी द्वारा शीलों का उल्लङ्घन न करना इन्द्रियसंवरशील कहलाता है। वह प्रातिमोक्षसंवरशील सम्पन्न भिक्षु आंख से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, नाक से गंध रूष कर, जीभ से रस चखकर, काय से स्पर्शकर, मन से धर्मों को जानकर निमित्त और अन.गजनों को ग्रहण नहीं करता है, जिनसे कि उन-उन इन्द्रियों में संवर रहित होने पर लोभदानस्यादि अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, उनके संवर के लिये उसका तत्पर होना, उसके द्वारा उनकी सुरक्षा करना ही इन्द्रिय-संवरशील है।
(ग) आजीविका के प्रसङ्ग में कहे गये छह शिक्षापादों अनुसार आचरण करना आजीवपारिशुद्धिशील कहलाता है। वे छह शिक्षापद पाराजिक में यों कहे है-१. आजीविका के लिए जनता को इन्द्रजाल दिखाना, २. ठग-विद्या, ३. अपने को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना कि जिससे कुछ मिले, ४. भिक्षु द्वारा अपने को बढ़ा-चढ़ा हुआ दिखाकर अच्छा भोजन या वस्त्र या अन्य लाभ की वस्तु प्राप्त करना, ५. या अपनी प्रशंसा कर जनता से उपभोग वस्तुएँ प्राप्त करना। इन छह शिक्षापदों के अनुसार आजीविकाशील-रक्षा ही आजीवपारिशुद्धिशील कहलाता है।