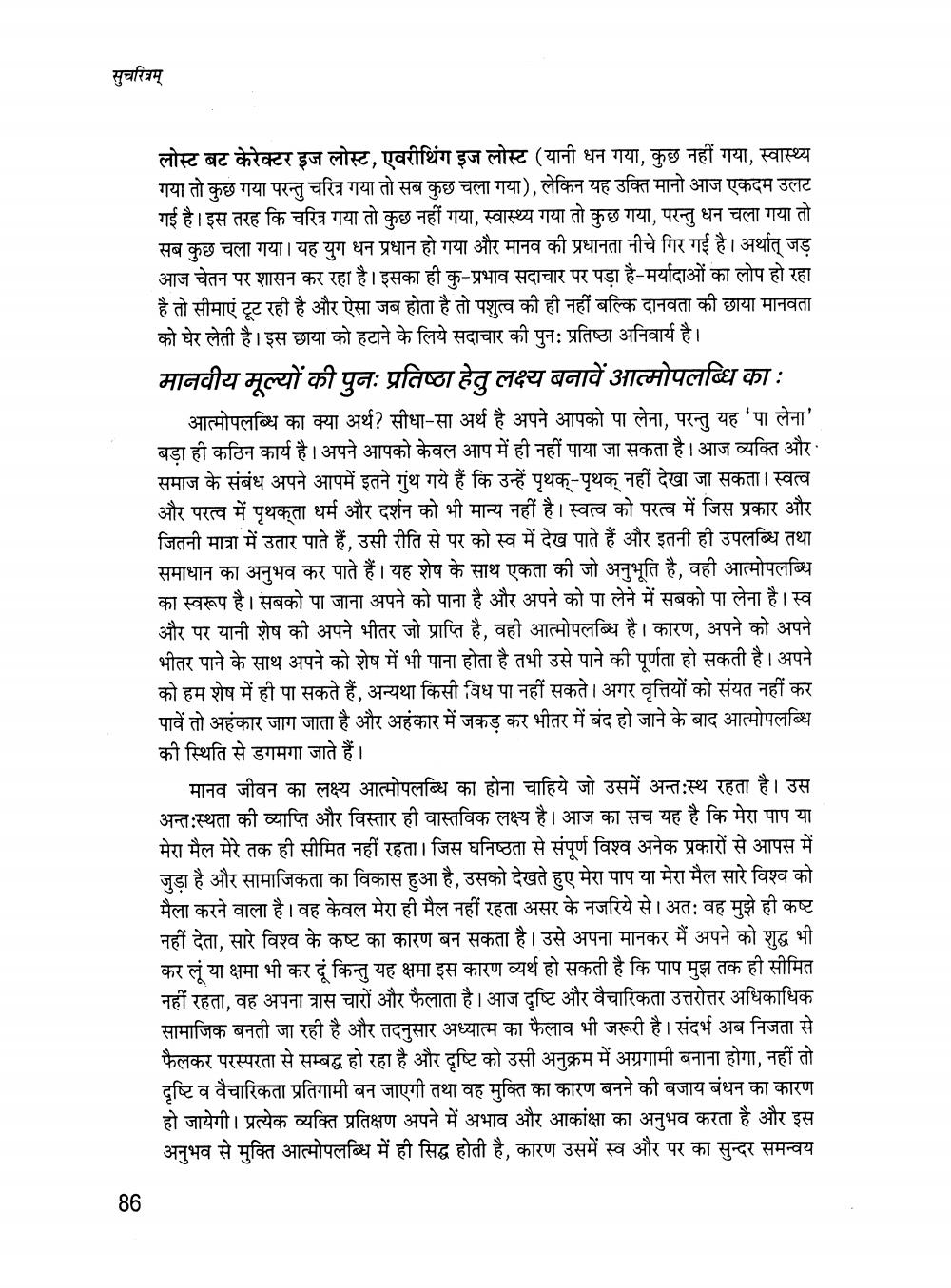________________
सुचरित्रम्
लोस्ट बट केरेक्टर इज लोस्ट, एवरीथिंग इज लोस्ट (यानी धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया परन्तु चरित्र गया तो सब कुछ चला गया), लेकिन यह उक्ति मानो आज एकदम उलट गई है। इस तरह कि चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परन्तु धन चला गया तो सब कुछ चला गया। यह युग धन प्रधान हो गया और मानव की प्रधानता नीचे गिर गई है। अर्थात् जड़ आज चेतन पर शासन कर रहा है। इसका ही कु-प्रभाव सदाचार पर पड़ा है-मर्यादाओं का लोप हो रहा है तो सीमाएं टूट रही है और ऐसा जब होता है तो पशुत्व की ही नहीं बल्कि दानवता की छाया मानवता को घेर लेती है। इस छाया को हटाने के लिये सदाचार की पुनः प्रतिष्ठा अनिवार्य है। मानवीय मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा हेतु लक्ष्य बनावें आत्मोपलब्धि का : ____ आत्मोपलब्धि का क्या अर्थ? सीधा-सा अर्थ है अपने आपको पा लेना, परन्तु यह 'पा लेना' बड़ा ही कठिन कार्य है। अपने आपको केवल आप में ही नहीं पाया जा सकता है। आज व्यक्ति और समाज के संबंध अपने आपमें इतने गुंथ गये हैं कि उन्हें पृथक्-पृथक् नहीं देखा जा सकता। स्वत्व
और परत्व में पृथक्ता धर्म और दर्शन को भी मान्य नहीं है। स्वत्व को परत्व में जिस प्रकार और जितनी मात्रा में उतार पाते हैं, उसी रीति से पर को स्व में देख पाते हैं और इतनी ही उपलब्धि तथा समाधान का अनुभव कर पाते हैं। यह शेष के साथ एकता की जो अनुभूति है, वही आत्मोपलब्धि का स्वरूप है। सबको पा जाना अपने को पाना है और अपने को पा लेने में सबको पा लेना है। स्व
और पर यानी शेष की अपने भीतर जो प्राप्ति है, वही आत्मोपलब्धि है। कारण, अपने को अपने भीतर पाने के साथ अपने को शेष में भी पाना होता है तभी उसे पाने की पूर्णता हो सकती है। अपने को हम शेष में ही पा सकते हैं, अन्यथा किसी विध पा नहीं सकते। अगर वृत्तियों को संयत नहीं कर पावें तो अहंकार जाग जाता है और अहंकार में जकड़ कर भीतर में बंद हो जाने के बाद आत्मोपलब्धि की स्थिति से डगमगा जाते हैं।
मानव जीवन का लक्ष्य आत्मोपलब्धि का होना चाहिये जो उसमें अन्तःस्थ रहता है। उस अन्त:स्थता की व्याप्ति और विस्तार ही वास्तविक लक्ष्य है। आज का सच यह है कि मेरा पाप या मेरा मैल मेरे तक ही सीमित नहीं रहता। जिस घनिष्ठता से संपूर्ण विश्व अनेक प्रकारों से आपस में जुड़ा है और सामाजिकता का विकास हुआ है, उसको देखते हुए मेरा पाप या मेरा मैल सारे विश्व को मैला करने वाला है। वह केवल मेरा ही मैल नहीं रहता असर के नजरिये से। अत: वह मुझे ही कष्ट नहीं देता, सारे विश्व के कष्ट का कारण बन सकता है। उसे अपना मानकर मैं अपने को शुद्ध भी कर लूं या क्षमा भी कर दूं किन्तु यह क्षमा इस कारण व्यर्थ हो सकती है कि पाप मुझ तक ही सीमित नहीं रहता, वह अपना त्रास चारों और फैलाता है। आज दृष्टि और वैचारिकता उत्तरोत्तर अधिकाधिक सामाजिक बनती जा रही है और तदनुसार अध्यात्म का फैलाव भी जरूरी है। संदर्भ अब निजता से फैलकर परस्परता से सम्बद्ध हो रहा है और दृष्टि को उसी अनुक्रम में अग्रगामी बनाना होगा, नहीं तो दृष्टि व वैचारिकता प्रतिगामी बन जाएगी तथा वह मुक्ति का कारण बनने की बजाय बंधन का कारण हो जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण अपने में अभाव और आकांक्षा का अनुभव करता है और इस अनुभव से मुक्ति आत्मोपलब्धि में ही सिद्ध होती है, कारण उसमें स्व और पर का सुन्दर समन्वय
86