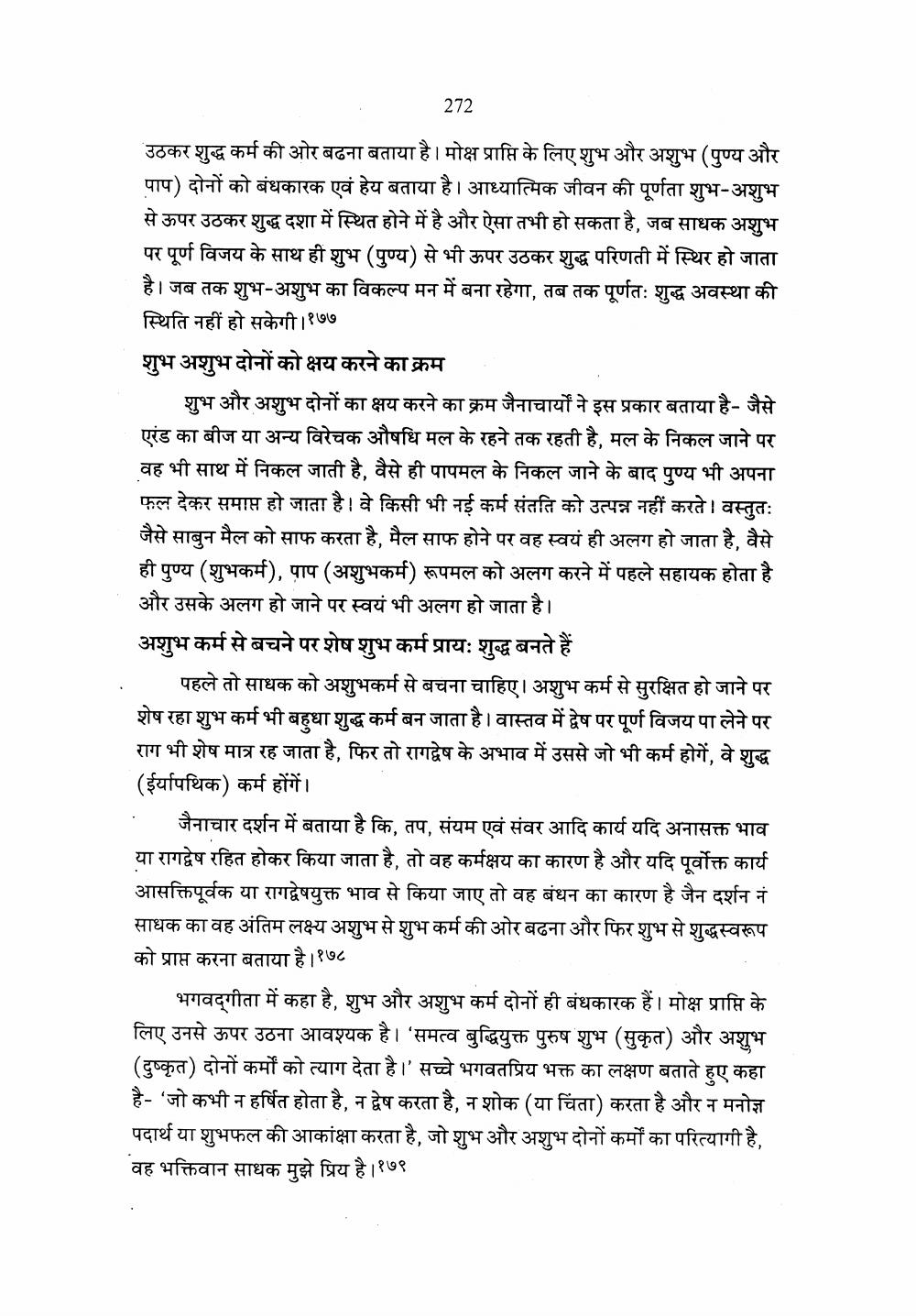________________
272
उठकर शुद्ध कर्म की ओर बढना बताया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ और अशुभ (पुण्य और पाप) दोनों को बंधकारक एवं हेय बताया है । आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता शुभ-अशुभ से ऊपर उठकर शुद्ध दशा में स्थित होने में है और ऐसा तभी हो सकता है, जब साधक अशुभ पर पूर्ण विजय के साथ ही शुभ (पुण्य) से भी ऊपर उठकर शुद्ध परिणती में स्थिर हो जाता है। जब तक शुभ-अशुभ का विकल्प मन में बना रहेगा, तब तक पूर्णतः शुद्ध अवस्था की स्थिति नहीं हो सकेगी। १७७
शुभ अशुभ दोनों को क्षय करने का क्रम
शुभ और अशुभ दोनों का क्षय करने का क्रम जैनाचार्यों ने इस प्रकार बताया है- जैसे एरंड का बीज या अन्य विरेचक औषधि मल के रहने तक रहती है, मल के निकल जाने पर वह भी साथ में निकल जाती है, वैसे ही पापमल के निकल जाने के बाद पुण्य भी अपना फल देकर समाप्त हो जाता है। वे किसी भी नई कर्म संतति को उत्पन्न नहीं करते । वस्तुतः जैसे साबुन मैल को साफ करता है, मैल साफ होने पर वह स्वयं ही अलग हो जाता है, वैसे ही पुण्य (शुभकर्म), पाप (अशुभकर्म) रूपमल को अलग करने में पहले सहायक होता है और उसके अलग हो जाने पर स्वयं भी अलग हो जाता है।
अशुभ कर्म से बचने पर शेष शुभ कर्म प्रायः शुद्ध बनते हैं
पहले तो साधक को अशुभकर्म से बचना चाहिए। अशुभ कर्म से सुरक्षित हो जाने पर शेष रहा शुभ कर्म भी बहुधा शुद्ध कर्म बन जाता है। वास्तव में द्वेष पर पूर्ण विजय पा लेने पर राग भी शेष मात्र रह जाता है, फिर तो रागद्वेष के अभाव में उससे जो भी कर्म होगें, वे शुद्ध (ईर्यापथिक) कर्म होंगें ।
जैनाचार दर्शन में बताया है कि, तप, संयम एवं संवर आदि कार्य यदि अनासक्त भाव या रागद्वेष रहित होकर किया जाता है, तो वह कर्मक्षय का कारण है और यदि पूर्वोक्त कार्य आसक्तिपूर्वक या रागद्वेषयुक्त भाव से किया जाए तो वह बंधन का कारण है जैन दर्शन नं साधक का वह अंतिम लक्ष्य अशुभ से शुभ कर्म की ओर बढना और फिर शुभ से शुद्धस्वरूप को प्राप्त करना बताया है । १७८
भगवद्गीता में कहा है, शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही बंधकारक हैं। मोक्ष प्राप्त लिए उनसे ऊपर उठना आवश्यक है । 'समत्व बुद्धियुक्त पुरुष शुभ (सुकृत) और अशुभ (दुष्कृत) दोनों कर्मों को त्याग देता है।' सच्चे भगवतप्रिय भक्त का लक्षण बताते हुए है- 'जो कभी न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक (या चिंता) करता है और न मनोज्ञ पदार्थ या शुभफल की आकांक्षा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का परित्यागी है, वह भक्तिवान साधक मुझे प्रिय है । १७९