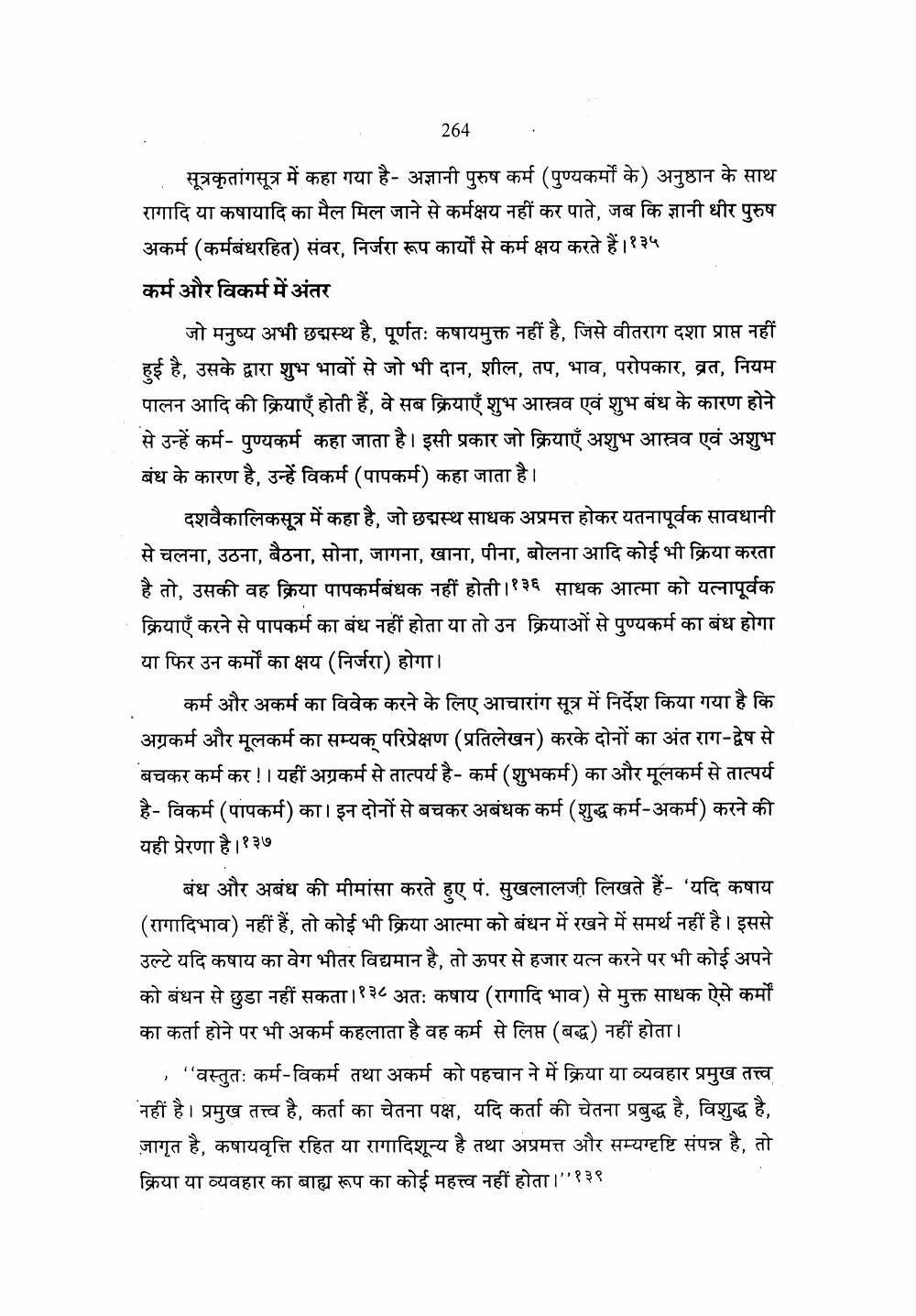________________
264
सूत्रकृतांगसूत्र में कहा गया है- अज्ञानी पुरुष कर्म (पुण्यकर्मों के) अनुष्ठान के साथ रागादि या कषायादि का मैल मिल जाने से कर्मक्षय नहीं कर पाते, जब कि ज्ञानी धीर पुरुष अकर्म (कर्मबंधरहित) संवर, निर्जरा रूप कार्यों से कर्म क्षय करते हैं।१३५ कर्म और विकर्म में अंतर
जो मनुष्य अभी छद्मस्थ है, पूर्णत: कषायमुक्त नहीं है, जिसे वीतराग दशा प्राप्त नहीं हुई है, उसके द्वारा शुभ भावों से जो भी दान, शील, तप, भाव, परोपकार, व्रत, नियम पालन आदि की क्रियाएँ होती हैं, वे सब क्रियाएँ शुभ आस्रव एवं शुभ बंध के कारण होने से उन्हें कर्म- पुण्यकर्म कहा जाता है। इसी प्रकार जो क्रियाएँ अशुभ आस्रव एवं अशुभ बंध के कारण है, उन्हें विकर्म (पापकर्म) कहा जाता है।
दशवैकालिकसूत्र में कहा है, जो छद्मस्थ साधक अप्रमत्त होकर यतनापूर्वक सावधानी से चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, बोलना आदि कोई भी क्रिया करता है तो, उसकी वह क्रिया पापकर्मबंधक नहीं होती।१३६ साधक आत्मा को यत्नापूर्वक क्रियाएँ करने से पापकर्म का बंध नहीं होता या तो उन क्रियाओं से पुण्यकर्म का बंध होगा या फिर उन कर्मों का क्षय (निर्जरा) होगा।
कर्म और अकर्म का विवेक करने के लिए आचारांग सूत्र में निर्देश किया गया है कि अग्रकर्म और मूलकर्म का सम्यक् परिप्रेक्षण (प्रतिलेखन) करके दोनों का अंत राग-द्वेष से बचकर कर्म कर ! । यहीं अग्रकर्म से तात्पर्य है- कर्म (शुभकर्म) का और मूलकर्म से तात्पर्य है- विकर्म (पापकर्म) का। इन दोनों से बचकर अबंधक कर्म (शुद्ध कर्म-अकर्म) करने की यही प्रेरणा है। १३७
बंध और अबंध की मीमांसा करते हुए पं. सुखलालजी लिखते हैं- 'यदि कषाय (रागादिभाव) नहीं हैं, तो कोई भी क्रिया आत्मा को बंधन में रखने में समर्थ नहीं है। इससे उल्टे यदि कषाय का वेग भीतर विद्यमान है, तो ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को बंधन से छुडा नहीं सकता। १३८ अत: कषाय (रागादि भाव) से मुक्त साधक ऐसे कर्मों का कर्ता होने पर भी अकर्म कहलाता है वह कर्म से लिप्त (बद्ध) नहीं होता।
, "वस्तुत: कर्म-विकर्म तथा अकर्म को पहचान ने में क्रिया या व्यवहार प्रमुख तत्त्व नहीं है। प्रमुख तत्त्व है, कर्ता का चेतना पक्ष, यदि कर्ता की चेतना प्रबुद्ध है, विशुद्ध है, जागृत है, कषायवृत्ति रहित या रागादिशून्य है तथा अप्रमत्त और सम्यग्दृष्टि संपन्न है, तो क्रिया या व्यवहार का बाह्य रूप का कोई महत्त्व नहीं होता।'' १३९