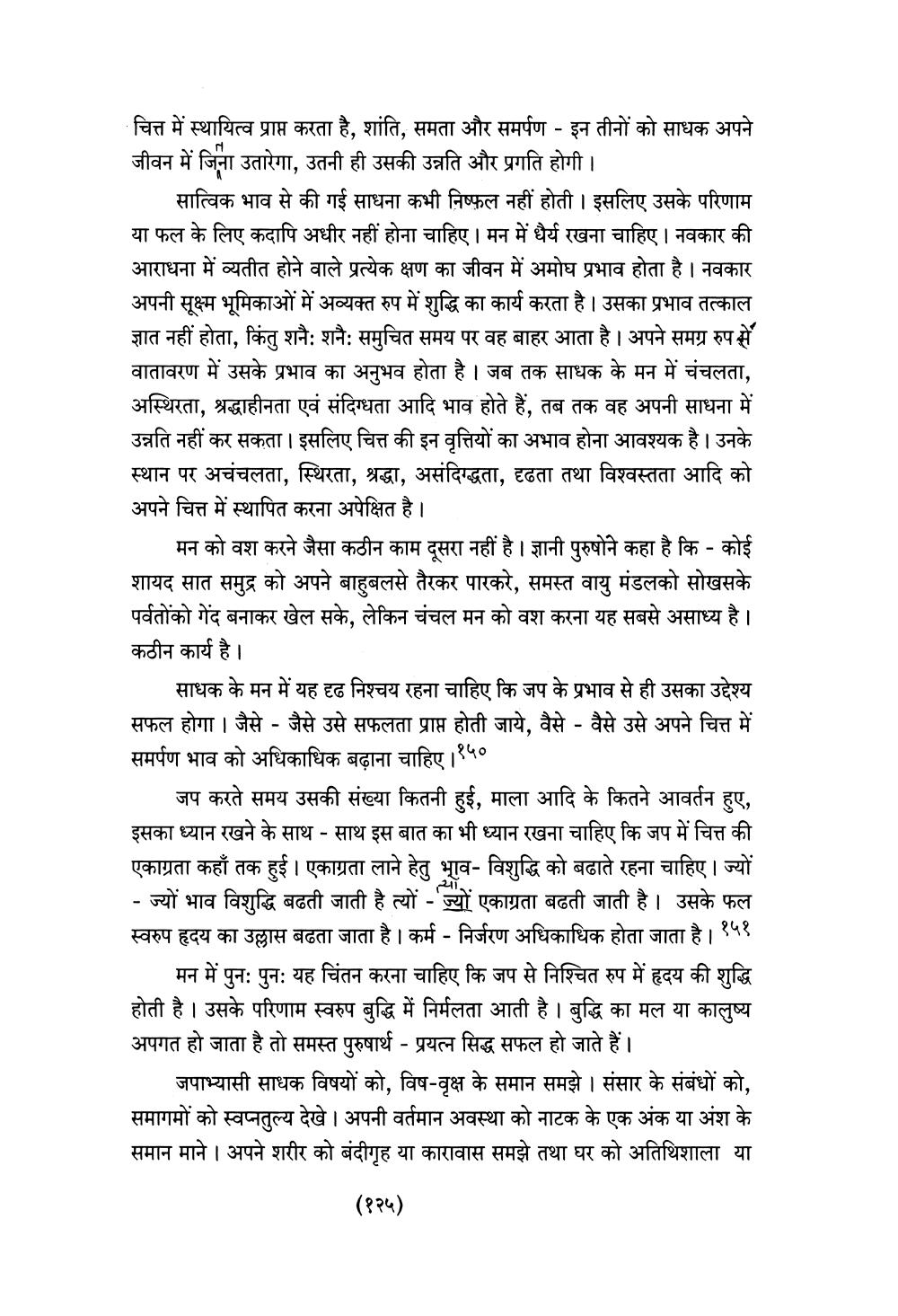________________
चित्त में स्थायित्व प्राप्त करता है, शांति, समता और समर्पण - इन तीनों को साधक अपने जीवन में जिना उतारेगा, उतनी ही उसकी उन्नति और प्रगति होगी।
सात्विक भाव से की गई साधना कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए उसके परिणाम या फल के लिए कदापि अधीर नहीं होना चाहिए । मन में धैर्य रखना चाहिए । नवकार की आराधना में व्यतीत होने वाले प्रत्येक क्षण का जीवन में अमोघ प्रभाव होता है । नवकार अपनी सूक्ष्म भूमिकाओं में अव्यक्त रुप में शुद्धि का कार्य करता है। उसका प्रभाव तत्काल ज्ञात नहीं होता, किंतु शनैः शनैः समुचित समय पर वह बाहर आता है। अपने समग्र रुप में वातावरण में उसके प्रभाव का अनुभव होता है। जब तक साधक के मन में चंचलता, अस्थिरता, श्रद्धाहीनता एवं संदिग्धता आदि भाव होते हैं, तब तक वह अपनी साधना में उन्नति नहीं कर सकता । इसलिए चित्त की इन वृत्तियों का अभाव होना आवश्यक है। उनके स्थान पर अचंचलता, स्थिरता, श्रद्धा, असंदिग्द्धता, दृढता तथा विश्वस्तता आदि को अपने चित्त में स्थापित करना अपेक्षित है।
मन को वश करने जैसा कठीन काम दूसरा नहीं है। ज्ञानी पुरुषोने कहा है कि - कोई शायद सात समुद्र को अपने बाहुबलसे तैरकर पारकरे, समस्त वायु मंडलको सोखसके पर्वतोंको गेंद बनाकर खेल सके, लेकिन चंचल मन को वश करना यह सबसे असाध्य है। कठीन कार्य है। ___साधक के मन में यह दृढ निश्चय रहना चाहिए कि जप के प्रभाव से ही उसका उद्देश्य सफल होगा । जैसे- जैसे उसे सफलता प्राप्त होती जाये, वैसे - वैसे उसे अपने चित्त में समर्पण भाव को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिए ।१५०
__जप करते समय उसकी संख्या कितनी हुई, माला आदि के कितने आवर्तन हुए, इसका ध्यान रखने के साथ - साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जप में चित्त की एकाग्रता कहाँ तक हुई । एकाग्रता लाने हेतु भाव- विशुद्धि को बढाते रहना चाहिए । ज्यों - ज्यों भाव विशुद्धि बढती जाती है त्यों - ज्यों एकाग्रता बढती जाती है। उसके फल स्वरुप हृदय का उल्लास बढता जाता है। कर्म - निर्जरण अधिकाधिक होता जाता है। १५१
मन में पुन: पुन: यह चिंतन करना चाहिए कि जप से निश्चित रुप में हृदय की शुद्धि होती है। उसके परिणाम स्वरुप बुद्धि में निर्मलता आती है। बुद्धि का मल या कालुष्य अपगत हो जाता है तो समस्त पुरुषार्थ - प्रयत्न सिद्ध सफल हो जाते हैं।
जपाभ्यासी साधक विषयों को, विष-वृक्ष के समान समझे । संसार के संबंधों को, समागमों को स्वप्नतुल्य देखे । अपनी वर्तमान अवस्था को नाटक के एक अंक या अंश के समान माने । अपने शरीर को बंदीगृह या कारावास समझे तथा घर को अतिथिशाला या
(१२५)