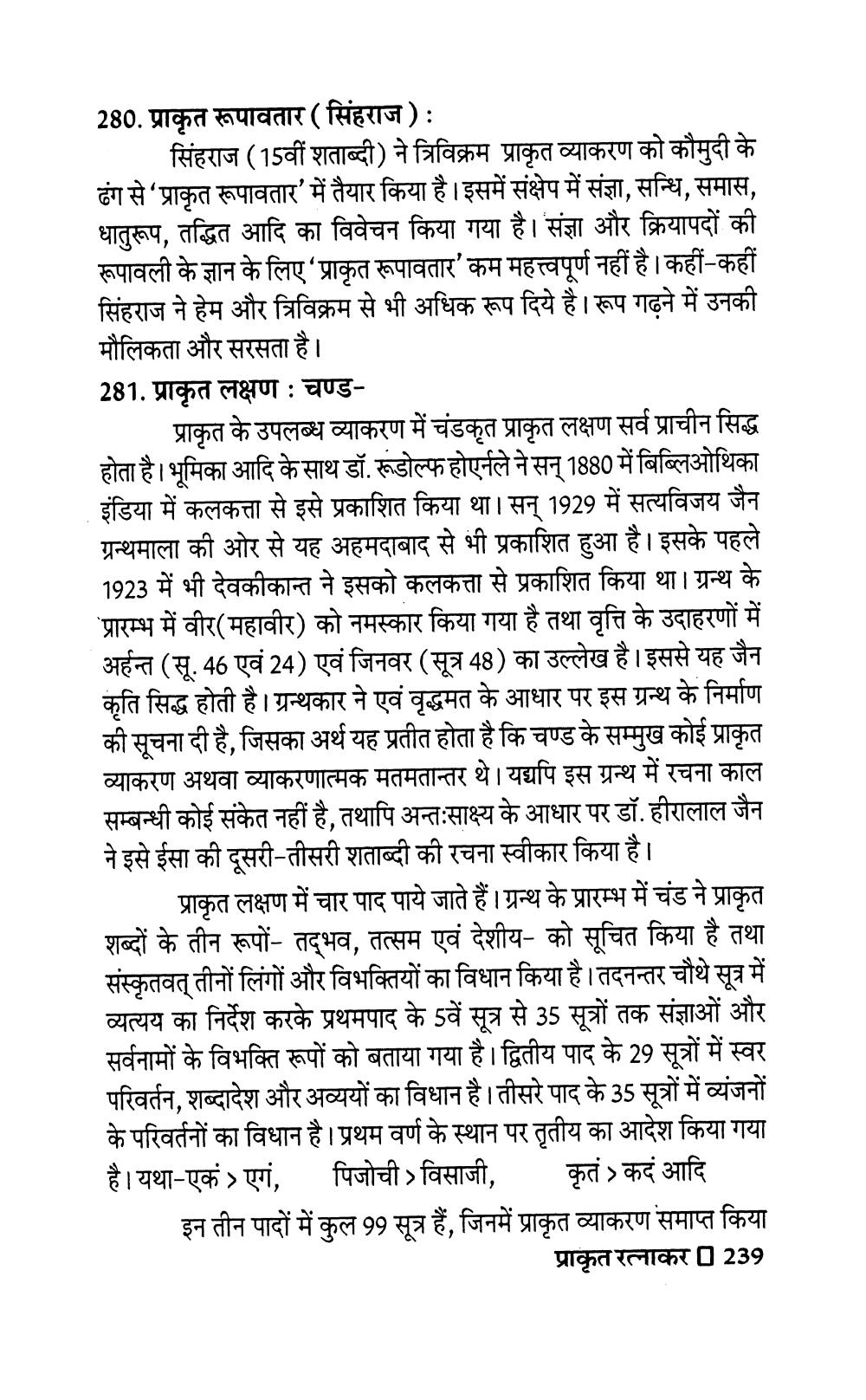________________
280. प्राकृत रूपावतार ( सिंहराज ) :
सिंहराज (15वीं शताब्दी) ने त्रिविक्रम प्राकृत व्याकरण को कौमुदी के ढंग से ‘प्राकृत रूपावतार' में तैयार किया है। इसमें संक्षेप में संज्ञा, सन्धि, समास, धातुरूप, तद्धित आदि का विवेचन किया गया है। संज्ञा और क्रियापदों की रूपावली के ज्ञान के लिए ‘प्राकृत रूपावतार' कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। कहीं-कहीं सिंहराज ने हेम और त्रिविक्रम से भी अधिक रूप दिये है। रूप गढ़ने में उनकी मौलिकता और सरसता है ।
281. प्राकृत लक्षण : चण्ड
प्राकृत के उपलब्ध व्याकरण में चंडकृत प्राकृत लक्षण सर्व प्राचीन सिद्ध होता है। भूमिका आदि के साथ डॉ. रूडोल्फ होएर्नले ने सन् 1880 में बिब्लिओथिका इंडिया में कलकत्ता से इसे प्रकाशित किया था। सन् 1929 में सत्यविजय जैन ग्रन्थमाला की ओर से यह अहमदाबाद से भी प्रकाशित हुआ है । इसके पहले 1923 में भी देवकीकान्त ने इसको कलकत्ता से प्रकाशित किया था । ग्रन्थ के `प्रारम्भ में वीर (महावीर) को नमस्कार किया गया है तथा वृत्ति के उदाहरणों में अर्हन्त (सू. 46 एवं 24) एवं जिनवर (सूत्र 48 ) का उल्लेख है। इससे यह जैन कृति सिद्ध होती है । ग्रन्थकार ने एवं वृद्धमत के आधार पर इस ग्रन्थ के निर्माण की सूचना दी है, जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि चण्ड के सम्मुख कोई प्राकृत व्याकरण अथवा व्याकरणात्मक मतमतान्तर थे । यद्यपि इस ग्रन्थ में रचना काल सम्बन्धी कोई संकेत नहीं है, तथापि अन्तः साक्ष्य के आधार पर डॉ. हीरालाल जैन ने इसे ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी की रचना स्वीकार किया है।
प्राकृत लक्षण में चार पाद पाये जाते हैं । ग्रन्थ के प्रारम्भ में चंड ने प्राकृत शब्दों के तीन रूपों - तद्भव, तत्सम एवं देशीय - को सूचित किया है तथा संस्कृतवत् तीनों लिंगों और विभक्तियों का विधान किया है। तदनन्तर चौथे सूत्र में व्यत्यय का निर्देश करके प्रथमपाद के 5वें सूत्र से 35 सूत्रों तक संज्ञाओं और सर्वनामों के विभक्ति रूपों को बताया गया है। द्वितीय पाद के 29 सूत्रों में स्वर परिवर्तन, शब्दादेश और अव्ययों का विधान है। तीसरे पाद के 35 सूत्रों में व्यंजनों के परिवर्तनों का विधान है। प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय का आदेश किया गया है । यथा - एकं > एगं, पिजोची > विसाजी, कृतं > कदं आदि
इन तीन पादों में कुल 99 सूत्र हैं, जिनमें प्राकृत व्याकरण समाप्त किया
प्राकृत रत्नाकर 239