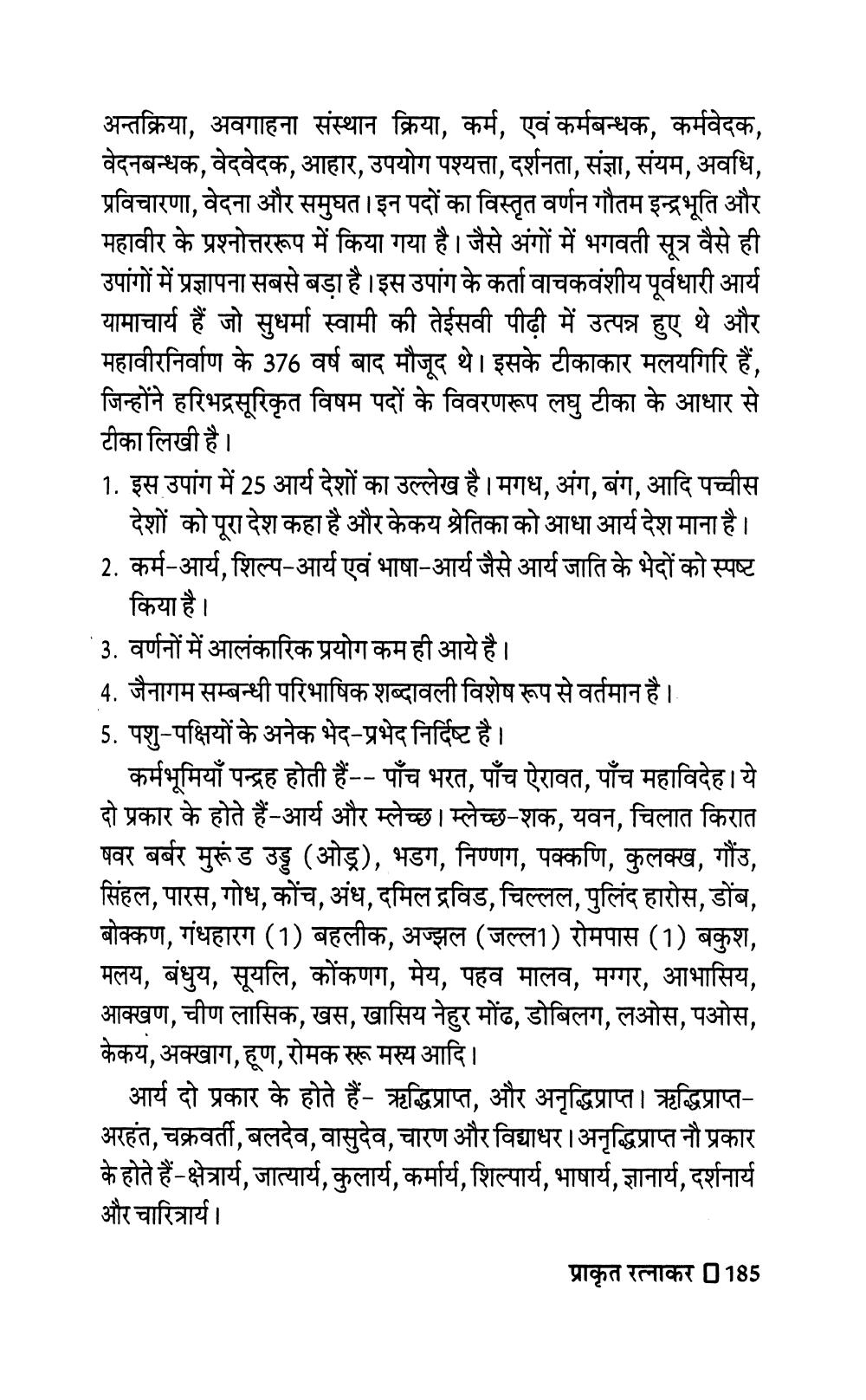________________
अन्तक्रिया, अवगाहना संस्थान क्रिया, कर्म, एवं कर्मबन्धक, कर्मवेदक, वेदनबन्धक, वेदवेदक, आहार, उपयोग पश्यत्ता, दर्शनता, संज्ञा, संयम, अवधि, प्रविचारणा, वेदना और समुघत । इन पदों का विस्तृत वर्णन गौतम इन्द्रभूति और महावीर के प्रश्नोत्तररूप में किया गया है। जैसे अंगों में भगवती सूत्र वैसे ही उपांगों में प्रज्ञापना सबसे बड़ा है। इस उपांग के कर्ता वाचकवंशीय पूर्वधारी आर्य यामाचार्य हैं जो सुधर्मा स्वामी की तेईसवी पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे और महावीरनिर्वाण के 376 वर्ष बाद मौजूद थे। इसके टीकाकार मलयगिरि हैं, जिन्होंने हरिभद्रसूरिकृत विषम पदों के विवरणरूप लघु टीका के आधार से टीका लिखी है ।
1. इस उपांग में 25 आर्य देशों का उल्लेख है । मगध, अंग, बंग, आदि पच्चीस देशों को पूरा देश कहा है और केकय श्रेतिका को आधा आर्य देश माना है। 2. कर्म - आर्य, शिल्प - आर्य एवं भाषा-आर्य जैसे आर्य जाति के भेदों को स्पष्ट किया है ।
3. वर्णनों में आलंकारिक प्रयोग कम ही आये है ।
4. जैनागम सम्बन्धी परिभाषिक शब्दावली विशेष रूप से वर्तमान है।
5. पशु-पक्षियों के अनेक भेद-प्रभेद निर्दिष्ट है।
कर्मभूमियाँ पन्द्रह होती हैं -- पाँच भरत, पाँच ऐरावत, पाँच महाविदेह । ये दो प्रकार के होते हैं - आर्य और म्लेच्छ । म्लेच्छ-शक, यवन, चिलात किरात षवर बर्बर मुरूंड उड्ड (ओडू), भडग, निण्णग, पक्कणि, कुलक्ख, गाँउ, सिंहल, पारस, गोध, कोंच, अंध, दमिल द्रविड, चिल्लल, पुलिंद हारोस, डोंब, बोक्कण, गंधहारग (1) बहलीक, अज्झल ( जल्ल 1 ) रोमपास ( 1 ) बकुश, मलय, बंधुय, सूयलि, कोंकणग, मेय, पहव मालव, मग्गर, आभासिय, आक्खण, चीण लासिक, खस, खासिय नेहुर मोंढ, डोबिलग, लओस, पओस, केकय, अक्खाग, हूण, रोमक रूरू मस्य आदि ।
आर्य दो प्रकार के होते हैं- ऋद्धिप्राप्त, और अनृद्धिप्राप्त। ऋद्धिप्राप्तअरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण और विद्याधर । अनृद्धिप्राप्त नौ प्रकार के होते हैं - क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कुलार्य, कर्मार्य, शिल्पार्य, भाषार्य, ज्ञानार्य, दर्शनार्य और चारित्रार्य ।
प्राकृत रत्नाकर 185