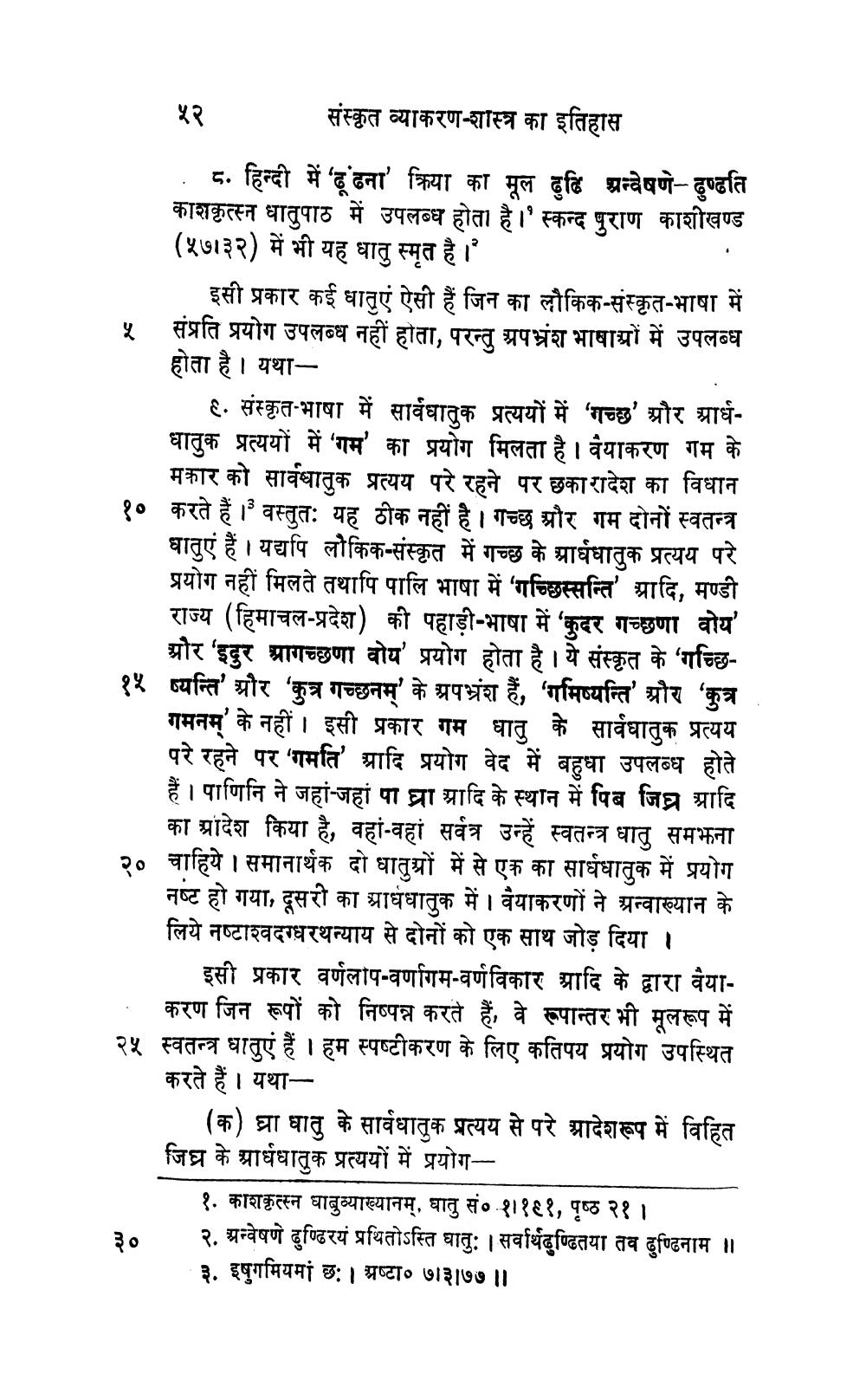________________
५
संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास
८. हिन्दी में 'ढूंढना' क्रिया का मूल दुढि प्रन्वेषणे - दुण्ढति काशकृत्स्न धातुपाठ में उपलब्ध होता है ।' स्कन्द पुराण काशीखण्ड (५७।३२ ) में भी यह धातु स्मृत है ।"
५२
३०
इसी प्रकार कई धातुएं ऐसी हैं जिन का लौकिक संस्कृत भाषा में संप्रति प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, परन्तु अपभ्रंश भाषाओं में उपलब्ध होता है । यथा
C. संस्कृत भाषा में सार्वधातुक प्रत्ययों में 'गच्छ' और अर्धधातुक प्रत्ययों में 'गम' का प्रयोग मिलता है । वैयाकरण गम के मकार को सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर छकारादेश का विधान १० करते हैं । वस्तुत: यह ठीक नहीं है । गच्छ और गम दोनों स्वतन्त्र धातुएं हैं । यद्यपि लौकिक - संस्कृत में गच्छ के प्रार्धधातुक प्रत्यय परे प्रयोग नहीं मिलते तथापि पालि भाषा में 'गच्छिस्सन्ति' आदि, मण्डी राज्य ( हिमाचल-प्रदेश) की पहाड़ी भाषा में 'कुदर गच्छणा वोय' और 'इदुर प्रागच्छणा वोय' प्रयोग होता है । ये संस्कृत के 'गच्छि - १५ ष्यन्ति' और 'कुत्र गच्छनम्' के अपभ्रंश हैं, 'गमिष्यन्ति' और 'कुत्र गमनम्' के नहीं । इसी प्रकार गम धातु के सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर 'गमति' आदि प्रयोग वेद में बहुधा उपलब्ध होते हैं । पाणिनि ने जहां-जहां पाघ्रा आदि के स्थान में पिब जिघ्र आदि का प्रदेश किया है, वहां-वहां सर्वत्र उन्हें स्वतन्त्र धातु समझना २० चाहिये । समानार्थक दो धातुत्रों में से एक का सार्धधातुक में प्रयोग नष्ट हो गया, दूसरी का आर्धधातुक में । वैयाकरणों ने अन्वाख्यान के लिये नष्टाश्वदग्धरथन्याय से दोनों को एक साथ जोड़ दिया ।
इसी प्रकार वर्णलाप वर्णागम वर्णविकार आदि के द्वारा वैयाकरण जिन रूपों को निष्पन्न करते हैं, वे रूपान्तर भी मूलरूप में २५ स्वतन्त्र धातुएं हैं । हम स्पष्टीकरण के लिए कतिपय प्रयोग उपस्थित
करते हैं । यथा—
( क ) घ्रा धातु के सार्वधातुक प्रत्यय से परे आदेशरूप में विहित जिघ्र के आर्धधातुक प्रत्ययों में प्रयोग
१. काशकृत्स्न धातुव्याख्यानम्, धातु सं० १ १९१, पृष्ठ २१ ।
२. अन्वेषणे ढुण्ढिरयं प्रथितोऽस्ति घातुः । सर्वार्थदुण्डितया तव दुण्डिनाम || ३. इषुगमियमां छः । अष्टा० ७।३।७७ ॥