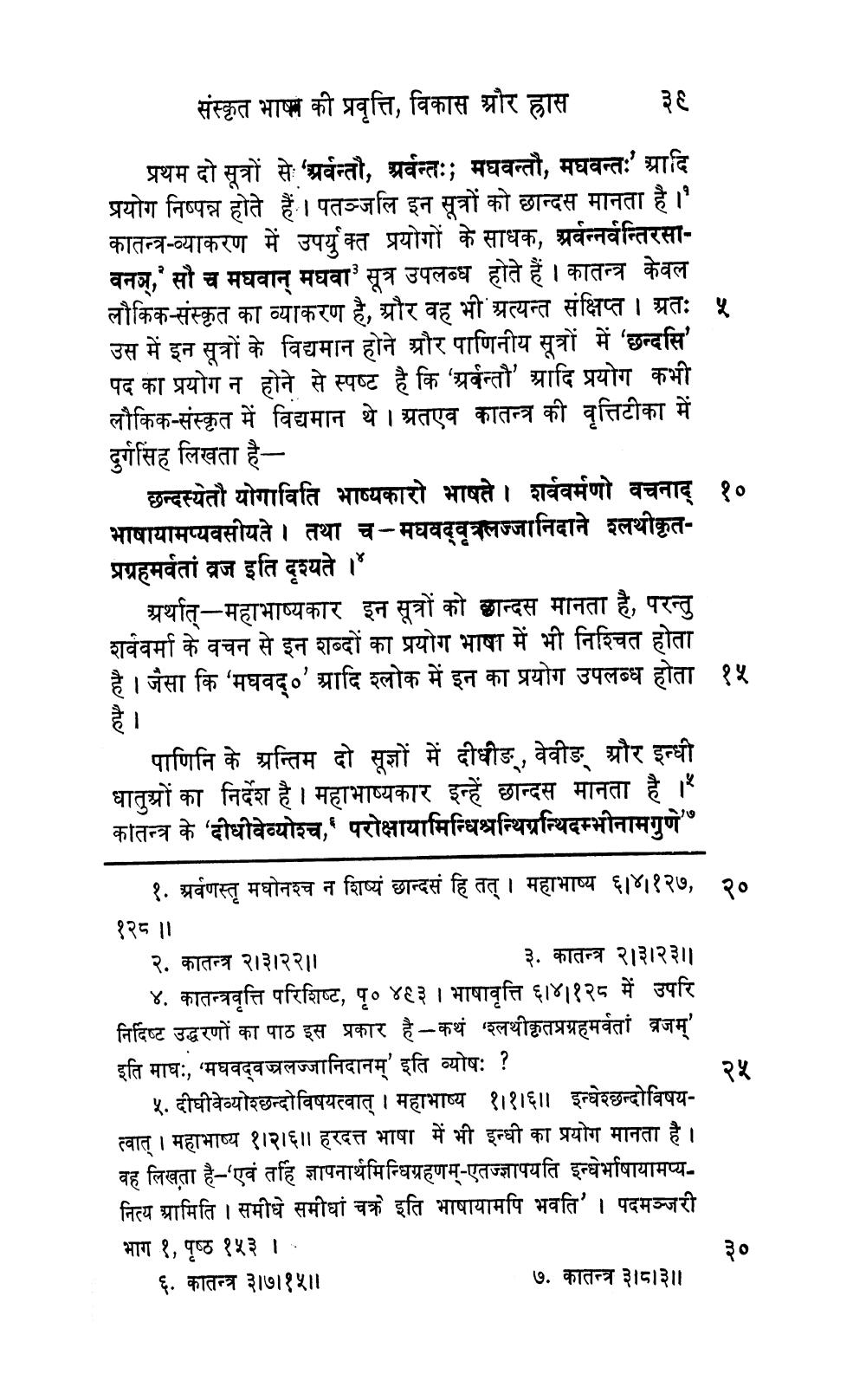________________
संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास और ह्रास ३६ प्रथम दो सूत्रों सेः 'अर्वन्तौ, अर्वन्तः; मघवन्तौ, मघवन्तः' आदि प्रयोग निष्पन्न होते हैं। पतञ्जलि इन सूत्रों को छान्दस मानता है।' कातन्त्र-व्याकरण में उपर्युक्त प्रयोगों के साधक, अर्वन्नर्वन्तिरसावनन्, सौ च मघवान् मघवा' सूत्र उपलब्ध होते हैं । कातन्त्र केवल लौकिक-संस्कृत का व्याकरण है, और वह भी अत्यन्त संक्षिप्त । अतः ५ उस में इन सूत्रों के विद्यमान होने और पाणिनीय सूत्रों में 'छन्दसि' पद का प्रयोग न होने से स्पष्ट है कि 'अर्वन्तौ' आदि प्रयोग कभी लौकिक-संस्कृत में विद्यमान थे । अतएव कातन्त्र की वृत्तिटीका में दुर्गसिंह लिखता है___ छन्दस्यतौ योगाविति भाष्यकारो भाषते । शर्ववर्मणो वचनाद् १० भाषायामप्यवसीयते। तथा च-मघवद्ववलज्जानिदाने श्लथीकृतप्रग्रहमर्वतां व्रज इति दृश्यते ।
अर्थात्-महाभाष्यकार इन सूत्रों को छान्दस मानता है, परन्तु शर्ववर्मा के वचन से इन शब्दों का प्रयोग भाषा में भी निश्चित होता है । जैसा कि 'मघवद्' आदि श्लोक में इन का प्रयोग उपलब्ध होता १५
__ पाणिनि के अन्तिम दो सूज्ञों में दीधीङ, वेवीङ और इन्धी धातुओं का निर्देश है । महाभाष्यकार इन्हें छान्दस मानता है ।' कातन्त्र के 'दीधीवेव्योश्च, परोक्षायामिन्धिश्रन्थिग्रन्थिदम्भीनामगुणे" ___ १. अर्वणस्तृ मघोनश्च न शिष्यं छान्दसं हि तत् । महाभाष्य ६।४।१२७, २० १२८ ॥ २. कातन्त्र २।३।२२॥
३. कातन्त्र २।३।२३॥ ४. कातन्त्रवृत्ति परिशिष्ट, पृ० ४६३ । भाषावृत्ति ६।४।१२८ में उपरि निर्दिष्ट उद्धरणों का पाठ इस प्रकार है -कथं 'श्लथीकृतप्रग्रहमर्वतां व्रजम्' इति माघः, 'मघवद्वज्रलज्जानिदानम्' इति व्योषः ?
५. दीघीवेव्योश्छन्दोविषयत्वात् । महाभाष्य १।१।६॥ इन्धेश्छन्दोविषयत्वात् । महाभाष्य ॥२॥६॥ हरदत्त भाषा में भी इन्धी का प्रयोग मानता है। वह लिखता है-‘एवं तहि ज्ञापनार्थमिन्धिग्रहणम्-एतज्ज्ञापयति इन्धेर्भाषायामप्य. नित्य प्रामिति । समीधे समीघां चक्र इति भाषायामपि भवति' । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ १५३ । ६. कातन्त्र ३७॥१५॥
७. कातन्त्र ३८॥३॥
२५