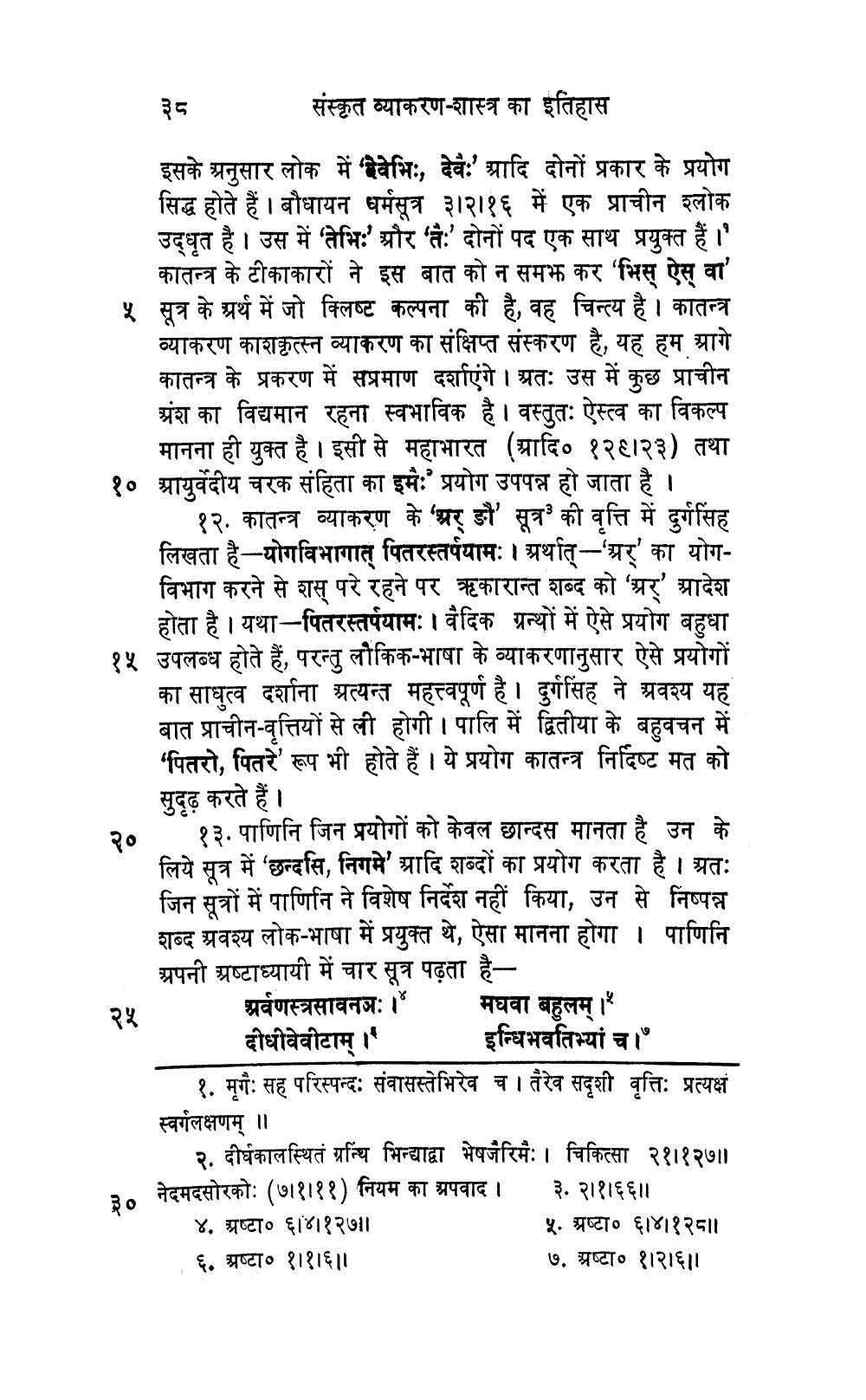________________
३८
संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास
इसके अनुसार लोक में 'बेवेभिः, देवैः' आदि दोनों प्रकार के प्रयोग सिद्ध होते हैं । बौधायन धर्मसूत्र ३।२।१६ में एक प्राचीन श्लोक उद्धत है। उस में 'तेभिः' और 'तः' दोनों पद एक साथ प्रयुक्त हैं।'
कातन्त्र के टीकाकारों ने इस बात को न समझ कर 'भिस् ऐस् वा' ५ सूत्र के अर्थ में जो क्लिष्ट कल्पना की है, वह चिन्त्य है। कातन्त्र
व्याकरण काशकृत्स्न व्याकरण का संक्षिप्त संस्करण है, यह हम आगे कातन्त्र के प्रकरण में सप्रमाण दर्शाएंगे। अतः उस में कुछ प्राचीन अंश का विद्यमान रहना स्वभाविक है। वस्तुतः ऐस्त्व का विकल्प
मानना ही युक्त है। इसी से महाभारत (आदि० १२६।२३) तथा १० आयुर्वेदीय चरक संहिता का इमैः प्रयोग उपपन्न हो जाता है ।
१२. कातन्त्र व्याकरण के 'अर् डौ' सूत्र की वृत्ति में दुर्गसिंह लिखता है-योगविभागात् पितरस्तर्पयामः । अर्थात् –'अर्' का योगविभाग करने से शस् परे रहने पर ऋकारान्त शब्द को 'अर' आदेश
होता है । यथा-पितरस्तर्पयामः । वैदिक ग्रन्थों में ऐसे प्रयोग बहुधा १५ उपलब्ध होते हैं, परन्तु लौकिक-भाषा के व्याकरणानुसार ऐसे प्रयोगों
का साधुत्व दर्शाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। दुर्गसिंह ने अवश्य यह बात प्राचीन-वृत्तियों से ली होगी। पालि में द्वितीया के बहुवचन में 'पितरो, पितरे' रूप भी होते हैं । ये प्रयोग कातन्त्र निर्दिष्ट मत को सुदृढ़ करते हैं।
१३. पाणिनि जिन प्रयोगों को केवल छान्दस मानता है उन के लिये सूत्र में 'छन्दसि, निगमे' आदि शब्दों का प्रयोग करता है। अतः जिन सूत्रों में पाणिनि ने विशेष निर्देश नहीं किया, उन से निष्पन्न शब्द अवश्य लोक-भाषा में प्रयुक्त थे, ऐसा मानना होगा । पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में चार सूत्र पढ़ता है
अर्वणस्त्रसावनञः। मघवा बहुलम् ।
दीधीवेवीटाम् । इन्धिभवतिभ्यां च। १. मृगैः सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । तैरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्ष स्वर्गलक्षणम् ॥
२. दीर्घकालस्थितं ग्रन्थि भिन्द्याद्वा भेषजैरिमैः । चिकित्सा २१११२७॥ ३० नेदमदसोरकोः (७।१।११) नियम का अपवाद। ३. २।११६६॥ ४. अष्टा० ६।४।१२७॥
५. अष्टा० ६।४।१२८॥ ६. अष्टा० १॥१६॥
७. अष्टा० १।२।६॥