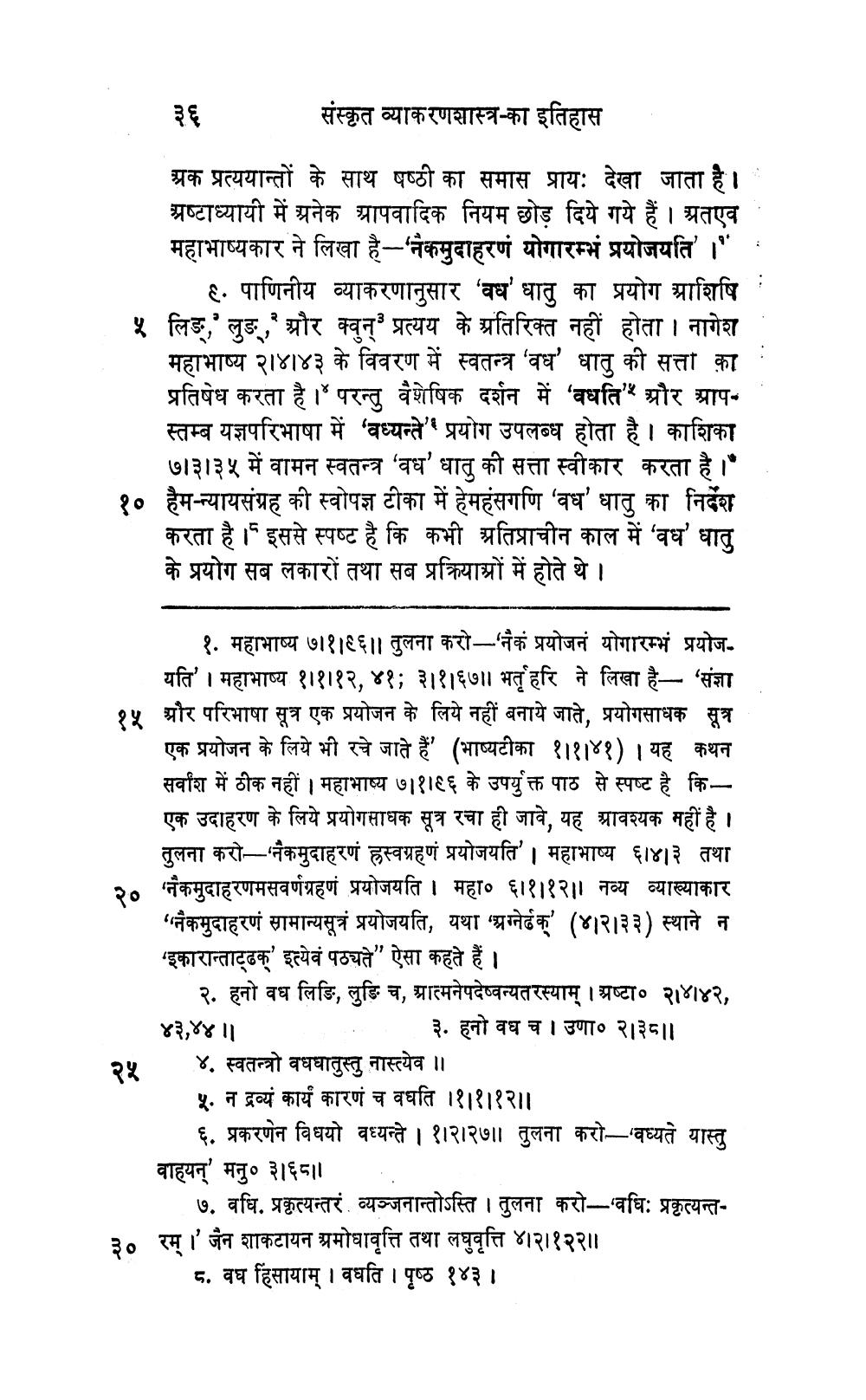________________
संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास
अक प्रत्ययान्तों के साथ षष्ठी का समास प्रायः देखा जाता है। अष्टाध्यायी में अनेक प्रापवादिक नियम छोड़ दिये गये हैं। अतएव महाभाष्यकार ने लिखा है-'नैकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति' ।"
६. पाणिनीय व्याकरणानुसार 'वध' धातु का प्रयोग आशिषि । ५ लिङ, लुङ, और क्वन् प्रत्यय के अतिरिक्त नहीं होता। नागेश
महाभाष्य २।४।४३ के विवरण में स्वतन्त्र 'वध' धातु की सत्ता का प्रतिषेध करता है। परन्तु वैशेषिक दर्शन में 'वधति और आप. स्तम्ब यज्ञपरिभाषा में 'वध्यन्ते प्रयोग उपलब्ध होता है। काशिका ७।३।३५ में वामन स्वतन्त्र 'वध' धातु की सत्ता स्वीकार करता है।' हैम-न्यायसंग्रह की स्वोपज्ञ टीका में हेमहंसगणि 'वध' धातु का निर्देश करता है। इससे स्पष्ट है कि कभी अतिप्राचीन काल में 'वध' धातु के प्रयोग सब लकारों तथा सब प्रक्रियाओं में होते थे।
१. महाभाष्य ७।१९६॥ तुलना करो- 'नकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोज. यति' । महाभाष्य १११।१२, ४१; ३।११६७॥ भर्तृहरि ने लिखा है- 'संज्ञा १५ और परिभाषा सूत्र एक प्रयोजन के लिये नहीं बनाये जाते, प्रयोगसाधक सूत्र
एक प्रयोजन के लिये भी रचे जाते हैं' (भाष्यटीका १११४१) । यह कथन सर्वांश में ठीक नहीं । महाभाष्य ७।११६६ के उपर्युक्त पाठ से स्पष्ट है किएक उदाहरण के लिये प्रयोगसाधक सूत्र रचा ही जावे, यह आवश्यक महीं है ।
तुलना करो—'नकमुदाहरणं ह्रस्वग्रहणं प्रयोजयति' । महाभाष्य ६।४।३ तथा २० 'नकमुदाहरणमसवर्णग्रहणं प्रयोजयति । महा० ६।१।१२॥ नव्य व्याख्याकार
"नकमुदाहरणं सामान्यसूत्रं प्रयोजयति, यथा 'अग्नेढ क्' (४।२।३३) स्थाने न 'इकारान्ताढक्' इत्येवं पठ्यते" ऐसा कहते हैं।
२. हनो वध लिङि, लुङि च, आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् । अष्टा० २।४।४२, ४३,४४॥
३. हनो वध च । उणा० २।३८॥ २५ ४. स्वतन्त्रो वधधातुस्तु नास्त्येव ॥
५. न द्रव्यं कार्य कारणं च वधति ।१।१।१२॥
६. प्रकरणेन विधयो वध्यन्ते । १।२।२७॥ तुलना करो—'वध्यते यास्तु वाहयन्' मनु० ३।६८॥
७. वधि. प्रकृत्यन्तरं व्यञ्जनान्तोऽस्ति । तुलना करो-'वधिः प्रकृत्यन्त३० रम् ।' जैन शाकटायन अमोधावृत्ति तथा लघुवृत्ति ४।२।१२२॥
८. वघ हिंसायाम् । वधति । पृष्ठ १४३ ।