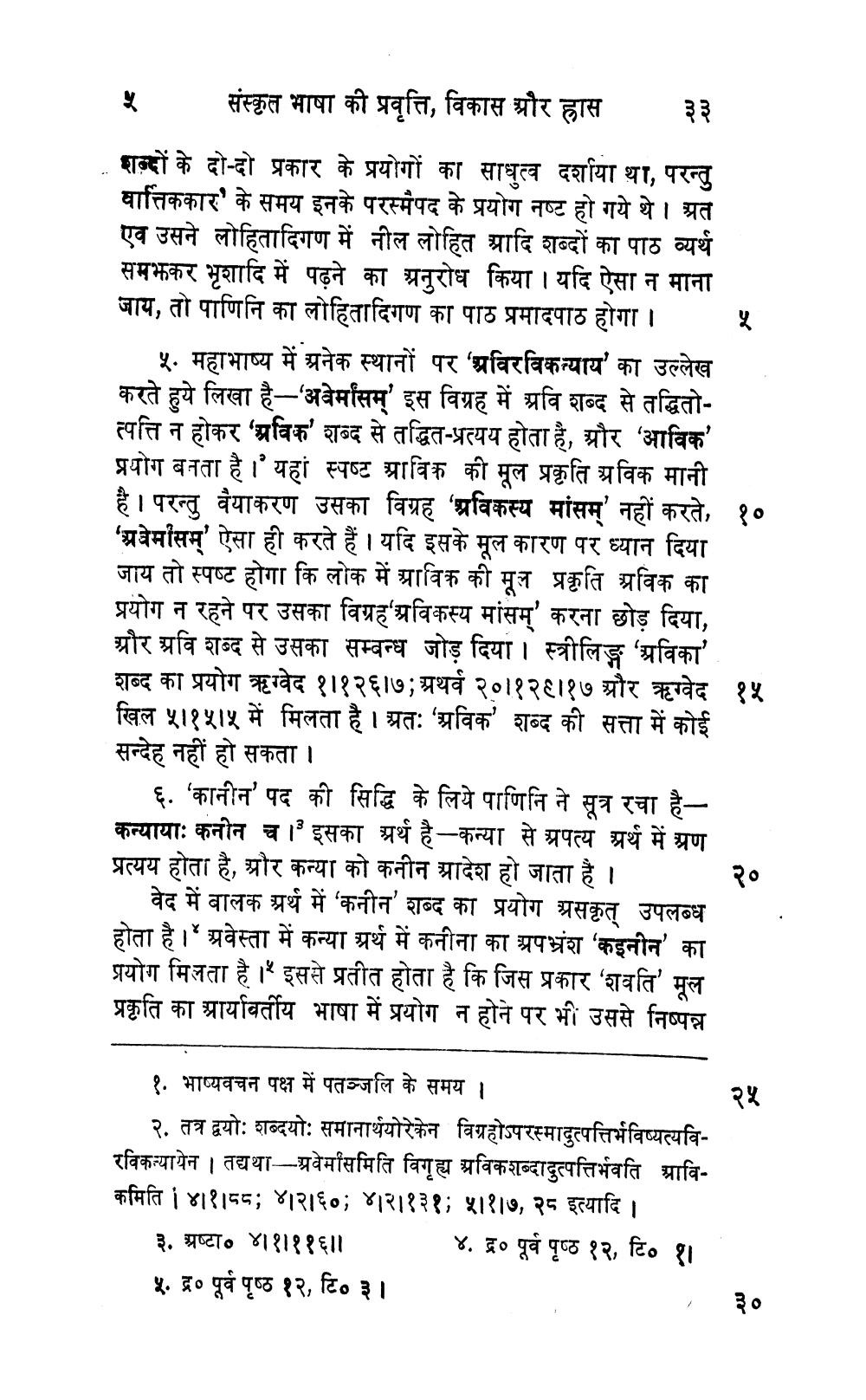________________
५ संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास और ह्रास शन्दों के दो-दो प्रकार के प्रयोगों का साधुत्व दर्शाया था, परन्तु वात्तिककार' के समय इनके परस्मैपद के प्रयोग नष्ट हो गये थे। अत एव उसने लोहितादिगण में नील लोहित आदि शब्दों का पाठ व्यर्थ समझकर भृशादि में पढ़ने का अनुरोध किया। यदि ऐसा न माना जाय, तो पाणिनि का लोहितादिगण का पाठ प्रमादपाठ होगा। ५
५. महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 'अविरविकन्याय' का उल्लेख करते हुये लिखा है-'अवेर्मासम्' इस विग्रह में अवि शब्द से तद्धितोत्पत्ति न होकर 'अविक' शब्द से तद्धित-प्रत्यय होता है, और 'आविक' प्रयोग बनता है। यहां स्पष्ट प्राविक की मूल प्रकृति अविक मानी है। परन्तु वैयाकरण उसका विग्रह 'अविकस्य मांसम्' नहीं करते, १० 'अवेमीसम्' ऐसा ही करते हैं । यदि इसके मूल कारण पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होगा कि लोक में प्राविक की मूल प्रकृति अविक का प्रयोग न रहने पर उसका विग्रह'अविकस्य मांसम्' करना छोड़ दिया, और अवि शब्द से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया। स्त्रीलिङ्ग 'अविका' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद १११२६७;अथर्व २०११२६।१७ और ऋग्वेद १५ खिल ५।१५।५ में मिलता है । अतः ‘अविक' शब्द की सत्ता में कोई सन्देह नहीं हो सकता।
६. 'कानीन' पद की सिद्धि के लिये पाणिनि ने सूत्र रचा हैकन्यायाः कनीन च। इसका अर्थ है-कन्या से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और कन्या को कनीन आदेश हो जाता है ।
वेद में बालक अर्थ में 'कनीन' शब्द का प्रयोग असकृत् उपलब्ध होता है। अवेस्ता में कन्या अर्थ में कनीना का अपभ्रंश 'कइनीन' का प्रयोग मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार 'शवति' मूल प्रकृति का आर्यावर्तीय भाषा में प्रयोग न होने पर भी उससे निष्पन्न
१. भाष्यवचन पक्ष में पतञ्जलि के समय ।
२. तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोरेकेन विग्रहोऽपरस्मादुत्पत्तिर्भविष्यत्यविरविकन्यायेन । तद्यथा—प्रवेमौसमिति विगृह्य अविकशब्दादुत्पत्तिर्भवति आविकमिति । ४।१।१८; ४।२।६०; ४।२।१३१; ५।१।७, २८ इत्यादि ।
३. अष्टा० ४।१।११६॥ ४. द्र० पूर्व पृष्ठ १२, टि. ॥ ५. द्र० पूर्व पृष्ठ १२, टि० ३।
। ३०