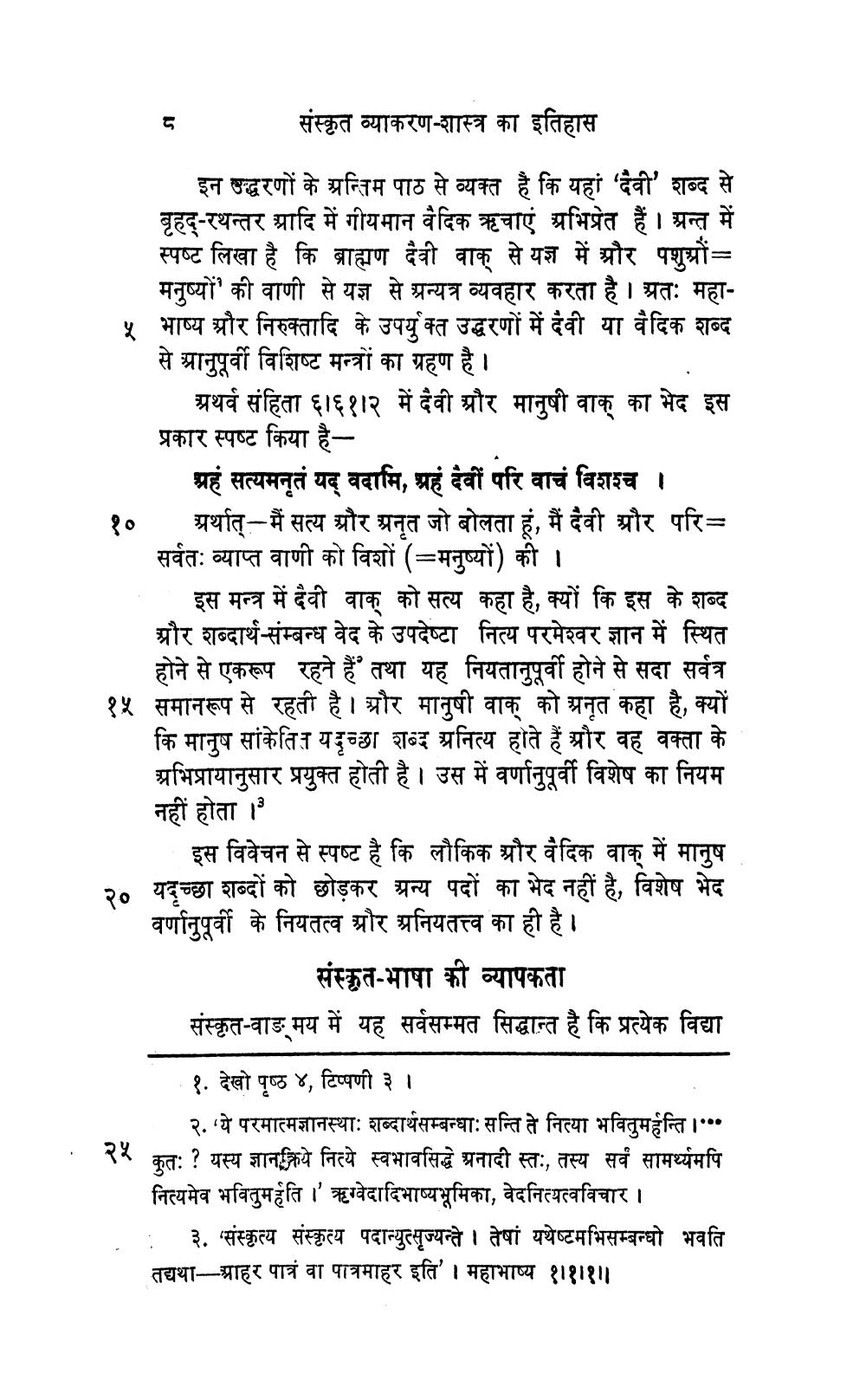________________
US
संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास
इन उद्धरणों के अन्तिम पाठ से व्यक्त है कि यहां 'देवी' शब्द से बृहद्-रथन्तर आदि में गीयमान वैदिक ऋचाएं अभिप्रेत हैं । अन्त में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण दैवी वाक् से यज्ञ में और पशुओं मनुष्यों' की वाणी से यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार करता है । अतः महाभाष्य और निरुक्तादि के उपर्युक्त उद्धरणों में देवी या वैदिक शब्द से प्रानुपूर्वी विशिष्ट मन्त्रों का ग्रहण है ।
अथर्व संहिता ६।६१।२ में देवी और मानुषी वाक् का भेद इस प्रकार स्पष्ट किया है
अहं सत्यमनृतं यद् वदामि, अहं देवीं परि वाचं विशश्च । १० अर्थात् -मैं सत्य और अन्त जो बोलता हूं, मैं देवी और परि=
सर्वतः व्याप्त वाणी को विशों (=मनुष्यों) की । ___इस मन्त्र में दैवी वाक् को सत्य कहा है, क्यों कि इस के शब्द
और शब्दार्थ-संम्बन्ध वेद के उपदेष्टा नित्य परमेश्वर ज्ञान में स्थित होने से एकरूप रहते हैं तथा यह नियतानुपूर्वी होने से सदा सर्वत्र समानरूप से रहती है। और मानुषी वाक् को अनृत कहा है, क्यों कि मानुष सांकेतित यदृच्छा शब्द अनित्य होते हैं और वह वक्ता के अभिप्रायानुसार प्रयुक्त होती है। उस में वर्णानुपूर्वी विशेष का नियम नहीं होता।
____ इस विवेचन से स्पष्ट है कि लौकिक और वैदिक वाक् में मानुष २० यदच्छा शब्दों को छोड़कर अन्य पदों का भेद नहीं है, विशेष भेद वर्णानुपूर्वी के नियतत्व और अनियतत्त्व का ही है।
संस्कृत-भाषा की व्यापकता संस्कृत-वाङमय में यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि प्रत्येक विद्या १. देखो पृष्ठ ४, टिप्पणी ३ ।
२. ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्धाः सन्ति ते नित्या भवितुमर्हन्ति ।... . २५
कुतः ? यस्य ज्ञान क्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे अनादी स्तः, तस्य सर्वं सामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमर्हति ।' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदनित्यत्वविचार । . ३. 'संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्युत्सृज्यन्ते । तेषां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति तद्यथा—आहर पात्रं वा पात्रमाहर इति' । महाभाष्य १११११॥
-