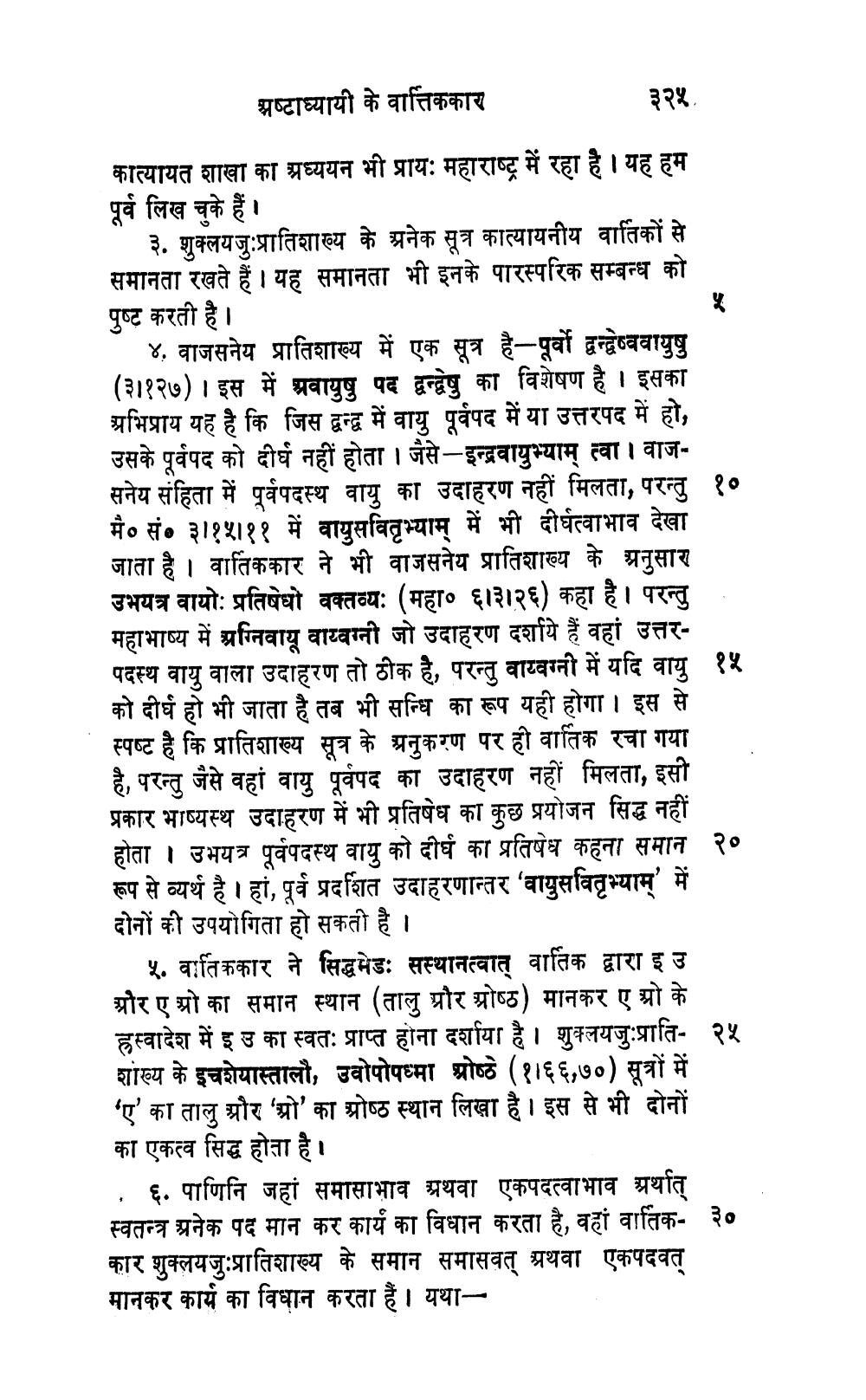________________
अष्टाध्यायी के वार्त्तिककार
३२५.
कात्यायत शाखा का अध्ययन भी प्रायः महाराष्ट्र में रहा है । यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।
३. शुक्लयजुः प्रातिशाख्य के अनेक सूत्र कात्यायनीय वार्तिकों से समानता रखते हैं । यह समानता भी इनके पारस्परिक सम्बन्ध को पुष्ट करती है ।
४, वाजसनेय प्रातिशाख्य में एक सूत्र है - पूर्वो द्वन्द्वेष्ववायुषु ( ३।१२७) । इस में प्रवायुषु पद द्वन्द्वेषु का विशेषण है । इसका अभिप्राय यह है कि जिस द्वन्द्व में वायु पूर्वपद में या उत्तरपद में हो, उसके पूर्वपद को दीर्घ नहीं होता । जैसे - इन्द्रवायुभ्याम् त्वा । वाजसनेय संहिता में पूर्वपदस्थ वायु का उदाहरण नहीं मिलता, परन्तु १० मै० सं० ३ | १५ | ११ में वायुसवितृभ्याम् में भी दीर्घत्वाभाव देखा जाता है । वार्तिककार ने भी वाजसनेय प्रातिशाख्य के अनुसार उभयत्र वायोः प्रतिषेधो वक्तव्य : ( महा० ६ | ३ |२६ ) कहा है । परन्तु महाभाष्य में अग्निवायू वाय्वग्नी जो उदाहरण दर्शाये हैं वहां उत्तरपदस्थ वायु वाला उदाहरण तो ठीक है, परन्तु वाय्वग्नी में यदि वायु १५ दीर्घ हो भी जाता है तब भी सन्धि का रूप यही होगा । इस से स्पष्ट है कि प्रातिशाख्य सूत्र के अनुकरण पर ही वार्तिक रचा गया है, परन्तु जैसे वहां वायु पूर्वपद का उदाहरण नहीं मिलता, इसी प्रकार भाष्यस्थ उदाहरण में भी प्रतिषेध का कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । उभयत्र पूर्वपदस्थ वायु को दीर्घ का प्रतिषेध कहना समान २० रूप से व्यर्थ है। हां, पूर्व प्रदर्शित उदाहरणान्तर 'वायुसवितृभ्याम्' में दोनों की उपयोगिता हो सकती है ।
५. वार्तिककार ने सिद्धमेड : सस्थानत्वात् वार्तिक द्वारा इ उ और ए ओ का समान स्थान ( तालु प्रौर प्रोष्ठ ) मानकर ए ओ के ह्रस्वादेश में इ उ का स्वतः प्राप्त होना दर्शाया है । शुक्लयजुः प्राति- २५ शांख्य के इचशेयास्तालौ, उवोपोपध्मा श्रोष्ठे (१।६६,७०) सूत्रों में 'ए' का तालु और 'प्रो' का प्रोष्ठ स्थान लिखा है । इस से भी दोनों का एकत्व सिद्ध होता है ।
६. पाणिनि जहां समासाभाव अथवा एकपदत्वाभाव अर्थात् स्वतन्त्र अनेक पद मान कर कार्य का विधान करता है, वहां वार्तिक- ३० कार शुक्लयजुः प्रातिशाख्य के समान समासवत् अथवा एकपदवत् मानकर कार्य का विधान करता हैं । यथा