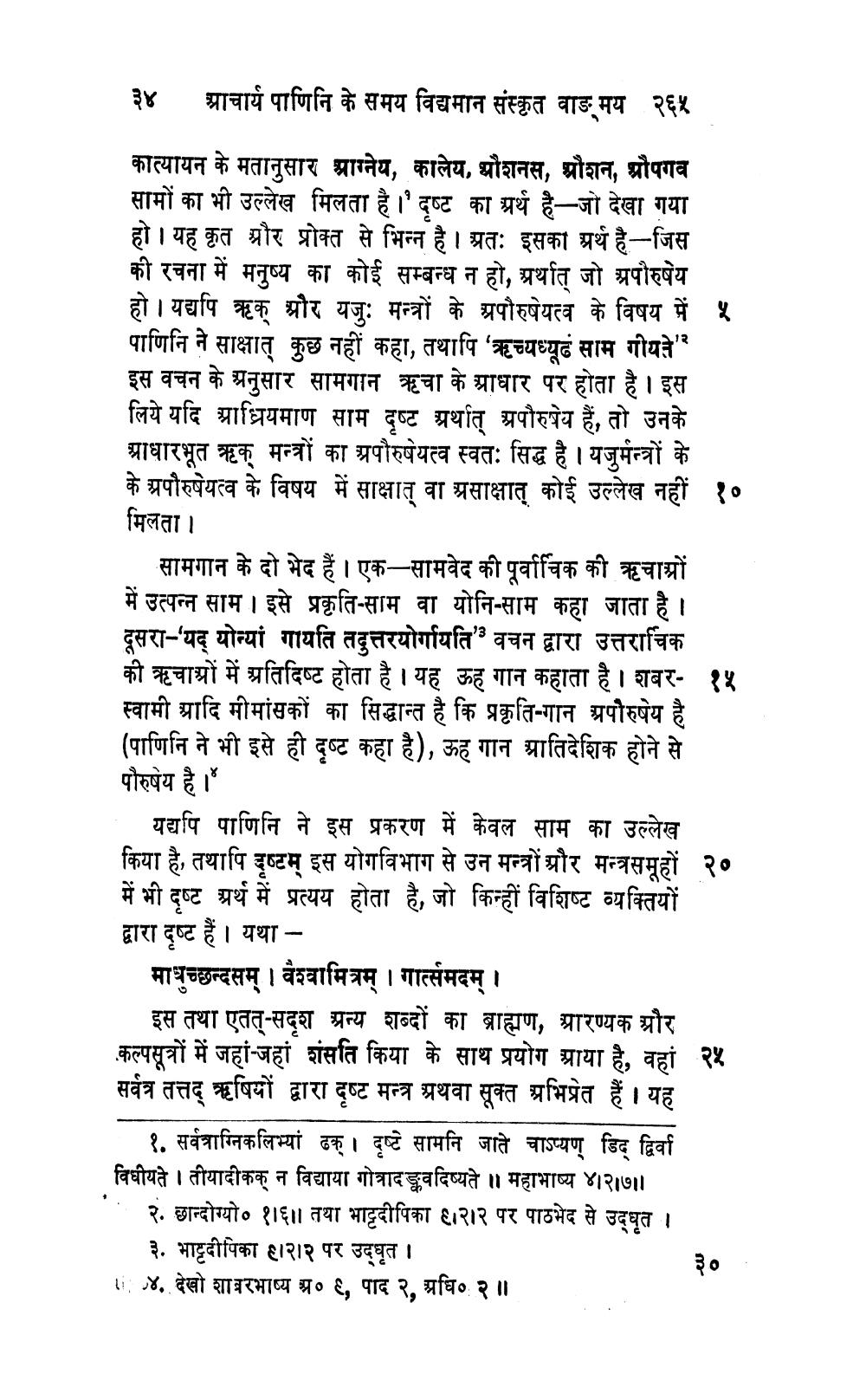________________
३४
आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङमय २६५
कात्यायन के मतानुसार आग्नेय, कालेय, प्रौशनस, प्रौशन, प्रौपगव सामों का भी उल्लेख मिलता है।' दृष्ट का अर्थ है जो देखा गया हो। यह कृत और प्रोक्त से भिन्न है । अतः इसका अर्थ है-जिस की रचना में मनुष्य का कोई सम्बन्ध न हो, अर्थात जो अपौरुषेय हो । यद्यपि ऋक् और यजुः मन्त्रों के अपौरुषेयत्व के विषय में ५ पाणिनि ने साक्षात् कुछ नहीं कहा, तथापि 'ऋच्यध्यूढं साम गीयते'२ इस वचन के अनुसार सामगान ऋचा के आधार पर होता है । इस लिये यदि आध्रियमाण साम दृष्ट अर्थात् अपौरुषेय हैं, तो उनके
आधारभूत ऋक मन्त्रों का अपौरुषेयत्व स्वतः सिद्ध है । यजूमन्त्रों के के अपौरुषेयत्व के विषय में साक्षात् वा असाक्षात् कोई उल्लेख नहीं १० मिलता।
सामगान के दो भेद हैं । एक–सामवेद की पूर्वाचिक की ऋचाओं में उत्पन्न साम । इसे प्रकृति-साम वा योनि-साम कहा जाता है । दूसरा-'यद् योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायति वचन द्वारा उत्तरार्चिक की ऋचाओं में प्रतिदिष्ट होता है । यह ऊह गान कहाता है । शबर- १५ स्वामी आदि मीमांसकों का सिद्धान्त है कि प्रकृति-गान अपौरुषेय है (पाणिनि ने भी इसे ही दृष्ट कहा है), ऊह गान प्रातिदेशिक होने से पौरुषेय है। __ यद्यपि पाणिनि ने इस प्रकरण में केवल साम का उल्लेख किया है, तथापि दृष्टम् इस योगविभाग से उन मन्त्रों और मन्त्रसमूहों २० में भी दृष्ट अर्थ में प्रत्यय होता है, जो किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दृष्ट हैं । यथा - माधुच्छन्दसम् । वैश्वामित्रम् । गामिदम् ।
इस तथा एतत्-सदृश अन्य शब्दों का ब्राह्मण, आरण्यक और कल्पसूत्रों में जहां-जहां शंसति किया के साथ प्रयोग आया है, वहां २५ सर्वत्र तत्तद् ऋषियों द्वारा दृष्ट मन्त्र अथवा सूक्त अभिप्रेत हैं । यह
१. सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढक् । दृष्टे सामनि जाते चाऽप्यण् डिद द्विर्वा विधीयते । तीयादीकक् न विद्याया गोत्रादङ्कवदिष्यते ॥ महाभाष्य ४।२।७॥
२. छान्दोग्यो० ११६॥ तथा भाट्टदीपिका ६।२।२ पर पाठभेद से उद्धृत । ३. भाट्टदीपिका ६।२।२ पर उद्धृत । ४. देखो शावरभाष्य अ० ६, पाद २, अधि० २॥