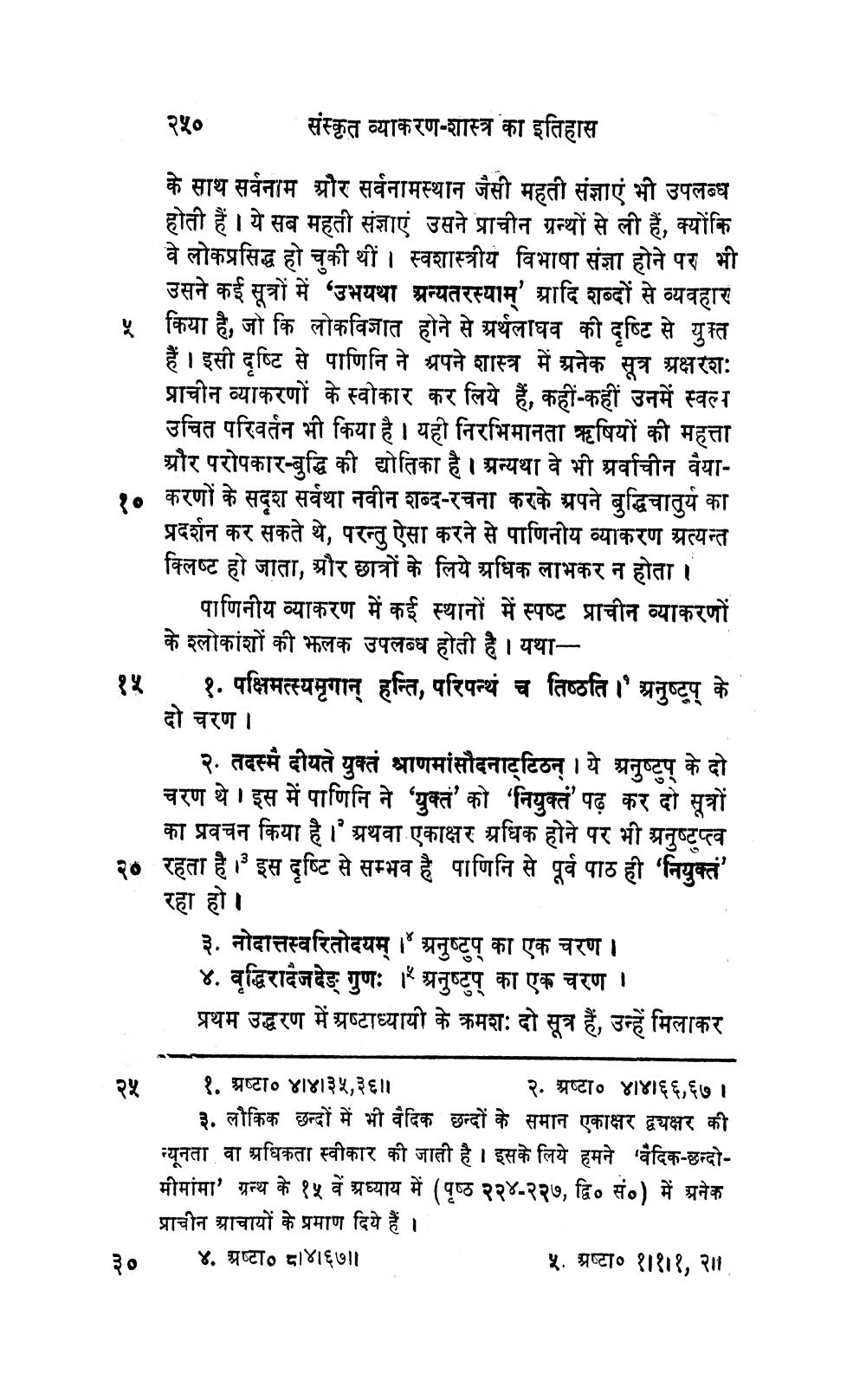________________
२५० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास के साथ सर्वनाम और सर्वनामस्थान जैसी महती संज्ञाएं भी उपलब्ध होती हैं। ये सब महती संज्ञाएं उसने प्राचीन ग्रन्थों से ली हैं, क्योंकि वे लोकप्रसिद्ध हो चुकी थीं। स्वशास्त्रीय विभाषा संज्ञा होने पर भी उसने कई सूत्रों में 'उभयथा अन्यतरस्याम्' आदि शब्दों से व्यवहार किया है, जो कि लोकविज्ञात होने से अर्थलाघव की दृष्टि से युक्त हैं । इसी दृष्टि से पाणिनि ने अपने शास्त्र में अनेक सूत्र अक्षरशः प्राचीन व्याकरणों के स्वीकार कर लिये हैं, कहीं-कहीं उनमें स्वल उचित परिवर्तन भी किया है। यही निरभिमानता ऋषियों की महत्ता और परोपकार-बुद्धि की धोतिका है। अन्यथा वे भी अर्वाचीन वैयाकरणों के सदृश सर्वथा नवीन शब्द-रचना करके अपने बुद्धिचातुर्य का प्रदर्शन कर सकते थे, परन्तु ऐसा करने से पाणिनीय व्याकरण अत्यन्त क्लिष्ट हो जाता, और छात्रों के लिये अधिक लाभकर न होता।
पाणिनीय व्याकरण में कई स्थानों में स्पष्ट प्राचीन व्याकरणों के श्लोकांशों की झलक उपलब्ध होती है । यथा१५ १. पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति, परिपन्थं च तिष्ठति ।' अनुष्टुप् के दो चरण।
२. तदस्मै दीयते युक्तं श्राणमांसौदनाटिठन् । ये अनुष्टुप् के दो चरण थे । इस में पाणिनि ने 'युक्तं' को 'नियुक्त' पढ़ कर दो सूत्रों
का प्रवचन किया है। अथवा एकाक्षर अधिक होने पर भी अनुष्टुप्त्व २० रहता है। इस दृष्टि से सम्भव है पाणिनि से पूर्व पाठ ही 'नियुक्तं' रहा हो।
३. नोदात्तस्वरितोदयम् । अनुष्टुप् का एक चरण । ४. वृद्धिरादैजदे गुणः । अनुष्टुप् का एक चरण । प्रथम उद्धरण में अष्टाध्यायी के क्रमशः दो सूत्र हैं, उन्हें मिलाकर
२५
१. अष्टा० ४।४।३५,३६॥
२. अष्टा० ४।४।६६,६७ । ३. लौकिक छन्दों में भी वैदिक छन्दों के समान एकाक्षर द्वयक्षर की न्यूनता वा अधिकता स्वीकार की जाती है । इसके लिये हमने 'वैदिक-छन्दोमीमांमा' ग्रन्थ के १५ वें अध्याय में (पृष्ठ २२४-२२७, द्वि० सं०) में अनेक प्राचीन आचायों के प्रमाण दिये हैं । ४. अष्टा० ८।४।६७॥
५. अष्टा० १।१।१, २॥
३०