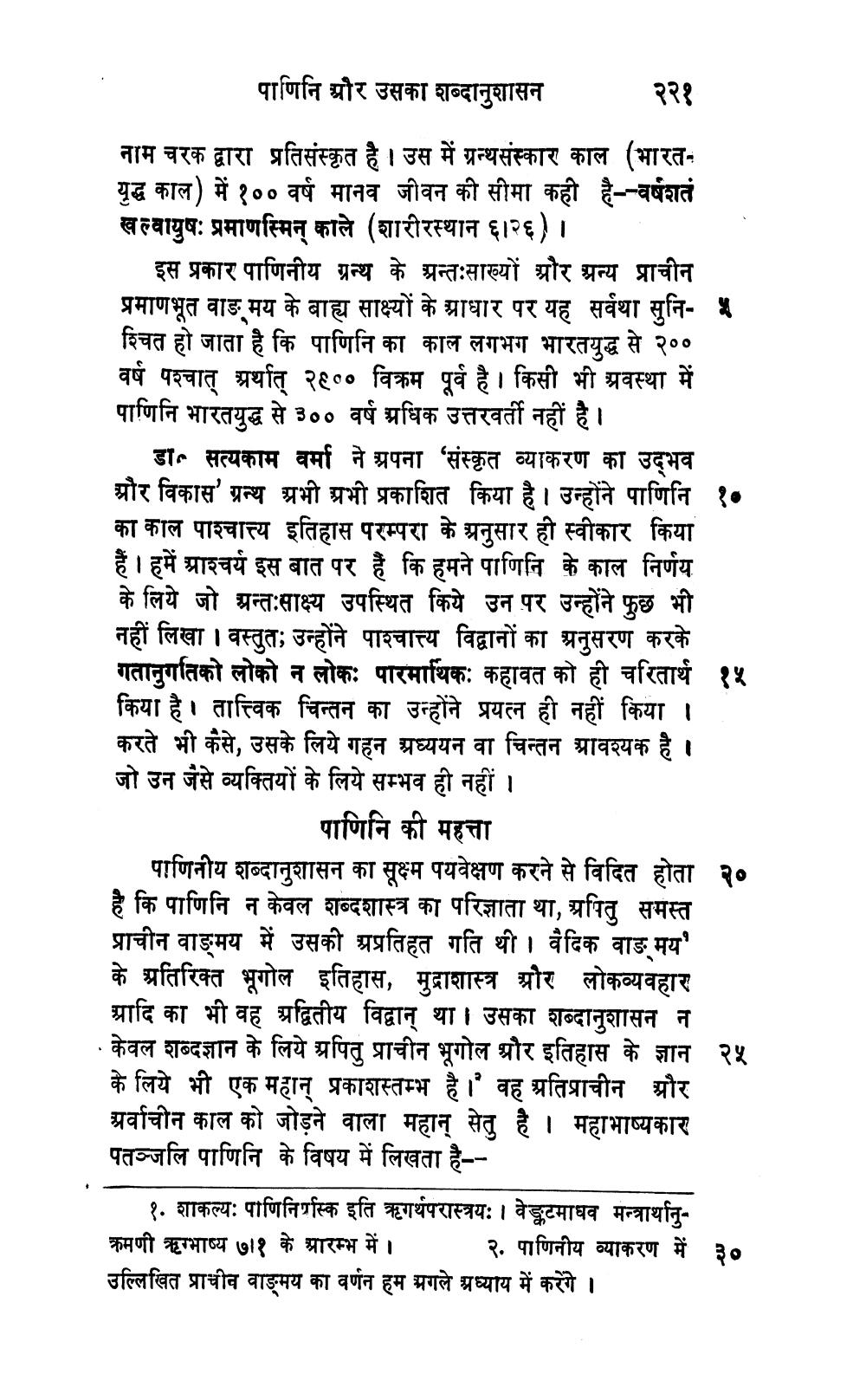________________
पाणिनि और उसका शब्दानुशासन
२२१
नाम चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत है। उस में ग्रन्थसंस्कार काल (भारतयुद्ध काल) में १०० वर्ष मानव जीवन की सीमा कही है--वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणस्मिन् काले (शारीरस्थान ६।२६)।
इस प्रकार पाणिनीय ग्रन्थ के अन्तःसाख्यों और अन्य प्राचीन प्रमाणभूत वाङमय के बाह्य साक्ष्यों के आधार पर यह सर्वथा सुनि- ५ श्चित हो जाता है कि पाणिनि का काल लगभग भारतयुद्ध से २०० वर्ष पश्चात् अर्थात् २६०० विक्रम पूर्व है। किसी भी अवस्था में पाणिनि भारतयुद्ध से 3०० वर्ष अधिक उत्तरवर्ती नहीं है।
डा. सत्यकाम वर्मा ने अपना 'संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास' ग्रन्थ अभी अभी प्रकाशित किया है। उन्होंने पाणिनि १० का काल पाश्चात्त्य इतिहास परम्परा के अनुसार ही स्वीकार किया हैं । हमें आश्चर्य इस बात पर है कि हमने पाणिनि के काल निर्णय के लिये जो अन्तःसाक्ष्य उपस्थित किये उन पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा । वस्तुत: उन्होंने पाश्चात्त्य विद्वानों का अनुसरण करके गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः कहावत को ही चरितार्थ १५ किया है। तात्त्विक चिन्तन का उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया । करते भी कैसे, उसके लिये गहन अध्ययन वा चिन्तन आवश्यक है । जो उन जैसे व्यक्तियों के लिये सम्भव ही नहीं।
पाणिनि की महत्ता पाणिनीय शब्दानुशासन का सूक्ष्म पयवेक्षण करने से विदित होता २० है कि पाणिनि न केवल शब्दशास्त्र का परिज्ञाता था, अपितु समस्त प्राचीन वाङ्मय में उसकी अप्रतिहत गति थी। वैदिक वाङमय' के अतिरिक्त भूगोल इतिहास, मुद्राशास्त्र और लोकव्यवहार आदि का भी वह अद्वितीय विद्वान् था। उसका शब्दानुशासन न केवल शब्दज्ञान के लिये अपितु प्राचीन भूगोल और इतिहास के ज्ञान २५ के लिये भी एक महान् प्रकाशस्तम्भ है।' वह अतिप्राचीन और अर्वाचीन काल को जोड़ने वाला महान् सेतु है । महाभाष्यकार पतञ्जलि पाणिनि के विषय में लिखता है--
१. शाकल्यः पाणिनिर्णस्क इति ऋगर्थपरास्त्रयः । वेङ्कटमाधव मन्त्रार्थानुक्रमणी ऋग्भाष्य ७१ के आरम्भ में। २. पाणिनीय व्याकरण में ३० उल्लिखित प्राचीन वाङ्मय का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे ।