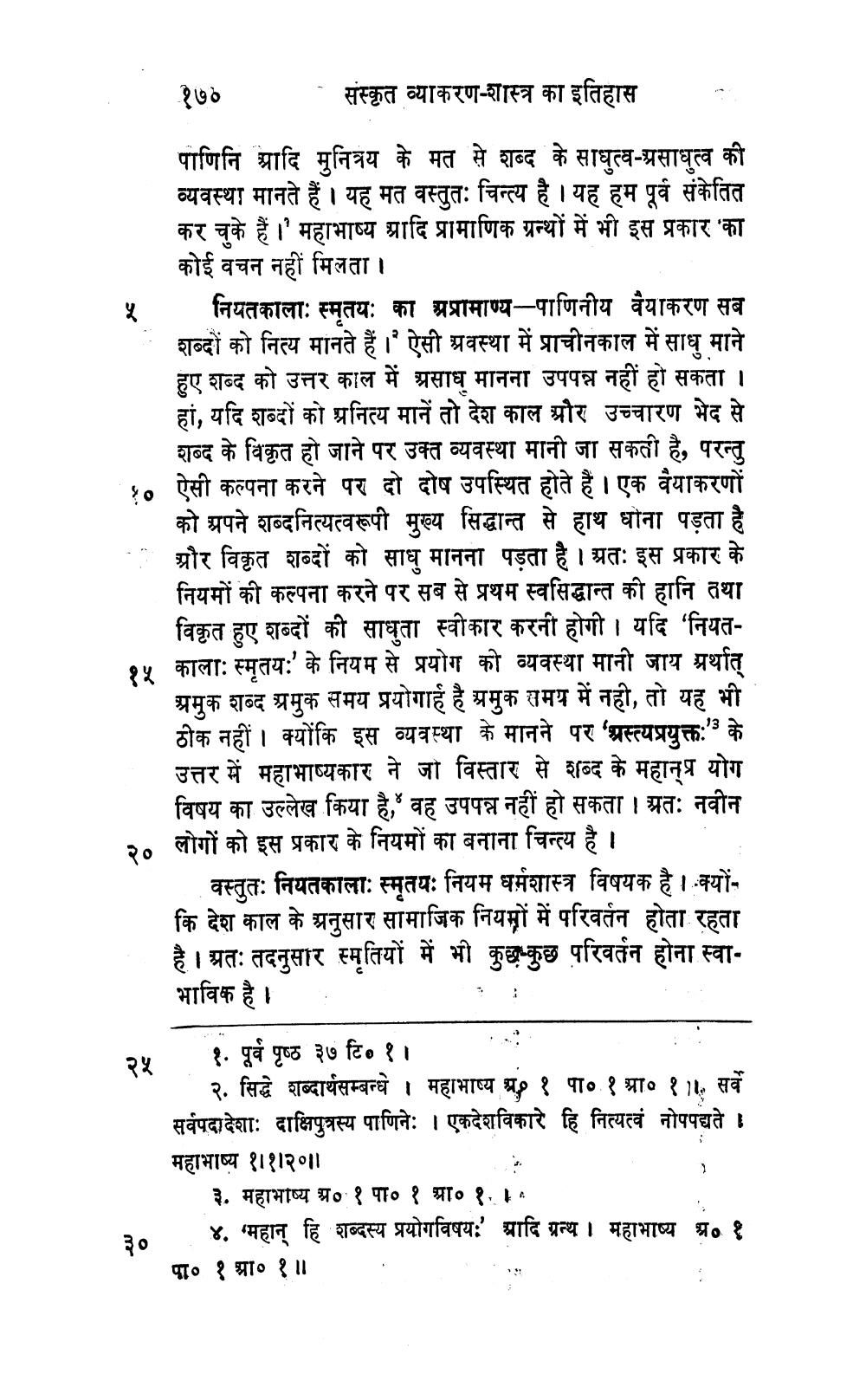________________
१७०
संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास
पाणिनि आदि मुनित्रय के मत से शब्द के साधुत्व-प्रसाधुत्व की व्यवस्था मानते हैं । यह मत वस्तुतः चिन्त्य है । यह हम पूर्व संकेतित कर चुके हैं।' महाभाष्य आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में भी इस प्रकार का कोई वचन नहीं मिलता।
नियतकालाः स्मृतयः का अप्रामाण्य–पाणिनीय वैयाकरण सब शब्दों को नित्य मानते हैं। ऐसी अवस्था में प्राचीनकाल में साधु माने हुए शब्द को उत्तर काल में असाध मानना उपपन्न नहीं हो सकता । हां, यदि शब्दों को प्रनित्य मानें तो देश काल और उच्चारण भेद से शब्द के विकृत हो जाने पर उक्त व्यवस्था मानी जा सकती है, परन्तु ऐसी कल्पना करने पर दो दोष उपस्थित होते हैं । एक वैयाकरणों को अपने शब्दनित्यत्वरूपी मुख्य सिद्धान्त से हाथ धोना पड़ता है और विकृत शब्दों को साधु मानना पड़ता है । अतः इस प्रकार के नियमों की कल्पना करने पर सब से प्रथम स्वसिद्धान्त की हानि तथा
विकृत हुए शब्दों की साधुता स्वीकार करनी होगी। यदि 'नियत१५ कालाः स्मृतयः' के नियम से प्रयोग को व्यवस्था मानी जाय अर्थात्
अमुक शब्द अमुक समय प्रयोगाह है अमुक समय में नही, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि इस व्यवस्था के मानने पर 'अस्त्यप्रयुक्तः' के उत्तर में महाभाष्यकार ने जो विस्तार से शब्द के महान्प्र योग
विषय का उल्लेख किया है, वह उपपन्न नहीं हो सकता । अतः नवीन २० लोगों को इस प्रकार के नियमों का बनाना चिन्त्य है।
वस्तुतः नियतकालाः स्मृतयः नियम धर्मशास्त्र विषयक है। क्योंकि देश काल के अनुसार सामाजिक नियमों में परिवर्तन होता रहता है । अतः तदनुसार स्मृतियों में भी कुछ-कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
२५ १. पूर्व पृष्ठ ३७ टि. १।
२. सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे । महाभाष्य अ १ पा० १ प्रा० १॥ सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते । महाभाष्य १११॥२०॥
३. महाभाष्य अ० १ पा० १ प्रा० १, ।।
४. 'महान् हि शब्दस्य प्रयोगविषयः' आदि ग्रन्थ । महाभाष्य अ०१ पा० १० १॥
३०