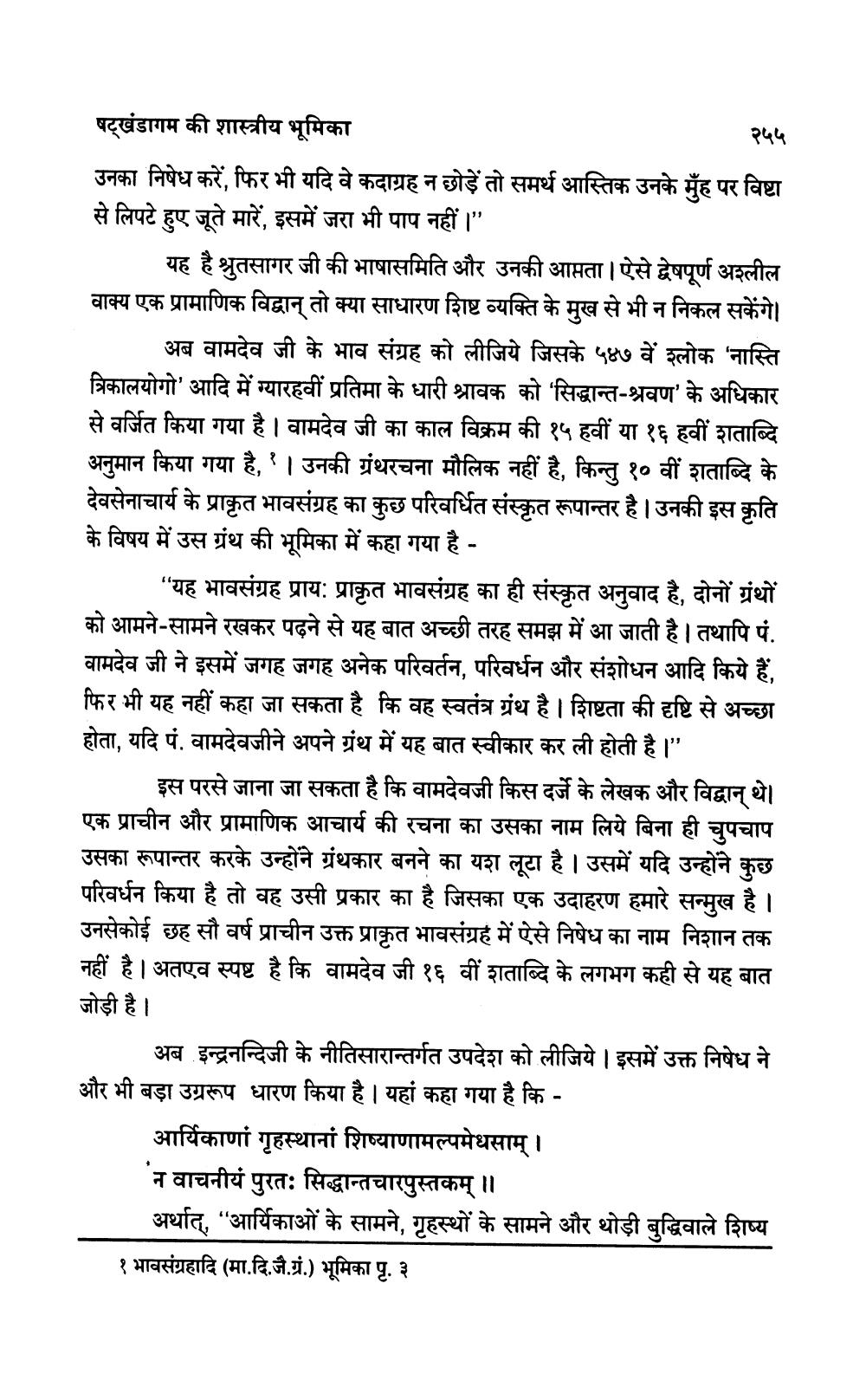________________
षट्खंडागम की शास्त्रीय भूमिका
२५५ उनका निषेध करें, फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़ें तो समर्थ आस्तिक उनके मुँह पर विष्टा से लिपटे हुए जूते मारें, इसमें जरा भी पाप नहीं।"
यह है श्रुतसागर जी की भाषासमिति और उनकी आप्तता । ऐसे द्वेषपूर्ण अश्लील वाक्य एक प्रामाणिक विद्वान् तो क्या साधारण शिष्ट व्यक्ति के मुख से भी न निकल सकेंगे।
अब वामदेव जी के भाव संग्रह को लीजिये जिसके ५४७ वें श्लोक 'नास्ति त्रिकालयोगो' आदि में ग्यारहवीं प्रतिमा के धारी श्रावक को 'सिद्धान्त-श्रवण' के अधिकार से वर्जित किया गया है । वामदेव जी का काल विक्रम की १५ हवीं या १६ हवीं शताब्दि अनुमान किया गया है, ' । उनकी ग्रंथरचना मौलिक नहीं है, किन्तु १० वीं शताब्दि के देवसेनाचार्य के प्राकृत भावसंग्रह का कुछ परिवर्धित संस्कृत रूपान्तर है । उनकी इस कृति के विषय में उस ग्रंथ की भूमिका में कहा गया है -
"यह भावसंग्रह प्राय: प्राकृत भावसंग्रह का ही संस्कृत अनुवाद है, दोनों ग्रंथों को आमने-सामने रखकर पढ़ने से यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है । तथापि पं. वामदेव जी ने इसमें जगह जगह अनेक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन आदि किये हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वह स्वतंत्र ग्रंथ है । शिष्टता की दृष्टि से अच्छा होता, यदि पं. वामदेवजीने अपने ग्रंथ में यह बात स्वीकार कर ली होती है।"
इस परसे जाना जा सकता है कि वामदेवजी किस दर्जे के लेखक और विद्वान् थे। एक प्राचीन और प्रामाणिक आचार्य की रचना का उसका नाम लिये बिना ही चुपचाप उसका रूपान्तर करके उन्होंने ग्रंथकार बनने का यश लूटा है। उसमें यदि उन्होंने कुछ परिवर्धन किया है तो वह उसी प्रकार का है जिसका एक उदाहरण हमारे सन्मुख है । उनसेकोई छह सौ वर्ष प्राचीन उक्त प्राकृत भावसंग्रह में ऐसे निषेध का नाम निशान तक नहीं है। अतएव स्पष्ट है कि वामदेव जी १६ वीं शताब्दि के लगभग कही से यह बात जोड़ी है।
अब इन्द्रनन्दिजी के नीतिसारान्तर्गत उपदेश को लीजिये । इसमें उक्त निषेध ने और भी बड़ा उग्ररूप धारण किया है । यहां कहा गया है कि -
आर्यिकाणां गृहस्थानां शिष्याणामल्पमेधसाम् । न वाचनीयं पुरत: सिद्धान्तचारपुस्तकम् ॥
अर्थात्, “आर्यिकाओं के सामने, गृहस्थों के सामने और थोड़ी बुद्धिवाले शिष्य १ भावसंग्रहादि (मा.दि.जै.ग्रं.) भूमिका पृ. ३