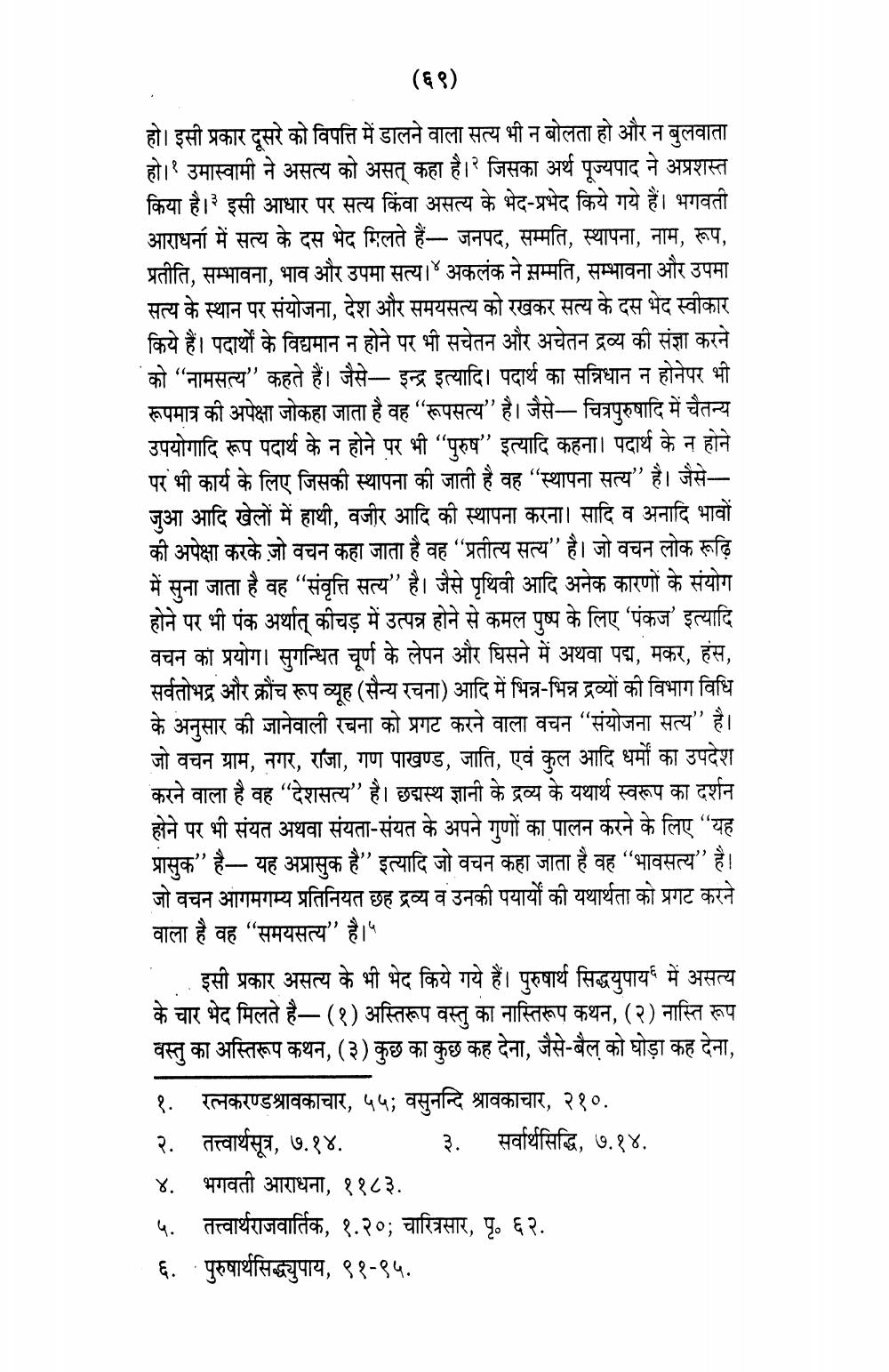________________
(६९) हो। इसी प्रकार दूसरे को विपत्ति में डालने वाला सत्य भी न बोलता हो और न बुलवाता हो।' उमास्वामी ने असत्य को असत् कहा है। जिसका अर्थ पूज्यपाद ने अप्रशस्त किया है। इसी आधार पर सत्य किंवा असत्य के भेद-प्रभेद किये गये हैं। भगवती आराधना में सत्य के दस भेद मिलते हैं- जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीति, सम्भावना, भाव और उपमा सत्य। अकलंक ने सम्मति, सम्भावना और उपमा सत्य के स्थान पर संयोजना, देश और समयसत्य को रखकर सत्य के दस भेद स्वीकार किये हैं। पदार्थों के विद्यमान न होने पर भी सचेतन और अचेतन द्रव्य की संज्ञा करने को “नामसत्य' कहते हैं। जैसे- इन्द्र इत्यादि। पदार्थ का सन्निधान न होनेपर भी रूपमात्र की अपेक्षा जोकहा जाता है वह “रूपसत्य” है। जैसे- चित्रपुरुषादि में चैतन्य उपयोगादि रूप पदार्थ के न होने पर भी “पुरुष' इत्यादि कहना। पदार्थ के न होने पर भी कार्य के लिए जिसकी स्थापना की जाती है वह “स्थापना सत्य' है। जैसेजुआ आदि खेलों में हाथी, वजीर आदि की स्थापना करना। सादि व अनादि भावों की अपेक्षा करके जो वचन कहा जाता है वह “प्रतीत्य सत्य' है। जो वचन लोक रूढ़ि में सुना जाता है वह “संवृत्ति सत्य' है। जैसे पृथिवी आदि अनेक कारणों के संयोग होने पर भी पंक अर्थात् कीचड़ में उत्पन्न होने से कमल पुष्प के लिए 'पंकज' इत्यादि वचन का प्रयोग। सुगन्धित चूर्ण के लेपन और घिसने में अथवा पद्म, मकर, हंस, सर्वतोभद्र और क्रौंच रूप व्यूह (सैन्य रचना) आदि में भिन्न-भिन्न द्रव्यों की विभाग विधि के अनुसार की जानेवाली रचना को प्रगट करने वाला वचन “संयोजना सत्य' है। जो वचन ग्राम, नगर, राजा, गण पाखण्ड, जाति, एवं कुल आदि धर्मों का उपदेश करने वाला है वह “देशसत्य' है। छद्मस्थ ज्ञानी के द्रव्य के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होने पर भी संयत अथवा संयता-संयत के अपने गुणों का पालन करने के लिए “यह प्रासुक" है- यह अप्रासुक है" इत्यादि जो वचन कहा जाता है वह "भावसत्य” है। जो वचन आगमगम्य प्रतिनियत छह द्रव्य व उनकी पयार्यों की यथार्थता को प्रगट करने वाला है वह “समयसत्य' है। - इसी प्रकार असत्य के भी भेद किये गये हैं। पुरुषार्थ सिद्धयुपायर्प में असत्य के चार भेद मिलते है- (१) अस्तिरूप वस्तु का नास्तिरूप कथन, (२) नास्ति रूप वस्तु का अस्तिरूप कथन, (३) कुछ का कुछ कह देना, जैसे-बैल को घोड़ा कह देना, १. रत्नकरण्डश्रावकाचार, ५५; वसुनन्दि श्रावकाचार, २१०. २. तत्त्वार्थसूत्र, ७.१४. ३. सर्वार्थसिद्धि, ७.१४. ४. भगवती आराधना, ११८३. ५. तत्त्वार्थराजवार्तिक, १.२०; चारित्रसार, पृ. ६२. ६. · पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, ९१-९५.