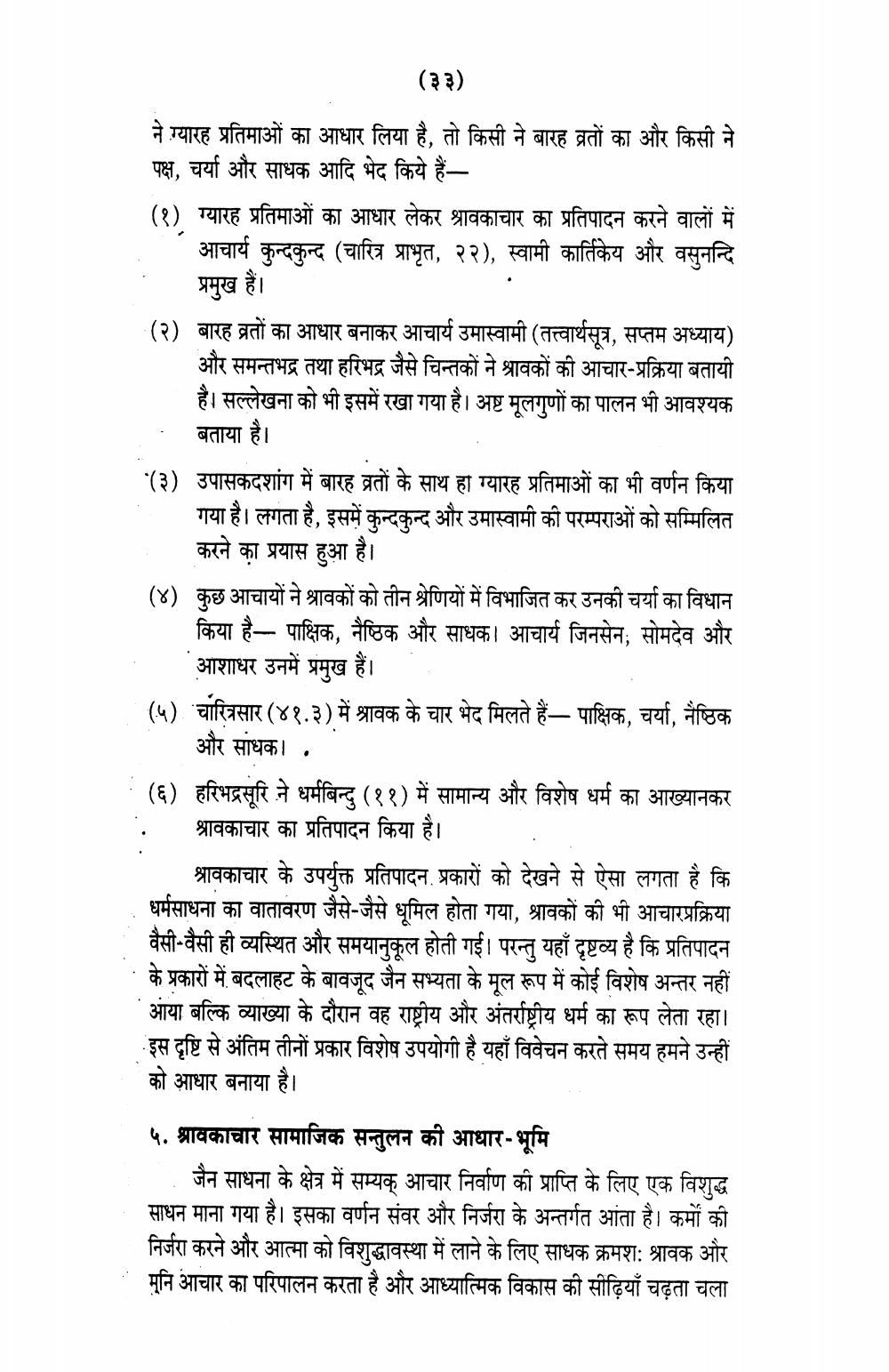________________
(३३)
ने ग्यारह प्रतिमाओं का आधार लिया है, तो किसी ने बारह व्रतों का और किसी ने पक्ष, चर्या और साधक आदि भेद किये हैं(१) ग्यारह प्रतिमाओं का आधार लेकर श्रावकाचार का प्रतिपादन करने वालों में
आचार्य कुन्दकुन्द (चारित्र प्राभृत, २२), स्वामी कार्तिकेय और वसुनन्दि
प्रमुख हैं। (२) बारह व्रतों का आधार बनाकर आचार्य उमास्वामी (तत्त्वार्थसूत्र, सप्तम अध्याय)
और समन्तभद्र तथा हरिभद्र जैसे चिन्तकों ने श्रावकों की आचार-प्रक्रिया बतायी है। सल्लेखना को भी इसमें रखा गया है। अष्ट मूलगुणों का पालन भी आवश्यक
बताया है। (३) उपासकदशांग में बारह व्रतों के साथ हा ग्यारह प्रतिमाओं का भी वर्णन किया
गया है। लगता है, इसमें कुन्दकुन्द और उमास्वामी की परम्पराओं को सम्मिलित
करने का प्रयास हुआ है। (४) कुछ आचायों ने श्रावकों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर उनकी चर्या का विधान
किया है- पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। आचार्य जिनसेन, सोमदेव और
आशाधर उनमें प्रमुख हैं। (५) चारित्रसार (४१.३) में श्रावक के चार भेद मिलते हैं— पाक्षिक, चर्या, नैष्ठिक
और साधक। . (६) हरिभद्रसूरि ने धर्मबिन्द (११) में सामान्य और विशेष धर्म का आख्यानकर
श्रावकाचार का प्रतिपादन किया है।
श्रावकाचार के उपर्युक्त प्रतिपादन प्रकारों को देखने से ऐसा लगता है कि धर्मसाधना का वातावरण जैसे-जैसे धूमिल होता गया, श्रावकों की भी आचारप्रक्रिया वैसी-वैसी ही व्यस्थित और समयानुकूल होती गई। परन्तु यहाँ दृष्टव्य है कि प्रतिपादन के प्रकारों में बदलाहट के बावजूद जैन सभ्यता के मूल रूप में कोई विशेष अन्तर नहीं आया बल्कि व्याख्या के दौरान वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धर्म का रूप लेता रहा। इस दृष्टि से अंतिम तीनों प्रकार विशेष उपयोगी है यहाँ विवेचन करते समय हमने उन्हीं को आधार बनाया है। ५. श्रावकाचार सामाजिक सन्तुलन की आधार-भूमि
जैन साधना के क्षेत्र में सम्यक् आचार निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक विशुद्ध साधन माना गया है। इसका वर्णन संवर और निर्जरा के अन्तर्गत आता है। कर्मों की निर्जरा करने और आत्मा को विशुद्धावस्था में लाने के लिए साधक क्रमशः श्रावक और मुनि आचार का परिपालन करता है और आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता चला