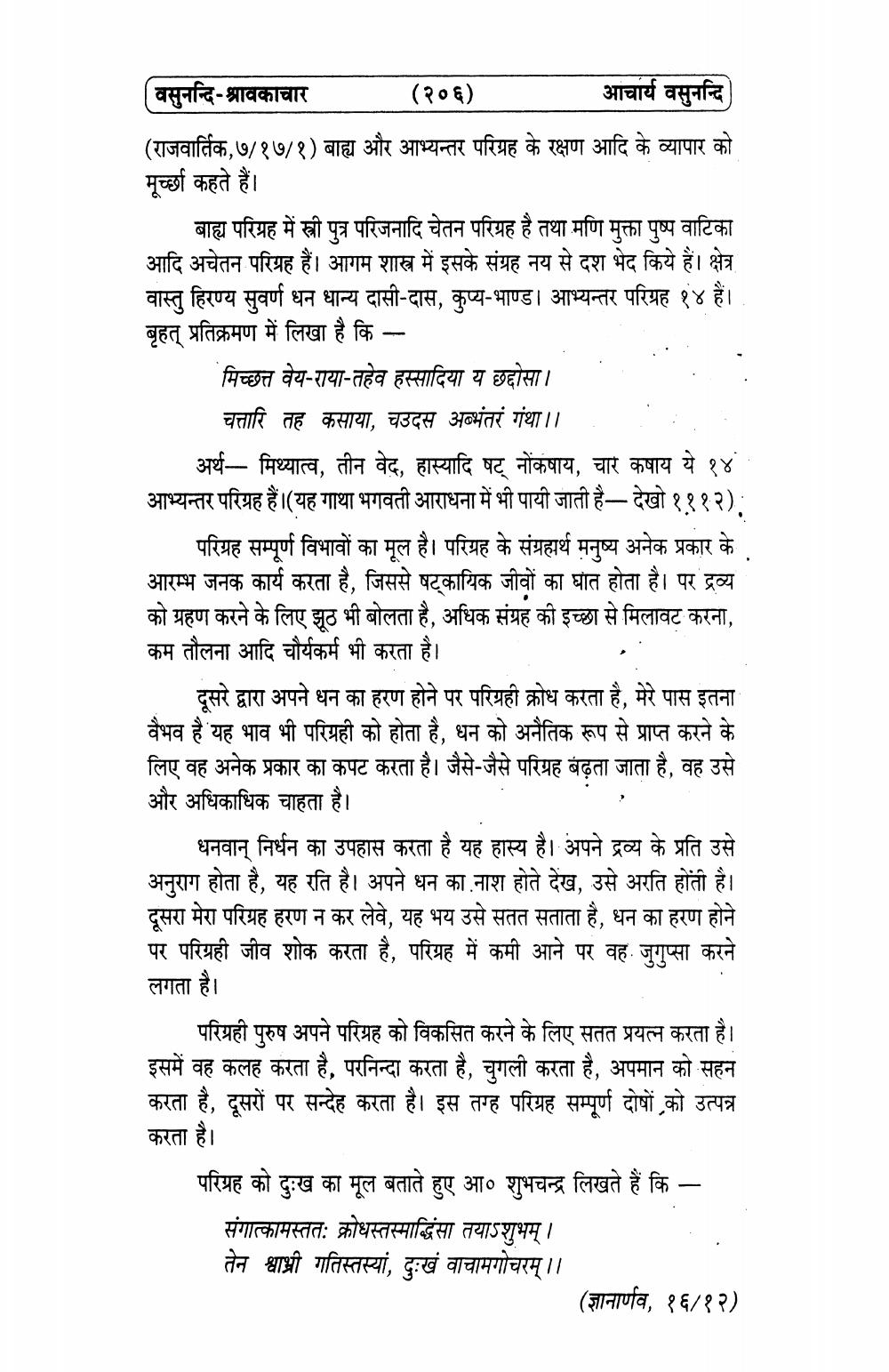________________
(वसुनन्दि-श्रावकाचार (२०६)
आचार्य वसुनन्दि) (राजवार्तिक,७/१७/१) बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह के रक्षण आदि के व्यापार को मूर्छा कहते हैं। ___ बाह्य परिग्रह में स्त्री पुत्र परिजनादि चेतन परिग्रह है तथा मणि मुक्ता पुष्प वाटिका आदि अचेतन परिग्रह हैं। आगम शास्त्र में इसके संग्रह नय से दश भेद किये हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी-दास, कुष्य-भाण्ड। आभ्यन्तर परिग्रह १४ हैं। बृहत् प्रतिक्रमण में लिखा है कि -
मिच्छत्त वेय-राया-तहेव हस्सादिया य छद्दोसा।
चत्तारि तह कसाया, चउदस अब्भंतरं गंथा।।
अर्थ- मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्यादि षट् नोंकषाय, चार कषाय ये १४ आभ्यन्तर परिग्रह हैं।(यह गाथा भगवती आराधना में भी पायी जाती है- देखो १.११२)
परिग्रह सम्पूर्ण विभावों का मूल है। परिग्रह के संग्रहार्थ मनुष्य अनेक प्रकार के आरम्भ जनक कार्य करता है, जिससे षट्कायिक जीवों का घात होता है। पर द्रव्य को ग्रहण करने के लिए झूठ भी बोलता है, अधिक संग्रह की इच्छा से मिलावट करना, कम तौलना आदि चौर्यकर्म भी करता है।
दूसरे द्वारा अपने धन का हरण होने पर परिग्रही क्रोध करता है, मेरे पास इतना वैभव है यह भाव भी परिग्रही को होता है, धन को अनैतिक रूप से प्राप्त करने के लिए वह अनेक प्रकार का कपट करता है। जैसे-जैसे परिग्रह बढ़ता जाता है, वह उसे और अधिकाधिक चाहता है।
धनवान् निर्धन का उपहास करता है यह हास्य है। अपने द्रव्य के प्रति उसे अनुराग होता है, यह रति है। अपने धन का नाश होते देख, उसे अरति होती है। दूसरा मेरा परिग्रह हरण न कर लेवे, यह भय उसे सतत सताता है, धन का हरण होने पर परिग्रही जीव शोक करता है, परिग्रह में कमी आने पर वह जुगुप्सा करने लगता है।
परिग्रही पुरुष अपने परिग्रह को विकसित करने के लिए सतत प्रयत्न करता है। इसमें वह कलह करता है, परनिन्दा करता है, चुगली करता है, अपमान को सहन करता है, दूसरों पर सन्देह करता है। इस तरह परिग्रह सम्पूर्ण दोषों को उत्पन्न करता है। परिग्रह को दुःख का मूल बताते हुए आ० शुभचन्द्र लिखते हैं कि -
संगात्कामस्तत: क्रोधस्तस्माद्धिंसा तयाऽशुभम् । तेन श्वाभ्री गतिस्तस्यां, दुःखं वाचामगोचरम् ।।
(ज्ञानार्णव, १६/१२)