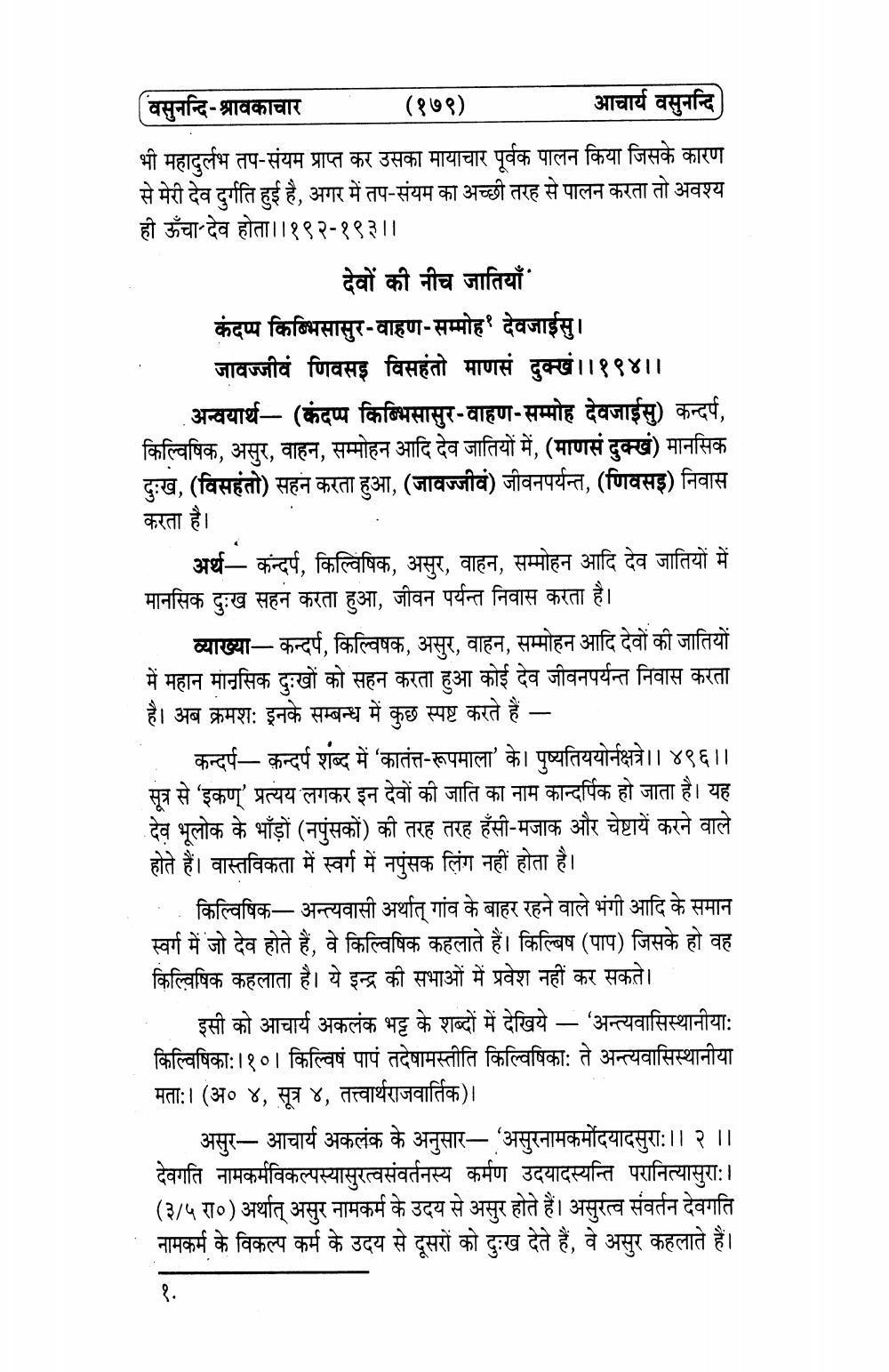________________
विसुनन्दि-श्रावकाचार (१७९)
आचार्य वसुनन्दि) भी महादुर्लभ तप-संयम प्राप्त कर उसका मायाचार पूर्वक पालन किया जिसके कारण से मेरी देव दुर्गति हुई है, अगर में तप-संयम का अच्छी तरह से पालन करता तो अवश्य ही ऊँचा देव होता।। १९२-१९३ ।।
देवों की नीच जातियाँ कंदप्य किन्भिसासुर-वाहण-सम्मोह देवजाईसु।
जावज्जीवं णिवसइ विसहंतो माणसं दुक्खं ।। १९४।।
अन्वयार्थ– (कंदप्प किन्भिसासुर-वाहण-सम्मोह देवजाईसु) कन्दर्प, किल्विषिक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देव जातियों में, (माणसं दुक्खं) मानसिक दुःख, (विसहंतो) सहन करता हुआ, (जावज्जीव) जीवनपर्यन्त, (णिवसइ) निवास करता है।
अर्थ- कन्दर्प, किल्विंषिक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देव जातियों में मानसिक दुःख सहन करता हुआ, जीवन पर्यन्त निवास करता है। ___व्याख्या- कन्दर्प, किल्विषक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देवों की जातियों में महान मानसिक दुःखों को सहन करता हुआ कोई देव जीवनपर्यन्त निवास करता है। अब क्रमश: इनके सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट करते हैं - . कन्दर्प- कन्दर्प शब्द में 'कातंत्त-रूपमाला' के। पुष्यतिययोर्नक्षत्रे।। ४९६।। सूत्र से 'इकण्' प्रत्यय लगकर इन देवों की जाति का नाम कान्दर्पिक हो जाता है। यह देव भूलोक के भाँड़ों (नपुंसकों) की तरह तरह हँसी-मजाक और चेष्टायें करने वाले होते हैं। वास्तविकता में स्वर्ग में नपुंसक लिंग नहीं होता है।
किल्विषिक- अन्त्यवासी अर्थात् गांव के बाहर रहने वाले भंगी आदि के समान स्वर्ग में जो देव होते हैं, वे किल्विषिक कहलाते हैं। किल्बिष (पाप) जिसके हो वह किल्विषिक कहलाता है। ये इन्द्र की सभाओं में प्रवेश नहीं कर सकते।
___ इसी को आचार्य अकलंक भट्ट के शब्दों में देखिये - ‘अन्त्यवासिस्थानीयाः किल्विषिकाः।१०। किल्विषं पापं तदेषामस्तीति किल्विषिका: ते अन्त्यवासिस्थानीया मताः। (अ० ४, सूत्र ४, तत्त्वार्थराजवार्तिक)। ___असुर- आचार्य अकलंक के अनुसार- ‘असुरनामकर्मोदयादसुराः।। २ ।। देवगति नामकर्मविकल्पस्यासुरत्वसंवर्तनस्य कर्मण उदयादस्यन्ति परानित्यासुराः। (३/५ रा०) अर्थात् असुर नामकर्म के उदय से असुर होते हैं। असुरत्व संवर्तन देवगति नामकर्म के विकल्प कर्म के उदय से दूसरों को दुःख देते हैं, वे असुर कहलाते हैं।