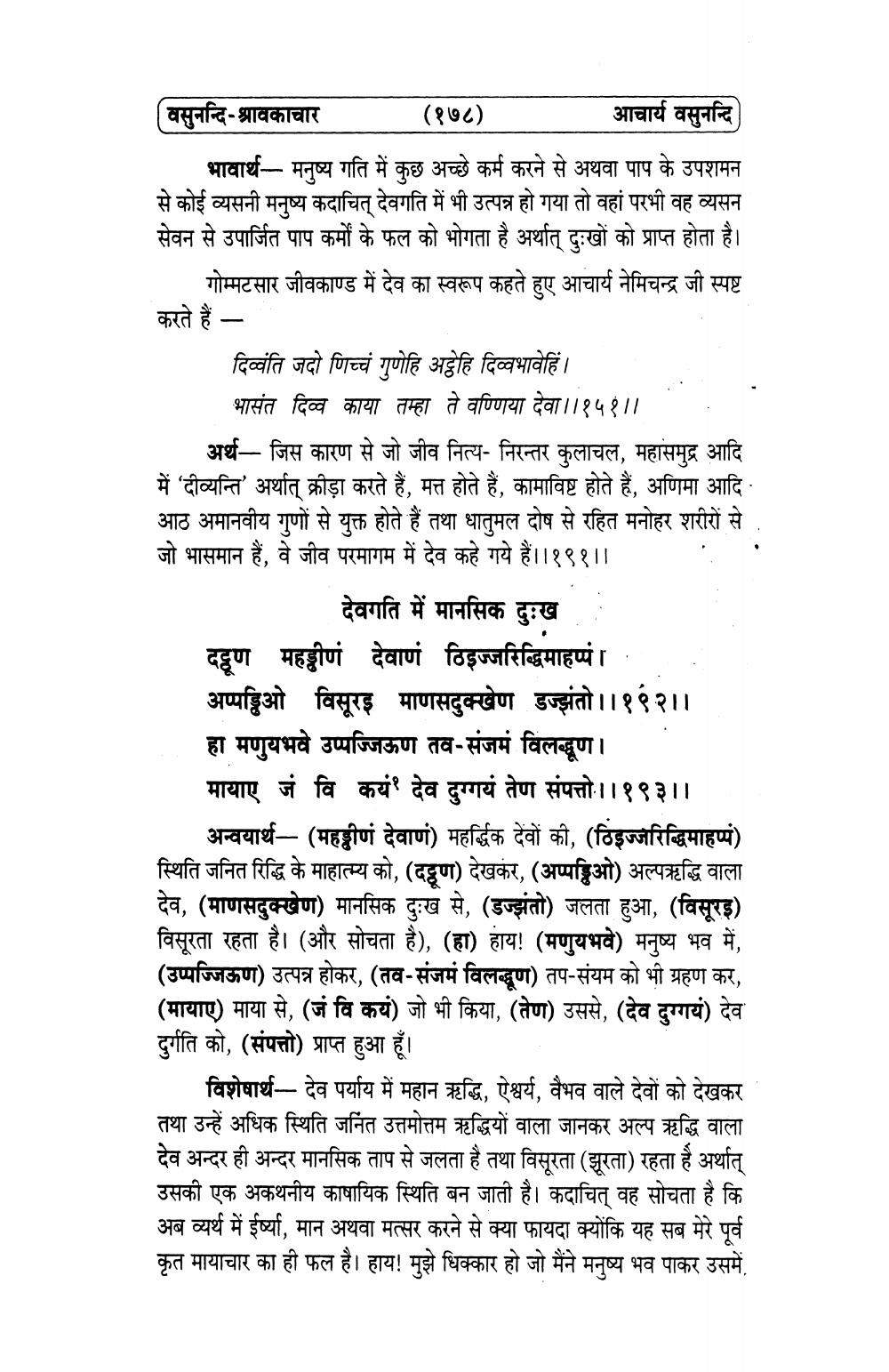________________
(वसुनन्दि-श्रावकाचार (१७८)
आचार्य वसुनन्दि भावार्थ- मनुष्य गति में कुछ अच्छे कर्म करने से अथवा पाप के उपशमन से कोई व्यसनी मनुष्य कदाचित् देवगति में भी उत्पन्न हो गया तो वहां परभी वह व्यसन सेवन से उपार्जित पाप कर्मों के फल को भोगता है अर्थात् दुःखों को प्राप्त होता है। ____ गोम्मटसार जीवकाण्ड में देव का स्वरूप कहते हुए आचार्य नेमिचन्द्र जी स्पष्ट करते हैं -
दिव्वंति जदो णिच्चं गुणेहि अट्ठहि दिव्वभावेहिं ।
भासंत दिव्व काया तम्हा ते वण्णिया देवा।।१५१।।
अर्थ- जिस कारण से जो जीव नित्य- निरन्तर कुलाचल, महासमुद्र आदि में 'दीव्यन्ति' अर्थात् क्रीड़ा करते हैं, मत्त होते हैं, कामाविष्ट होते हैं, अणिमा आदि . आठ अमानवीय गुणों से युक्त होते हैं तथा धातुमल दोष से रहित मनोहर शरीरों से . जो भासमान हैं, वे जीव परमागम में देव कहे गये हैं। । १९१।।
देवगति में मानसिक दुःख दगुण महड्डीणं देवाणं ठिइज्जरिद्धिमाहप्पं । अप्पड्डिओ विसूरइ माणसदुक्खेण डझंतो।। १९२।। हा मणुयभवे उप्पज्जिऊण तव-संजमं विलद्भूण। मायाए जं वि कयं देव दुग्गयं तेण संपत्तो।।१९३।।
अन्वयार्थ- (महड्डीणं देवाणं) महर्द्धिक देवों की, (ठिइज्जरिद्धिमाहप्पं) स्थिति जनित रिद्धि के माहात्म्य को, (दट्ठण) देखकर, (अप्पटिओ) अल्पऋद्धि वाला देव, (माणसदुक्खेण) मानसिक दुःख से, (डझंतो) जलता हुआ, (विसूरइ) विसूरता रहता है। (और सोचता है), (हा) हाय! (मणुयभवे) मनुष्य भव में, (उप्पज्जिऊण) उत्पन्न होकर, (तव-संजमं विलखूण) तप-संयम को भी ग्रहण कर, (मायाए) माया से, (जं वि कयं) जो भी किया, (तेण) उससे, (देव दुग्गयं) देव दुर्गति को, (संपत्तो) प्राप्त हुआ हूँ।
विशेषार्थ- देव पर्याय में महान ऋद्धि, ऐश्वर्य, वैभव वाले देवों को देखकर तथा उन्हें अधिक स्थिति जनित उत्तमोत्तम ऋद्धियों वाला जानकर अल्प ऋद्धि वाला देव अन्दर ही अन्दर मानसिक ताप से जलता है तथा विसूरता (झूरता) रहता है अर्थात् उसकी एक अकथनीय काषायिक स्थिति बन जाती है। कदाचित् वह सोचता है कि अब व्यर्थ में ईर्ष्या, मान अथवा मत्सर करने से क्या फायदा क्योंकि यह सब मेरे पूर्व कृत मायाचार का ही फल है। हाय! मुझे धिक्कार हो जो मैंने मनुष्य भव पाकर उसमें,