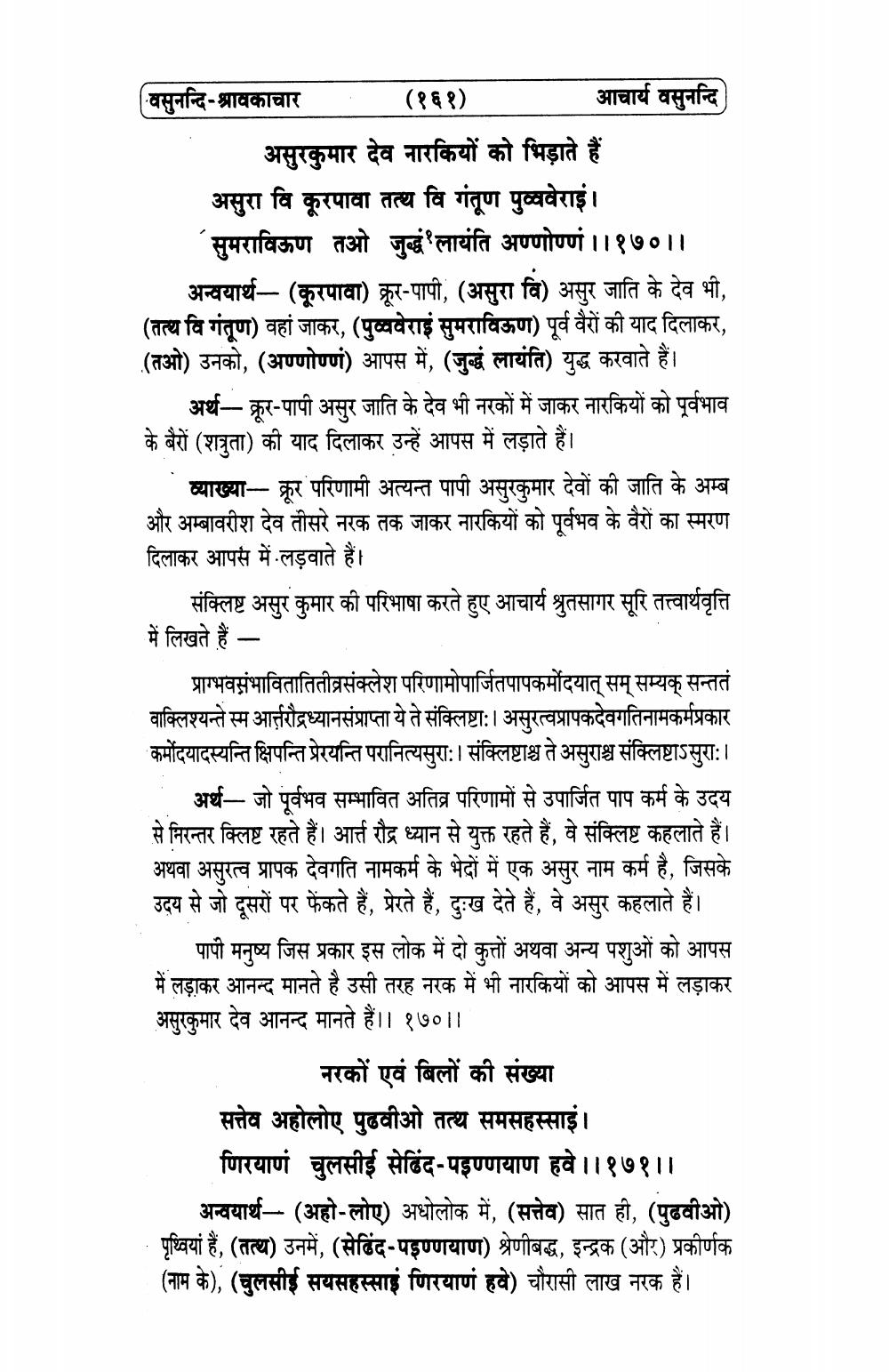________________
वसुनन्दि-श्रावकाचार (१६१) आचार्य वसुनन्दि
असुरकुमार देव नारकियों को भिड़ाते हैं असुरा वि कूरपावा तत्थ वि गंतूण पुष्ववेराई।
सुमराविऊण तओ जुद्धं लायंति अण्णोण्णं ।। १७० ।। अन्वयार्थ— (कूरपावा) क्रूर-पापी, (असुरा वि) असुर जाति के देव भी, (तत्थ वि गंतूण) वहां जाकर, (पुव्ववेराई सुमराविऊण) पूर्व वैरों की याद दिलाकर, (तओ) उनको, (अण्णोण्णं) आपस में, (जुद्धं लायंति) युद्ध करवाते हैं। ____ अर्थ- क्रूर-पापी असुर जाति के देव भी नरकों में जाकर नारकियों को पूर्वभाव के बैरों (शत्रुता) की याद दिलाकर उन्हें आपस में लड़ाते हैं।
व्याख्या- क्रूर परिणामी अत्यन्त पापी असुरकुमार देवों की जाति के अम्ब और अम्बावरीश देव तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को पूर्वभव के वैरों का स्मरण दिलाकर आपस में लड़वाते हैं।
संक्लिष्ट असुर कुमार की परिभाषा करते हुए आचार्य श्रुतसागर सूरि तत्त्वार्थवृत्ति में लिखते हैं -
प्राग्भवसंभावितातितीव्रसंक्लेश परिणामोपार्जितपापकर्मोदयात् सम् सम्यक् सन्ततं वाक्लिश्यन्ते स्म आर्तरौद्रध्यानसंप्राप्ता ये ते संक्लिष्टाः । असुरत्वप्रापकदेवगतिनामकर्मप्रकार कर्मोदयादस्यन्ति क्षिपन्ति प्रेरयन्ति परानित्यसुराः । संक्लिष्टाश्च ते असुराश्च संक्लिष्टाऽसुराः । - अर्थ- जो पूर्वभव सम्भावित अतिव्र परिणामों से उपार्जित पाप कर्म के उदय से निरन्तर क्लिष्ट रहते हैं। आर्त रौद्र ध्यान से युक्त रहते हैं, वे संक्लिष्ट कहलाते हैं। अथवा असुरत्व प्रापक देवगति नामकर्म के भेदों में एक असुर नाम कर्म है, जिसके उदय से जो दूसरों पर फेंकते हैं, प्रेरते हैं, दुःख देते हैं, वे असुर कहलाते हैं।
पापी मनुष्य जिस प्रकार इस लोक में दो कुत्तों अथवा अन्य पशुओं को आपस में लड़ाकर आनन्द मानते है उसी तरह नरक में भी नारकियों को आपस में लड़ाकर असुरकुमार देव आनन्द मानते हैं।। १७०।।
नरकों एवं बिलों की संख्या सत्तेव अहोलोए पुढवीओ तत्थ समसहस्साइं। णिरयाणं चुलसीई सेटिंद-पइण्णयाण हवे ।। १७१।।
अन्वयार्थ- (अहो-लोए) अधोलोक में, (सत्तेव) सात ही, (पुढवीओ) पृथ्वियां हैं, (तत्थ) उनमें, (सेढिंद-पइण्णयाण) श्रेणीबद्ध, इन्द्रक (और) प्रकीर्णक (नाम के), (चुलसीई सयसहस्साई णिरयाणं हवे) चौरासी लाख नरक हैं।