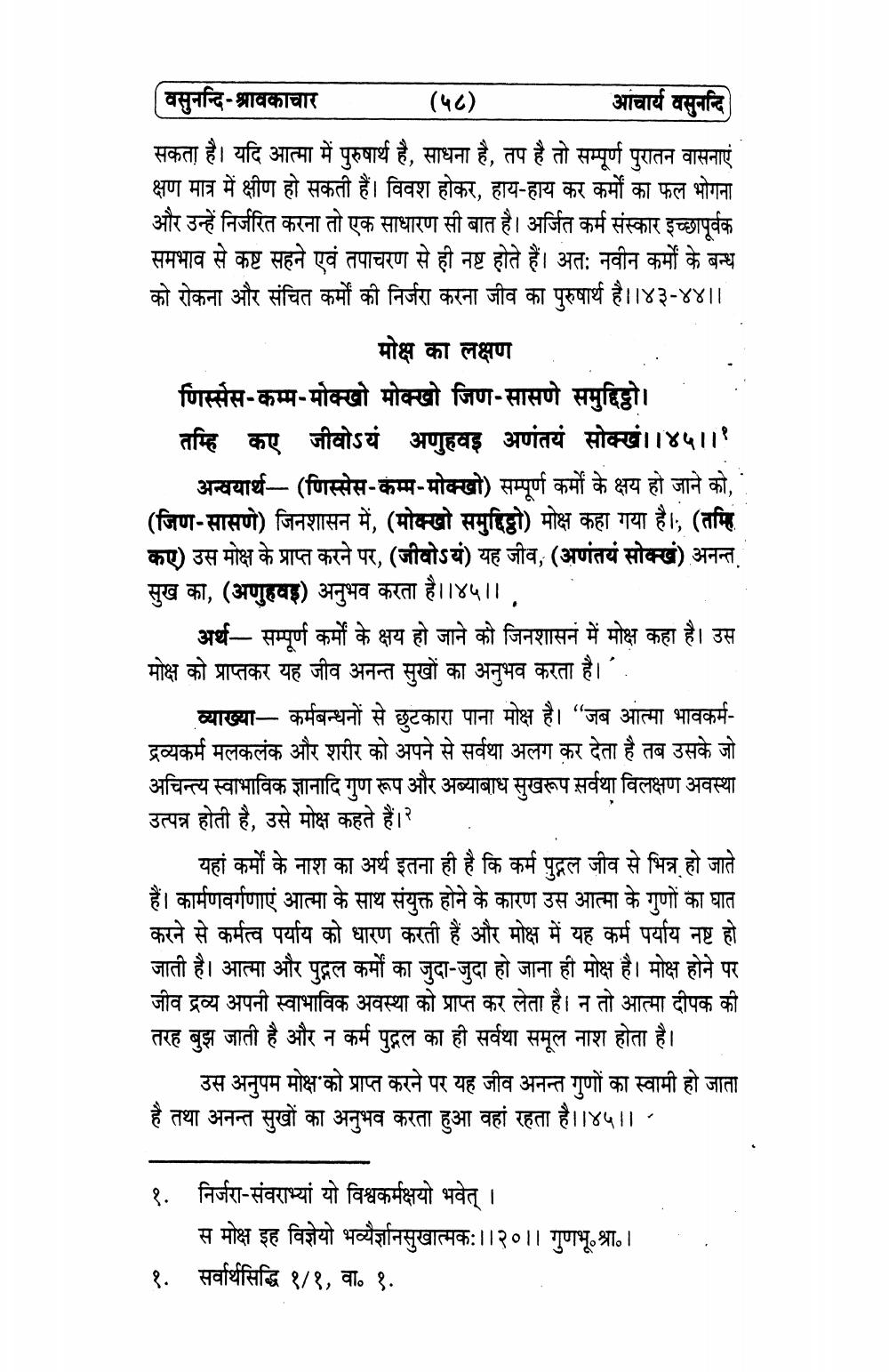________________
(वसुनन्दि-श्रावकाचार
आचार्य वसुनन्दि सकता है। यदि आत्मा में पुरुषार्थ है, साधना है, तप है तो सम्पूर्ण पुरातन वासनाएं क्षण मात्र में क्षीण हो सकती हैं। विवश होकर, हाय-हाय कर कर्मों का फल भोगना और उन्हें निर्जरित करना तो एक साधारण सी बात है। अर्जित कर्म संस्कार इच्छापूर्वक समभाव से कष्ट सहने एवं तपाचरण से ही नष्ट होते हैं। अत: नवीन कर्मों के बन्ध को रोकना और संचित कर्मों की निर्जरा करना जीव का पुरुषार्थ है।।४३-४४।।
मोक्ष का लक्षण हिस्सैस-कम्म-मोक्खो मोक्खो जिण-सासणे समुद्दिट्ठो। तम्हि कए जीवोऽयं अणुहवइ अणंतयं सोक्खं।।४५।।
अन्वयार्थ- (णिस्सेस-कम्म-मोक्खो) सम्पूर्ण कर्मों के क्षय हो जाने को, (जिण-सासणे) जिनशासन में, (मोक्खो समुट्ठिो) मोक्ष कहा गया है।; (तम्हि कए) उस मोक्ष के प्राप्त करने पर, (जीवोऽयं) यह जीव, (अणंतयं सोक्खं) अनन्त सुख का, (अणुहवइ) अनुभव करता है।।४५।। ,
अर्थ- सम्पूर्ण कर्मों के क्षय हो जाने को जिनशासनं में मोक्ष कहा है। उस मोक्ष को प्राप्तकर यह जीव अनन्त सुखों का अनुभव करता है।'
व्याख्या- कर्मबन्धनों से छुटकारा पाना मोक्ष है। "जब आत्मा भावकर्मद्रव्यकर्म मलकलंक और शरीर को अपने से सर्वथा अलग कर देता है तब उसके जो अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अब्याबाध सुखरूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं।२
यहां कर्मों के नाश का अर्थ इतना ही है कि कर्म पद्गल जीव से भिन्न हो जाते हैं। कार्मणवर्गणाएं आत्मा के साथ संयुक्त होने के कारण उस आत्मा के गुणों का घात करने से कर्मत्व पर्याय को धारण करती हैं और मोक्ष में यह कर्म पर्याय नष्ट हो जाती है। आत्मा और पुद्गल कर्मों का जुदा-जुदा हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष होने पर जीव द्रव्य अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। न तो आत्मा दीपक की तरह बुझ जाती है और न कर्म पुद्गल का ही सर्वथा समूल नाश होता है। __उस अनुपम मोक्ष को प्राप्त करने पर यह जीव अनन्त गुणों का स्वामी हो जाता है तथा अनन्त सुखों का अनुभव करता हुआ वहां रहता है।।४५।। ।
१. निर्जरा-संवराभ्यां यो विश्वकर्मक्षयो भवेत् ।
स मोक्ष इह विज्ञेयो भव्यैर्ज्ञानसुखात्मकः।।२०।। गुणभू श्रा.। १. सर्वार्थसिद्धि १/१, वा. १.
.