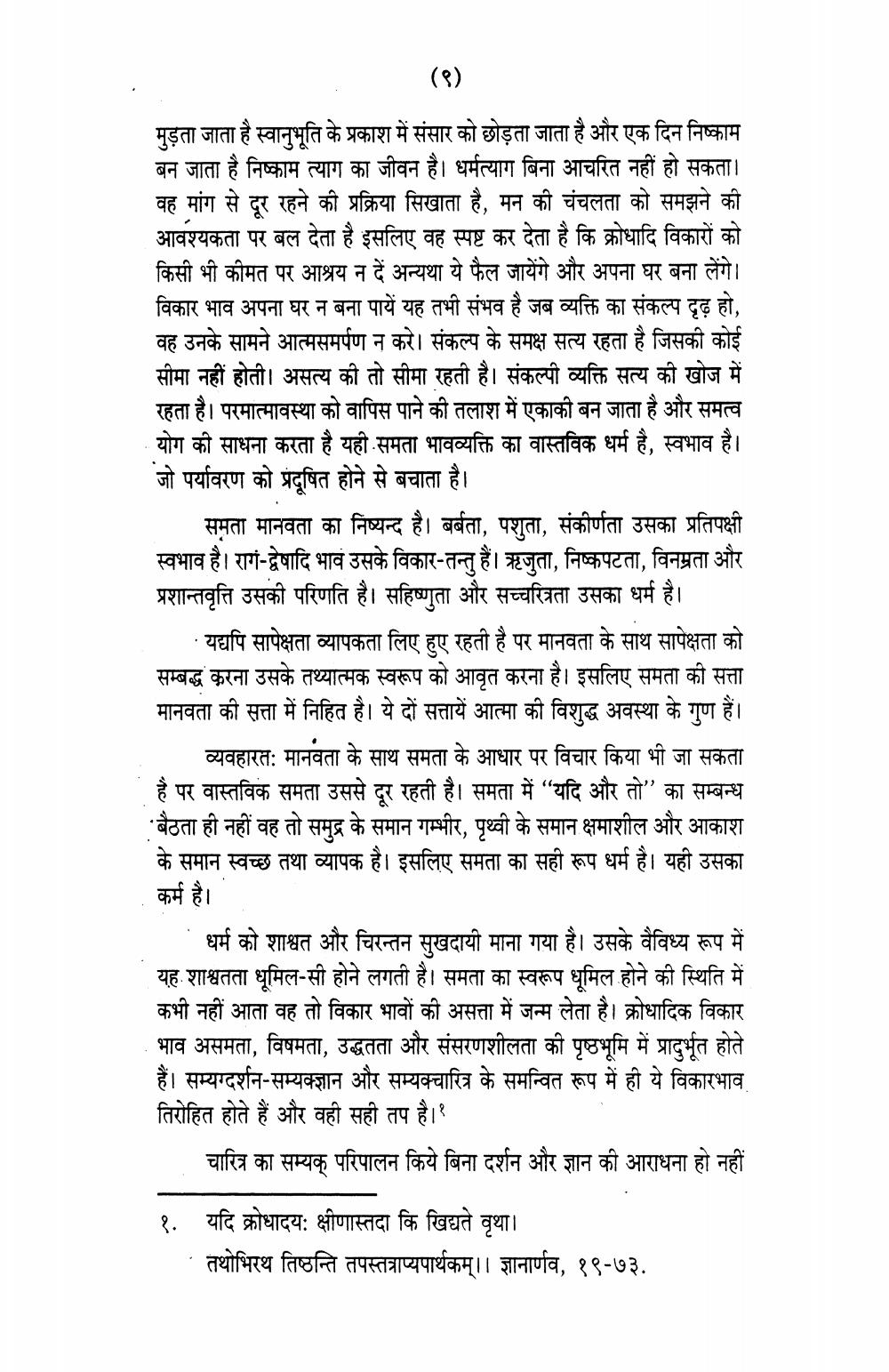________________
(९)
मुड़ता जाता है स्वानुभूति के प्रकाश में संसार को छोड़ता जाता है और एक दिन निष्काम बन जाता है निष्काम त्याग का जीवन है। धर्मत्याग बिना आचरित नहीं हो सकता। वह मांग से दूर रहने की प्रक्रिया सिखाता है, मन की चंचलता को समझने की
आवश्यकता पर बल देता है इसलिए वह स्पष्ट कर देता है कि क्रोधादि विकारों को किसी भी कीमत पर आश्रय न दें अन्यथा ये फैल जायेंगे और अपना घर बना लेंगे। विकार भाव अपना घर न बना पायें यह तभी संभव है जब व्यक्ति का संकल्प दृढ़ हो, वह उनके सामने आत्मसमर्पण न करे। संकल्प के समक्ष सत्य रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। असत्य की तो सीमा रहती है। संकल्पी व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है। परमात्मावस्था को वापिस पाने की तलाश में एकाकी बन जाता है और समत्व योग की साधना करता है यही समता भावव्यक्ति का वास्तविक धर्म है, स्वभाव है। जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है।
समता मानवता का निष्यन्द है। बर्बता, पशुता, संकीर्णता उसका प्रतिपक्षी स्वभाव है। राग-द्वेषादि भावं उसके विकार-तन्तु हैं। ऋजुता, निष्कपटता, विनम्रता और प्रशान्तवृत्ति उसकी परिणति है। सहिष्णुता और सच्चरित्रता उसका धर्म है।
· यद्यपि सापेक्षता व्यापकता लिए हुए रहती है पर मानवता के साथ सापेक्षता को सम्बद्ध करना उसके तथ्यात्मक स्वरूप को आवृत करना है। इसलिए समता की सत्ता मानवता की सत्ता में निहित है। ये दो सत्तायें आत्मा की विशुद्ध अवस्था के गुण हैं।
व्यवहारत: मानवता के साथ समता के आधार पर विचार किया भी जा सकता है पर वास्तविक समता उससे दूर रहती है। समता में “यदि और तो' का सम्बन्ध बैठता ही नहीं वह तो समुद्र के समान गम्भीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील और आकाश के समान स्वच्छ तथा व्यापक है। इसलिए समता का सही रूप धर्म है। यही उसका कर्म है।
— धर्म को शाश्वत और चिरन्तन सुखदायी माना गया है। उसके वैविध्य रूप में यह शाश्वतता धूमिल-सी होने लगती है। समता का स्वरूप धूमिल होने की स्थिति में कभी नहीं आता वह तो विकार भावों की असत्ता में जन्म लेता है। क्रोधादिक विकार भाव असमता, विषमता, उद्धतता और संसरणशीलता की पृष्ठभूमि में प्रादुर्भूत होते हैं। सम्यग्दर्शन-सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के समन्वित रूप में ही ये विकारभाव तिरोहित होते हैं और वही सही तप है। १
चारित्र का सम्यक् परिपालन किये बिना दर्शन और ज्ञान की आराधना हो नहीं
१. यदि क्रोधादय: क्षीणास्तदा कि खिद्यते वृथा।
· तथोभिरथ तिष्ठन्ति तपस्तत्राप्यपार्थकम्।। ज्ञानार्णव, १९-७३.