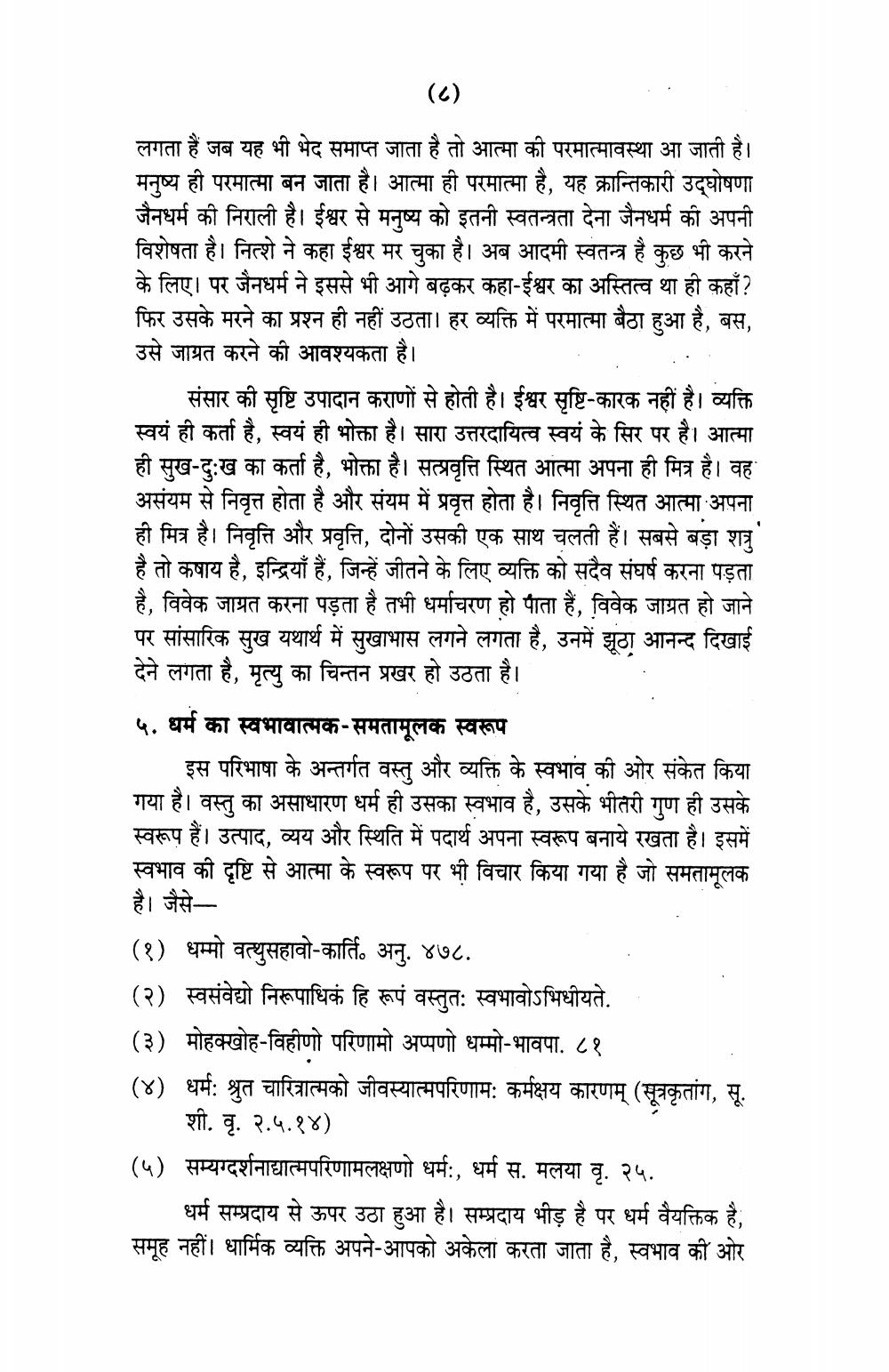________________
लगता हैं जब यह भी भेद समाप्त जाता है तो आत्मा की परमात्मावस्था आ जाती है। मनुष्य ही परमात्मा बन जाता है। आत्मा ही परमात्मा है, यह क्रान्तिकारी उद्घोषणा जैनधर्म की निराली है। ईश्वर से मनुष्य को इतनी स्वतन्त्रता देना जैनधर्म की अपनी विशेषता है। नित्शे ने कहा ईश्वर मर चुका है। अब आदमी स्वतन्त्र है कुछ भी करने के लिए। पर जैनधर्म ने इससे भी आगे बढ़कर कहा-ईश्वर का अस्तित्व था ही कहाँ? फिर उसके मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। हर व्यक्ति में परमात्मा बैठा हुआ है, बस, उसे जाग्रत करने की आवश्यकता है।
__संसार की सृष्टि उपादान कराणों से होती है। ईश्वर सृष्टि-कारक नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही कर्ता है, स्वयं ही भोक्ता है। सारा उत्तरदायित्व स्वयं के सिर पर है। आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता है, भोक्ता है। सत्प्रवृत्ति स्थित आत्मा अपना ही मित्र है। वह असंयम से निवृत्त होता है और संयम में प्रवृत्त होता है। निवृत्ति स्थित आत्मा अपना ही मित्र है। निवृत्ति और प्रवृत्ति, दोनों उसकी एक साथ चलती हैं। सबसे बड़ा शत्रु है तो कषाय है, इन्द्रियाँ हैं, जिन्हें जीतने के लिए व्यक्ति को सदैव संघर्ष करना पड़ता है, विवेक जाग्रत करना पड़ता है तभी धर्माचरण हो पाता हैं, विवेक जाग्रत हो जाने पर सांसारिक सुख यथार्थ में सुखाभास लगने लगता है, उनमें झूठा आनन्द दिखाई देने लगता है, मृत्यु का चिन्तन प्रखर हो उठता है। ५. धर्म का स्वभावात्मक-समतामूलक स्वरूप
इस परिभाषा के अन्तर्गत वस्तु और व्यक्ति के स्वभाव की ओर संकेत किया गया है। वस्तु का असाधारण धर्म ही उसका स्वभाव है, उसके भीतरी गुण ही उसके स्वरूप हैं। उत्पाद, व्यय और स्थिति में पदार्थ अपना स्वरूप बनाये रखता है। इसमें स्वभाव की दृष्टि से आत्मा के स्वरूप पर भी विचार किया गया है जो समतामूलक है। जैसे(१) धम्मो वत्थुसहावो-कार्ति. अनु. ४७८. (२) स्वसंवेद्यो निरूपाधिकं हि रूपं वस्तुतः स्वभावोऽभिधीयते. (३) मोहक्खोह-विहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो-भावपा. ८१ (४) धर्मः श्रुत चारित्रात्मको जीवस्यात्मपरिणाम: कर्मक्षय कारणम् (सूत्रकृतांग, सू.
शी. वृ. २.५.१४) (५) सम्यग्दर्शनाद्यात्मपरिणामलक्षणो धर्मः, धर्म स. मलया वृ. २५.
धर्म सम्प्रदाय से ऊपर उठा हुआ है। सम्प्रदाय भीड़ है पर धर्म वैयक्तिक है, समूह नहीं। धार्मिक व्यक्ति अपने-आपको अकेला करता जाता है, स्वभाव की ओर