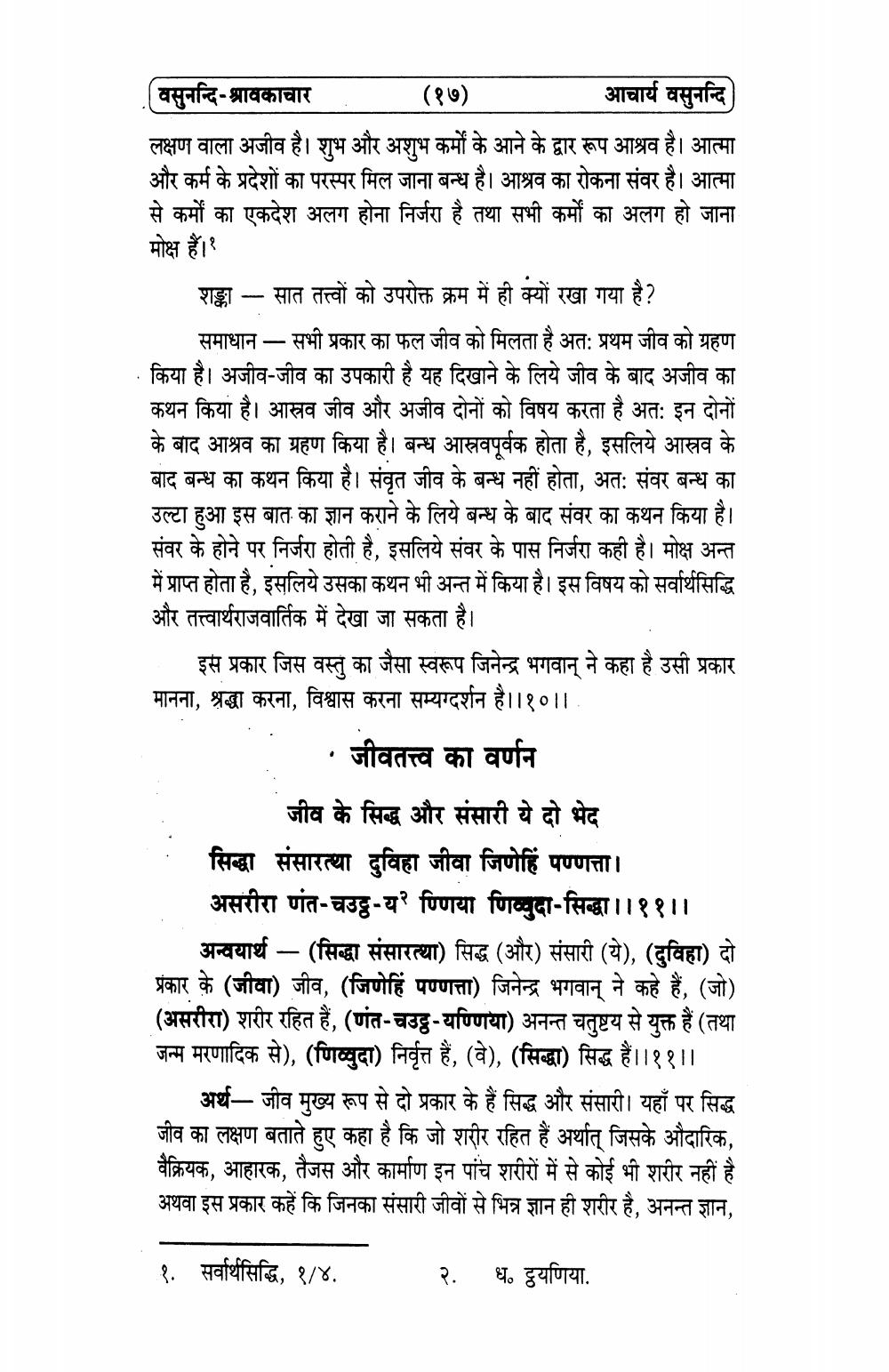________________
(वसुनन्दि- श्रावकाचार
(१७)
आचार्य वसुनन्दि
लक्षण वाला अजीव है। शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार रूप आश्रव है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बन्ध है। आश्रव का रोकना संवर है। आत्मा से कर्मों का एकदेश अलग होना निर्जरा है तथा सभी कर्मों का अलग हो जाना मोक्ष हैं।
शङ्का सात तत्त्वों को उपरोक्त क्रम में ही क्यों रखा गया है ?
-
-
समाधान - सभी प्रकार का फल जीव को मिलता है अत: प्रथम जीव को ग्रहण किया है। अजीव-जीव का उपकारी है यह दिखाने के लिये जीव के बाद अजीव का कथन किया है। आस्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है अतः इन दोनों के बाद आश्रव का ग्रहण किया है । बन्ध आस्रवपूर्वक होता है, इसलिये आस्रव के बाद बन्ध का कथन किया है। संवृत जीव के बन्ध नहीं होता, अतः संवर बन्ध का उल्टा हुआ इस बात का ज्ञान कराने के लिये बन्ध के बाद संवर का कथन किया है। संवर के होने पर निर्जरा होती है, इसलिये संवर के पास निर्जरा कही है। मोक्ष अन्त में प्राप्त होता है, इसलिये उसका कथन भी अन्त में किया है। इस विषय को सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थराजवार्तिक में देखा जा सकता है।
इस प्रकार जिस वस्तु का जैसा स्वरूप जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है उसी प्रकार मानना, श्रद्धा करना, विश्वास करना सम्यग्दर्शन है ।। १० ।
जीवतत्त्व का वर्णन
जीव के सिद्ध और संसारी ये दो भेद
सिद्धा संसारत्या दुविहा जीवा जिणेहिं पण्णत्ता ।
असरीरा णंत - चउट्ठ-य ण्णिया णिव्वुदा- सिद्धा । । ११ । ।
•
अन्वयार्थ (सिद्धा संसारत्या) सिद्ध (और) संसारी (ये), (दुविहा) दो प्रकार के (जीवा) जीव, (जिणेहिं पण्णत्ता) जिनेन्द्र भगवान् ने कहे हैं, (जो) (असरीरा) शरीर रहित हैं, (णंत - चउट्ठ- यण्णिया) अनन्त चतुष्टय से युक्त हैं (तथा जन्म मरणादिक से), (णिव्वुदा) निर्वृत्त हैं, (वे), (सिद्धा) सिद्ध हैं । । ११ । ।
—
अर्थ — जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं सिद्ध और संसारी । यहाँ पर सिद्ध जीव का लक्षण बताते हुए कहा है कि जो शरीर रहित हैं अर्थात् जिसके औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण इन पांच शरीरों में से कोई भी शरीर नहीं है अथवा इस प्रकार कहें कि जिनका संसारी जीवों से भिन्न ज्ञान ही शरीर है, अनन्त ज्ञान,
१. सर्वार्थसिद्धि, १/४.
२.
ध॰ ट्ठयणिया.