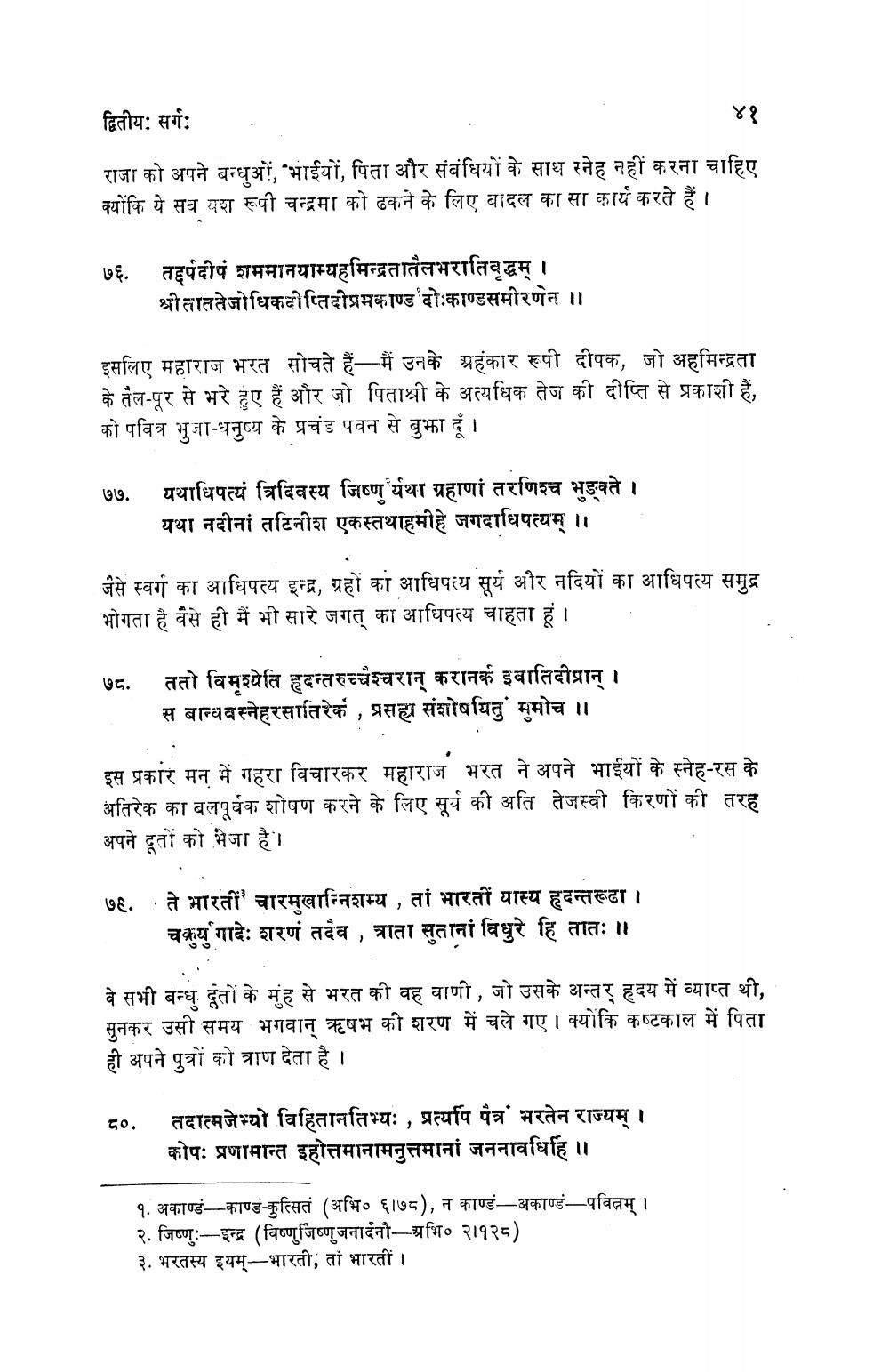________________
४१
द्वितीयः सर्गः
राजा को अपने बन्धुओं, भाईयों, पिता और संबंधियों के साथ स्नेह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब यश रूपी चन्द्रमा को ढकने के लिए बादल का सा कार्य करते हैं ।
७६.
इसलिए महाराज भरत सोचते हैं— मैं उनके अहंकार रूपी दीपक, जो अहमिन्द्रता के तैल-पूर से भरे हुए हैं और जो पिताश्री के अत्यधिक तेज की दीप्ति से प्रकाशी हैं, को पवित्र भुजा धनुष्य के प्रचंड पवन से बुझा दूँ ।
७७.
७८.
तद्दर्पदीपं शममानयाम्यहमिन्द्रतातैलभरातिवृद्धम् । श्री ताततेजोधिकदीप्तिदीप्रमकाण्ड' दोः काण्डसमीरणेन ॥
जैसे स्वर्ग का आधिपत्य इन्द्र, ग्रहों का आधिपत्य सूर्य और नदियों का आधिपत्य समुद्र भोगता है वैसे ही मैं भी सारे जगत् का आधिपत्य चाहता हूं ।
७६.
धिपत्यं त्रिविस्य जिष्णु यथा ग्रहाणां तरणिश्च भुङ्क्ते । यथा नदीनां तटिनीश एकस्तथाहमी हे जगदाधिपत्यम् ||
इस प्रकार मन में गहरा विचारकर महाराज भरत ने अपने भाईयों के स्नेह रस के अतिरेक का बलपूर्वक शोषण करने के लिए सूर्य की अति तेजस्वी किरणों की तरह अपने दूतों को भेजा है।
८०.
ततो विमृश्येति हृदन्तरुच्चैश्चरान् करानर्क इवातिदीप्रान् । सबान्धवस्नेहरसातिरेक, प्रसह्य संशोषयितुं मुमोच ॥
,
ते भारती' चारमुखान्निशम्य तां भारतीं यास्य हृदन्तरूढा । चक्रुर्युगादेः शरणं तदैव त्राता सुतानां विधुरे हि तातः ॥
}
वे सभी बन्धु द्वेतों के मुंह से भरत की वह वाणी, जो उसके अन्तर् हृदय में व्याप्त थी, सुनकर उसी समय भगवान् ऋषभ की शरण में चले गए । क्योंकि कष्टकाल में पिता 'अपने पुत्रों को त्राण देता है ।
तदात्मजेभ्यो विहितानतिभ्यः प्रत्यपि पत्र भरतेन राज्यम् । कोपः प्रणामान्त इहोत्तमानामनुत्तमानां जननावहि ॥
1
१. अकाण्डं -- काण्डं - कुत्सितं ( अभि० ६ । ७८), न काण्डं - अकाण्डं - पवित्रम् ।
२. जिष्णुः - इन्द्र (विष्णु जिष्णु जनार्दनी - अभि० २।१२८ ) ३. भरतस्य इयम् - भारती, तां भारतीं ।