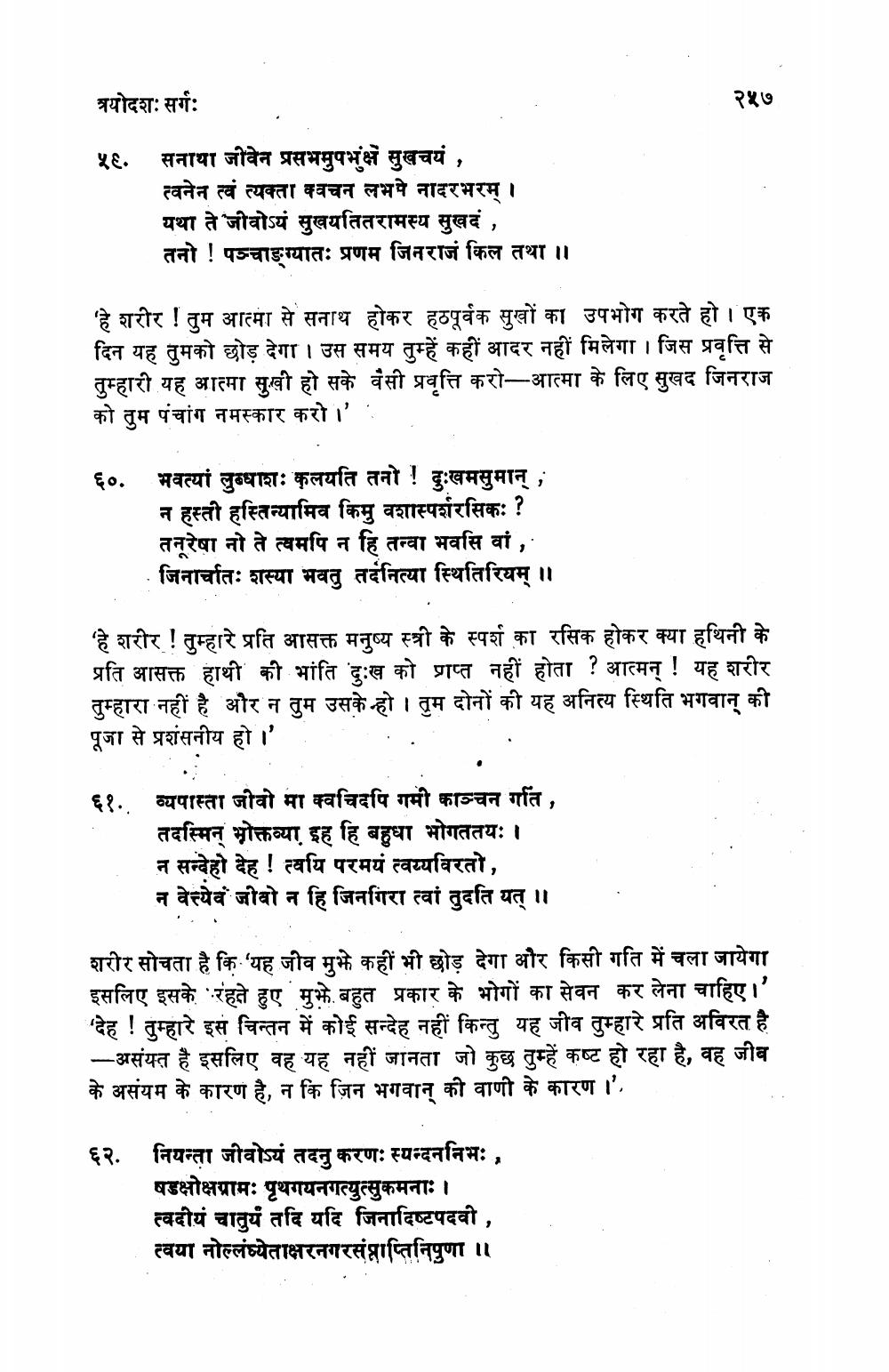________________
त्रयोदशः सर्गः
२५७
५६.
सनाया जीवेन प्रसभमुपभुक्षे सुखचयं , त्वनेन त्वं त्यक्ता क्वचन लभपे नादरभरम । यथा ते जीवोऽयं सुखयतितरामस्य सुखदं , तनो ! पञ्चाङ्ग्यातः प्रणम जिनराजं किल तथा ॥
'हे शरीर ! तुम आत्मा से सनाथ होकर हठपूर्वक सुखों का उपभोग करते हो । एक दिन यह तुमको छोड़ देगा। उस समय तुम्हें कहीं आदर नहीं मिलेगा । जिस प्रवृत्ति से तुम्हारी यह आत्मा सुखी हो सके वैसी प्रवृत्ति करो-आत्मा के लिए सुखद जिनराज को तुम पंचांग नमस्कार करो।'
६०.
भवत्यां लुब्धाशः कलयति तनो ! दुःखमसुमान् ; न हस्ती हस्तिन्यामिव किमु वशास्पर्शरसिकः? तनूरेषा नो ते त्वमपि न हि तन्वा भवसि वां , जिनार्चातः शस्या भवतु तदनित्या स्थितिरियम् ॥
'हे शरीर ! तुम्हारे प्रति आसक्त मनुष्य स्त्री के स्पर्श का रसिक होकर क्या हथिनी के प्रति आसक्त हाथी की भांति दुःख को प्राप्त नहीं होता ? आत्मन् ! यह शरीर तुम्हारा नहीं है और न तुम उसके हो । तुम दोनों की यह अनित्य स्थिति भगवान् की पूजा से प्रशंसनीय हो।'
६१.. व्यपास्ता जीवो मा क्वचिदपि गमी काञ्चन गति ,
तदस्मिन् भोक्तव्या इह हि बहुधा भोगततयः । न सन्देहो देह ! त्वयि परमयं त्वय्यविरतो, न वेत्त्येवं जीवो न हि जिनगिरा त्वां तुदति यत् ॥
शरीर सोचता है कि 'यह जीव मुझे कहीं भी छोड़ देगा और किसी गति में चला जायेगा इसलिए इसके रहते हुए मुझे बहुत प्रकार के भोगों का सेवन कर लेना चाहिए।' 'देह ! तुम्हारे इस चिन्तन में कोई सन्देह नहीं किन्तु यह जीव तुम्हारे प्रति अविरत है
-असंयत है इसलिए वह यह नहीं जानता जो कुछ तुम्हें कष्ट हो रहा है, वह जीव के असंयम के कारण है, न कि जिन भगवान् की वाणी के कारण।'.
६२. नियन्ता जीवोऽयं तदनु करणः स्यन्दननिमः,
षडक्षोक्षग्रामः पृथगयनगत्युत्सुकमनाः। त्वदीयं चातुर्य तदि यदि जिनादिष्टपदवी , त्वया नोल्लंध्येताक्षरनगरसंप्राप्तिनिपुणा ॥